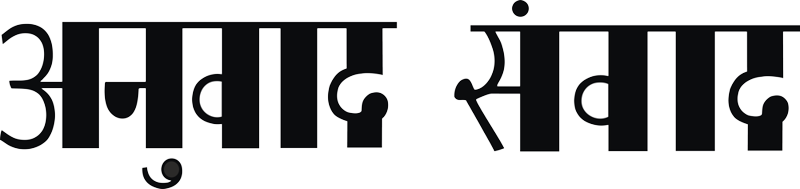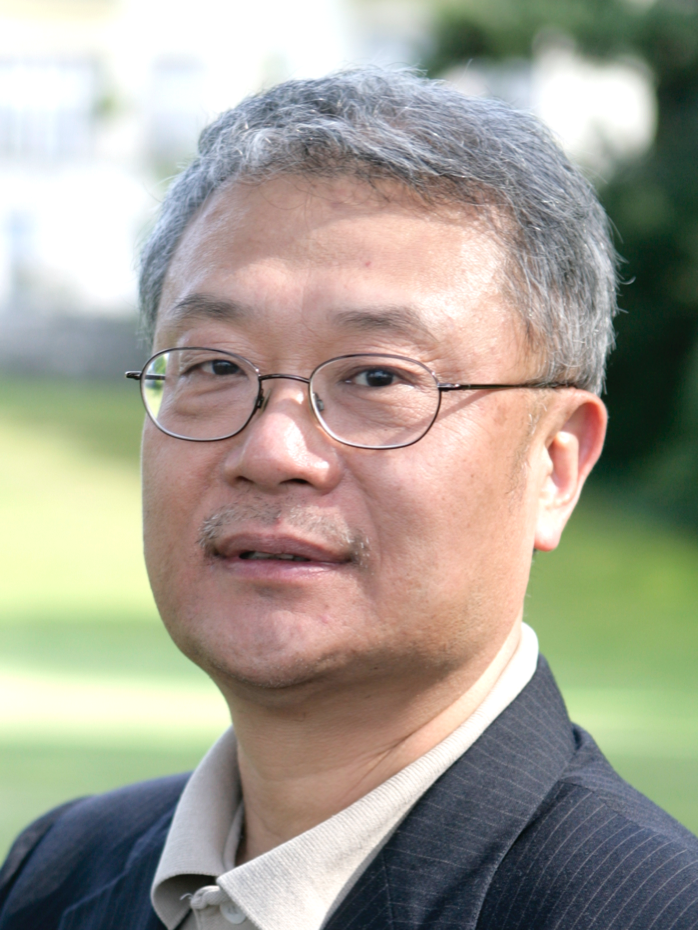Listen to this story
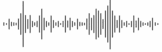
अनुवादक: कुणाल सिंह
स्तोत्र: JSTOR
हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी था ली वान। कभी वह फ़ौज में डॉक्टर रहा था, सन् 63 में नौकरी छोड़ने के बाद से अब वह कम्यून क्लीनिक में डॉक्टरी करता है। उसकी बीवी भी बतौर नर्स वहीं कार्यरत है। शहर के लोग उसे पीठ पीछे ‘दस हज़ारी’ के नाम से पुकारते हैं। उसका यह नाम इसलिए पड़ा कि बैंक में उसने दस हज़ार रुपये जमा कर रखे हैं। सालों पहले लोग-बाग उसे ‘हज़ारी’ कहा करते थे, क्योंकि तब तक उसकी जोड़ी गई रकम की राशि पांच अंकों तक नहीं पहुंची थी। हज़ारी से दस हज़ारी बनने का भी एक क़िस्सा है, जिसे शहर में सब जानते हैं।
हां तो, ली वान बड़ा ही कंजूस आदमी था। उसकी कंजूसी के तमाम क़िस्से शहर के लोगों में आम थे—कि वह टूथपेस्ट या साबुन की जगह सोडे की झाग से काम चलाया करता है, कि उसने अपनी बीवी को इसकी सख्त ताक़ीद कर रखी है कि नूडल्स बनाते समय वह चार से ज़्यादा झींगे न डाले, कि वह एक बार में सिगरेट की पूरी डिब्बी लेने की बजाय चार या पांच सिगरेट ही ख़रीदता है, कि वह टॉयलेट पेपर की जगह भुट्टे के छिलकों का इस्तेमाल करता है आदि। निश्चित रूप से आदमी को फिजूलखर्ची से बचना ही चाहिए। सभी समझते हैं, जैसा कि राशन कार्ड के अंतिम पृष्ठ पर लिखा भी रहता है कि एक दाने का अपव्यय भी किसी भूखे के मुंह से एक कौर छीनने जैसा है।
लेकिन ली वान की तनख्वाह थी 110 युवान, जो किसी औसत मज़दूर के महीने-भर की मज़दूरी का लगभग दूना है। अब इतनी आमदनी वाले किसी व्यक्ति की ऐसी मितव्ययिता लोगों को ज़रूर खटकती है। ऐसे आदमी को थोड़ा-बहुत तो खुले हाथ वाला होना चाहिए। सब्ज़ी या अंडे वालों से उस प्रकार मोल-भाव हरगिज़ नहीं करना चाहिए मानों वह घरेलू चीज़ें नहीं, गाय-बैल ख़रीद रहा हो, या फिर इतना तो ज़रूर करना चाहिए कि बाल-दिवस या किसी ऐसे स्कूली आयोजन पर अपने किसी पड़ोसी के बच्चे को न कुछ तो पेंसिल का डिब्बा ही दे दे, या फिर अन्नोत्सव पर किसी बूढ़े अशक्त को गन्ने का छोटा गट्ठर भेंट कर दे। लेकिन नहीं, इस तरह की किसी सामाजिक सहकारिता में उसे आगे आते आज तक किसी ने नहीं देखा। ‘देना’ क्या होता है, वह जानता ही नहीं। यह उस जैसे किसी संपन्न आदमी को भला शोभा देता है!
ऐसा नहीं था कि ली वान में पैसे की गर्मी और हेकड़ी नहीं थी। अपनी स्वभावगत कृपणता को बहाल रखते हुए भी उसने भौतिक सम्पदा के तमाम दिखावों को प्रश्रय दे रखा था। पूरे इलाक़े में सिर्फ़ उसी के पास दोनाली बन्दूक थी, एक जर्मन कैमरा था और मोटरसाइकिल भी थी। कहते हैं कि पहाड़ी के उस पार एक और आदमी था, जिसके पास मोटरसाइकिल थी। कृषि उर्वरक कारख़ाने में वेल्डरी का काम करने वाला वह आदमी शौक़िया मोटरसाइकिल रखता था, अनजानी लड़कियों को फांसने की गरज से अपने को इंजीनियर से कम ओहदे वाला न बताता था और उन्हें मोटरसाइकिल पर घुमाता रहता। इसके विपरीत ली वान अपनी मोटरसाइकिल को बड़ी संवार-संभाल कर रखता था, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता था।
पुरानी कहावत है कि जहां ऊंच और नीच में कोई भेद नहीं, वहां किसी दुख का वास नहीं। जहां अमीरी और ग़रीबी का फ़र्क़ न हो, वहां सब सुखी और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए पूरा शहर ही ली वान के प्रति ईर्ष्यालु था, जिसकी कृपणता और संपन्नता ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। सभी का मानना था कि यह भगवान का न्याय ही है, जो आज तक उसने बच्चे का मुंह नहीं देखा।
जिन दिनों पूरे देश में सांस्कृतिक क्रान्ति की लहर दौड़ रही थी, शहर में जिन दो जनसंगठनों का अभ्युदय हुआ—माओवादी दल तथा माओ त्से तुंग विचार संघ—दोनों ने ली वान को अपना सदस्य बनाना चाहा, महज़ इसलिए नहीं कि वह अमीर था, बल्कि इसलिए भी कि वह कभी देश की फ़ौज में रहा था। इसके अलावा, वह डॉक्टर था, जो इस तरह के जनसंगठनों में बड़े काम आते हैं, ख़ासकर जब इनके मुक़ाबिल ऐसे गणशत्रु हों, जिनसे निबटने के लिए कभी भी लाठियों, तलवारों, बंदूकों और हथगोलों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन ली वान ने दोनों ही संगठनों को मना कर दिया। चेयरमैन माओ ने कहा था, अगर तुम जनता के दोस्त नहीं हो, तो तुम जनता के दुश्मन हो। इस आलोक में उसकी मनाही ने लोगों में प्रचंड ग़ुस्से और रोष का बीजारोपण कर दिया।
‘माओ विचार संघ’ के कुछ सदस्यों ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया कि ली वान को सबक कैसे सिखाया जाए! यह इतना आसान न था। ली वान के पुरखे ग़रीब खेतिहर थे और वह पार्टी का सदस्य भी था। इस प्रकार भीतर और बाहर से वामपंथ समर्थक ही प्रतीत होता था। बावजूद इसके उन्होंने उस पर नज़र रखने का तय किया, तोंग फेई नाम के एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया कि वह उसके ख़िलाफ़ सबूत जुटाए, उसकी फ़ाइल तैयार करे। जब पूरा शहर क्रान्ति में मसरूफ़ हो, ऐसे कैसे होने दिया जा सकता है कि एक आदमी सप्ताह के आख़िरी दिनों अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा, पीठ पर चमचमाती दोनाली लटकाये पहाड़ों में फाख़्ते का शिकार करता फिरे!
एक दोपहर तोंग फेई ‘माओ विचार संघ’ के दफ़्तर में हांफता हुआ पहुंचा। उपसभापति जियाओ लूमिंग तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के सामने उत्तेजित होकर उसने कहा, “इस बार हमने ली वान को अपने जाल में पूरी तरह फांस लिया है। उसके ख़िलाफ़ ऐसा सबूत लाया हूं कि आप लोगों की बाछें खिल उठेंगी।”
उसने मेज़ पर काग़ज़ के गोले को रखा और उसकी तहें उतारने लगा। उस गोले में से एक टूटा हुआ बिल्ला निकला। बिल्ले पर माओ का मुस्कराता हुआ चेहरा तो सलामत था, लेकिन उस चेहरे से उनकी गर्दन टूटकर अलग हो रही थी। वे सभी उस टूटे बिल्ले को देखकर दंग रह गए।
“यह तुम्हें कहां से मिला?” जियाओ ने उत्तेजित स्वर में पूछा।
“ली वान ने इसे विक्टरी रेस्त्रां के सामने कूड़े के ढेर पर फेंका था। उसे ऐसा करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा,” तोंग ने गर्वोन्नत होकर कहा।
यह जघन्य अपराध था। उन्होंने उसी दम ली वान की पेशनगोई मुक़र्रर कर दी।
उस दिन पत्थर तोड़ने वाले एक घायल मज़दूर के इलाज़ के बाद ली वान को क्लीनिक से निकलने में अबेर हुई। जब वह घर पहुंचा तो छह लोग उसका इंतज़ार करते हुए मिले। जैसे ही उन लोगों की उस पर नज़र पड़ी, उन्होंने कहा, “आपको अभी हमारे साथ बैठक में चलना होगा।”
“कैसी बैठक?” ली ने अपने ऊपरी होंठ पर ज़ुबान फेरते हुए पूछा।
“आप पर कुछ संगीन आरोप लगे हैं।”
“मुझ पर? मैं कोई प्रतिक्रियावादी थोड़े हूं जो मुझ पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगे।”
“आप हैं। भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। हम सभी जानते हैं कि आपने चेयरमैन माओ की तस्वीर वाले बिल्ले को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि उसे कचरे के ढेर में फेंका भी।”
“ओ वह! ...उसे मैंने तोड़ा नहीं था। वह चीनी मिट्टी का था, गलती से फ़र्श पर गिर कर टूट गया।”
बहस का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने उसे पकड़ा और ज़बरदस्ती सराय ले जाने लगे, जहां संघ का मुख्यालय था। इनके ऊपर जो भी व्यक्ति होगा, उससे निबटना ली वान के लिए कोई मुश्किल काम न था, ऐसा उसका मानना था। इसलिए उसने उनके साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं की। फ़ौज के दिनों में उसे इस तरह की पेशियों के पेंचो-ख़म का अनुभव था। उसकी पहुंच भी ऊपर तक थी। उसने साथ चल रहे छहों लोगों पर दृष्टिपात करते हुए सोचा, इन कीड़े-मकोड़ों से तू-तू, मैं-मैं का कोई फ़ायदा नहीं, सीधे इनके बाप से बात करते हैं। उसने जेब में से लपेटकर बनाई गई सिगरेट निकाली और इत्मीनान से पीता हुआ उनके साथ चल पड़ा।
मुख्यालय पहुंचकर वे उसे सीधे डायनिंग रूम में ले गए, जहां क़रीब सौ लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। नारेबाज़ियों के अन्धड़ को पार करते हुए उसे आगे की तरफ़ ले जाया गया और काग़ज़ी बैनर उसके गले में डाल दिया गया, जिस पर बड़े-बड़े काले हर्फ़ों में लिखा था—‘क्रान्ति का दुश्मन।’
संघ के सभापति लिन शोऊ ने चीखते शब्दों में घोषणा की, “कॉमरेड्स, इसे हमने कचरे के ढेर से हासिल किया है।” उसने उस टूटे हुए बिल्ले को ऊंचा करते हुए भीड़ को दिखाया, “...और यह गुनाह किया है आप लोगों के सामने खड़े इस मुजरिम, ली वान ने। हमें यक़ीन है कि ऐसी घिनौनी हरक़त सिर्फ़ वही शख्स कर सकता है जिसके मन में हमारे इस महान नेता के लिए अथाह नफ़रत हो।”
“ली हज़ारी, मुर्दाबाद!” सहसा उस भीड़ में से एक अधेड़ महिला चीखी। उसकी देखा-देखी बाक़ी लोग भी मुक्के लहराते हुए नारेबाज़ी करने लगे। ली वान न सिर्फ़ धन-दौलत के मामले में, बल्कि रहन-सहन और पहनावे-ओढ़ावे के मामले में भी उनसे अलहदा था, बल्कि कहा जाए उन पर बीस था। उसके अपराध को सत्यापित करने के लिए इतना ही काफी था।
लेकिन बस इतने से भयभीत हो जाने वालों में से ली वान नहीं था। सामने की भीड़ पर अवज्ञा और अवहेलना से भरी मुस्कराहट फेंकने के बाद उसने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, “आप लोग आज मुझे क्रान्ति के दुश्मन का तमगा दे रहे हैं। क्या मज़ाक़ है! मैं पूछता हूं, जब मैं अपनी जान की बाज़ी लगाकर कोरिया में उन अमेरिकी भूतों से भिड़ा हुआ था, उस वक़्त आप लोग कहां थे? मैं जानना चाहता हूं कि तब आप लोगों ने देश के लिए, पार्टी के लिए क्या किया? आप लोगों को बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि अपनी सेवाओं के लिए मुझे एक बार नहीं, पार्टी की तरफ़ से दो बार सम्मानित किया गया। अपने इन्हीं हाथों से...” उसने अपने दोनों हाथों को पंखे की तरह लहराया, “...इन्हीं हाथों से मैंने सैकड़ों क्रान्तिकारियों की जानें बचाई हैं, जो आज भी मेरा अहसान मानते हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं। और आप कहते हैं कि मैं क्रान्ति का दुश्मन हूं...”
“कल तुमने देश के लिए क्या किया, इससे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है कि आज तुम देश के लिए क्या कर रहे हो!” भीड़ में से सहसा किसी ने माओ की यह लोकप्रिय उक्ति उछाली।
“यह ले!” जियाओ ने सहसा ली वान के चेहरे पर ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया, फिर दांत पीसते हुए बोला, “...यहां तुझे अपनी शेखी बघारने के लिए नहीं बुलाया गया। आइन्दा अगर एक लफ़्ज़ भी कहा तो तेरी खोपड़ी चटका दूंगा। ...बेशर्म, बद्तमीज़... तू ग़रीब खेतिहर की औलाद था, लेकिन था... आज की तारीख़ में इस शहर में तुझसे बड़ा सामन्त कोई नहीं।”
“ली सामन्त, मुर्दाबाद!” एक आदमी चीखा, तो भीड़ ने तुरन्त यह नारा भी लपक लिया।
तमाचे और इस नए तमगे से ली वान एकाएक हतप्रभ रह गया। उसने अपनी छोटी-छोटी मंगोली आंखों को झुका लिया। किसी तरह बोला, “...मैं कोई गुनहगार नहीं। जो भी हुआ, अचानक और औचक हुआ। काम पर जाते हुए इसी बिल्ले को मैं अपनी वर्दी पर लगाया करता था। जब मैं इसकी सफ़ाई कर रहा था, यह मेरे हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और टूट गया।”
“किसने देखा कि ऐसा ही हुआ?” सभापति लिन ने पूछा।
“किसी ने नहीं। लेकिन मैं भी आपकी तरह ही पार्टी का सम्मानित सदस्य हूं। मैं क़सम खाकर कहता हूं कि मैंने अभी जो कहा, उसमें एक शब्द भी झूठ नहीं था।”
“यह एक नम्बर का झूठा और मक्कार है!” एक साथ बहुत सारे लोगों ने चिल्ला कर कहा। लिन की शान्त और संयत रवैये ने उन्हें क्रुद्ध कर दिया। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा होता तो अब तक अपने घुटनों के बल बैठा दया की भीख मांग रहा होता। लेकिन इस ली वान को देखो, इसे मानो कोई फ़र्क़ ही नहीं पड़ रहा।
सहसा पीछे से निकलकर चार लोग हाथों में लाठियां और रस्सी लिए आगे आए। वे ली वान के दोनों तरफ़ खड़े हो गए, मानो अगले आदेश का इंतज़ार कर रहे हों। उपसभापति जियाओ ने पूछा, “हां तो ली वान, जनता की इस अदालत में क्या तुम अपना यह गुनाह क़बूल करते हो?”
यद्यपि ली वान अब तक किंचित् डर चुका था, उसने धीमे से कहा, “क़बूल करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मैं चेयरमैन माओ के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा अर्पित करता हूं, उनके लिए अपना यह जीवन तक निछावर कर सकता हूं। मैं उनसे नफ़रत क्योंकर करूंगा? उन्होंने मेरे कुटुम्ब की रक्षा की। मेरे दादा-परदादा, सभी सामन्तों के यहां काम करने वाले खेतिहर मज़दूर थे। उन्होंने मेरे दादा-परदादाओं की तरह न जाने कितने लोगों को ग़ुलामी के इस जाल से आज़ाद किया, उन्हें आबाद किया। मैं उनसे भला नफ़रत क्योंकर करूंगा?”
“बन्द करो ये बकवास!” अपना आपा खोकर लिन चिल्ला पड़ा, “खोखले शब्दों से ज़्यादा पुख्ता तथ्य बोलते हैं। अगर तुम चेयरमैन माओ के इतने ही बड़े भक्त हो तो इसे साबित करके दिखाओ।”
“हां-हां, साबित करके दिखाओ।”
“दिखाओ... दिखाओ!”
इसके बाद उस पूरे कमरे में शान्ति छा गई। सभी की आंखें ली वान के मांसल चेहरे पर टिकी थीं, कुछ इस तरह मानो अभी वह देशभक्ति की भावना से पूरित कोई गीत गाने वाला हो अथवा निष्ठा की भंगिमाओं से निर्मित कोई नृत्य प्रस्तुत करने वाला हो अथवा कुछ भी ऐसा करने वाला हो, जो राष्ट्र के प्रति उसके बुलंद जज़्बे का द्योतक हो। वहां इतनी शांति थी कि सराय के पीछे की अस्तबल से किसी घोड़े की हिनहिनाहट और उसका पैर पटकना साफ़ सुनाई दे रहा था।
ली वान थोड़ा सीधा हुआ, तनिक मुस्कराया, गला साफ़ करते हुए बोलना शुरू किया, “अच्छी बात है। मैं आप लोगों को एक क़िस्सा सुनाता हूं। चार साल पहले मैंने चेयरमैन माओ को कुछ फूड कूपन, लगभग पचास किलो एकमुश्त, भेजा था। अकाल में आपकी क्या दशा हुई थी, आपको भली-भांति याद होगा। मेरी भी स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने आप लोगों के विपरीत, राशन में जो भी मिला पूरा का पूरा अपने पेट के हवाले करने की बजाय उन फूड कूपन्स को बचाया और चेयरमैन माओ को भेज दिया। ...क्यों? ...क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं और नहीं चाहता कि वे भी हमारी तरह अनाज के अभाव का सामना करें। यह एकदम सच है—अक्षरशः। आप चाहें तो मेरे पुराने फ़ौजी दस्ते से इस बारे में दरियाफ़्त कर सकते हैं। अगर इसमें एक लफ़्ज़ भी झूठ निकले, आप मेरी गर्दन तराश सकते हैं।”
ली वान की इस बात को सुनकर भीड़ में जैसे खलबली मच गई। कुछ लोग यह सोचकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे कि ली वान जैसा अहमक उन्होंने नहीं देखा। चेयरमैन माओ जैसी हस्ती को भला अनाज का अभाव होगा कभी, जो उन्हें इस अहमक के फूड कूपन्स की अहसानदारी मोल लेनी पड़े! इसके बावजूद ली वान के इस वक्तव्य के बाद इतना तो तय था कि अब कोई यह कतई नहीं कह सकेगा कि उसके मन में चेयरमैन के प्रति निष्ठा और समर्पण का अभाव है। संघ के मेम्बरान भी मन ही मन हंस रहे थे, फिर भी इस पेशी में अचानक आ खड़े हुए इस पेंच का इल्म उन्हें ज़रूर था।
“कृपया शांति बनाए रखें...” सभापति लिन ने अपने मुंह पर हाथ का गोल घेरा बनाकर ऊंची आवाज़ में दरख्वास्त की।
सहसा भीड़ को चीरता हुआ होऊ मेंगशियन नामक मिडिल स्कूल शिक्षक निकला और मंच पर जा चढ़ा। आंखों पर भारी चश्मा चढ़ाये इस नाटे आदमी को आते देख ली वान के शरीर में कंपकंपी-सी दौड़ गई। उसे याद है कि एक बार यह उससे कैमरा उधार मांगने आया था, आदत के अनुसार जिसे देने से ली वान ने साफ़ मना कर दिया था। आगे आकर वह लोगों की तरफ़ उन्मुख हुआ और कहने लगा, “आप लोग इसकी बातों में न आइये। अभी इसने जो कुछ कहा, वह भी एक तरह की प्रतिक्रियावादी हरक़त ही है। अपनी बातों से इसने प्रमाणित कर दिया कि यह क्रान्ति का दुश्मन ही है।” इसके बाद वह ली वान की तरफ़ मुड़ा, “तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो और कोई तुम्हारी चालाकी को ताड़ नहीं सकता, क्यों? ...यह स्पष्ट है कि तुमने वे फूड कूपन्स चेयरमैन माओ को नीचा दिखाने के लिए भेजे थे। तुम उन पर ये ज़ाहिर करना चाहते थे कि उनकी वजह से पूरा देश, तुम दाने-दाने को मोहताज हो गए हो, भूखे मर रहे हो।”
“बिल्कुल नहीं,” ली वान ने तत्परता से उसे खारिज करते हुए कहा, “मैं उनसे प्रेम करता था, इसलिए ख़ुशी-ख़ुशी भूखे मर रहा था।”
“देखिए इसकी शब्दों की बाज़ीगरी...” होऊ ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, “...यह चेयरमैन माओ को कसूरवार बना रहा है। कह रहा है कि यह उनसे प्रेम करता था, इसलिए भूखे मर रहा था। यानी उनसे प्रेम नहीं करता तो भूखे नहीं मरता।”
जनता एकदम चुप थी। लोगों के चेहरों पर एक क़िस्म का उत्सुक विभ्रम छाया हुआ था। ली वान ने होऊ की इस वकालत के लिए दबे स्वर में उसे गाली दी।
“ऐ... ज़बान पर लगाम दे।” तोंग फेई ने चिल्लाकर कहा।
“साहेबान, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं,” होऊ ने बल देकर कहा, “देखिए चार साल पहले, जैसा कि इसने बताया, इसने चेयरमैन को वे कूपन्स भेजे। फिर अचानक से ऐसी कौन-सी बात हो गई कि अगले ही साल ये जनाब फ़ौज में कप्तान रैंक की अपनी नौकरी छोड़कर इस छोटे से गांव में आ बसे? हुजूर ने समझा था कि बीजिंग के नेता मूर्ख हैं, जो इनकी चालाकी नहीं समझेंगे? ...उन्होंने इसकी इस ओछी हरक़त को समझा, और ख़ूब समझा। नतीज़ा?... इसे फ़ौज से निकाल फेंका और इसके पास यहां आकर क्लीनिक में काम करने के अलावा और कोई रास्ता ही न बचा।”
ली वान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह कांपने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई मज़बूत हथौड़े से उसके मस्तिष्क पर लगातार प्रहार किए जा रहा हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहां से कहां जा रही थी। अनजाने ही आंसू की लकीरें उसके कपोलों को सींचने लगीं।
“कॉमरेड्स...” होऊ ने अपनी आवाज़ में ख़म भरते हुए कहा, “मैं सुझाव देता हूं कि हमें किसी को भेज कर सच्चाई का पता ज़रूर लगाना चाहिए कि फ़ौज की नौकरी इसने ख़ुद छोड़ी या इसे वहां से निकाला गया था... और अगर निकाला गया था तो इसकी वजहें क्या और कितनी वाज़िब रही थीं?”
“हमें बताया गया था... फ़ौज में... कि जो हम खाते हैं, चेयरमैन माओ... उन्हें भी वही राशन...” अचानक ली वान फूट-फूटकर रोने लगा। उसके मुंह से जो शब्द निकलते थे, वे हिचकियों और सुबकियों के बीच रगड़ खाकर अपने अर्थ खो दे रहे थे। उसे रोता देखकर लोगों को यक़ीन हो गया कि वह भेड़ की खाल में छिपा बैठा भेड़िया है। नारे और गालियों से पूरा कमरा गुंजायमान हो गया। चार लोग जो लाठी लिए मुस्तैद थे, इशारा पाते ही ली वान पर टूट पड़े।
“बचाओ... हां-हां मैं क्रान्ति का दुश्मन हूं... छोड़ो मुझे, मारो मत।”
“मार डालो इसे।”
“इसकी बखिया उधेड़ दो।”
उस रात ली वान को उस सराय के पीछे वाली अस्तबल में क़ैद करके रखा गया। कार्यकर्ताओं का एक दल उसके घर गया और उसकी समस्त मूल्यवान चीज़ों तथा बैंक के खातों को जब्त कर लिया गया। अगले दिन से उसकी मोटरसाइकिल व कैमरे को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। संघ का कोई भी सदस्य उनका उपयोग कर सकता था। इसी बहाने कइयों ने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया। उसकी दोनाली बन्दूक को संघ की सशस्त्र वाहिनी के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार उन्होंने पहाड़ी पर फाख्तों और खरहों के शिकार करने के बहाने गोली चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
महीने-भर बाद ली वान को सी-नेस्ट नामक गांव में अपने गुनाहों के प्रायश्चित के लिए भेज दिया गया। यह तो ठीक था कि उसे खेतों में नहीं खटवाया गया, बल्कि उसे डॉक्टर के रूप में ही घर-घर जाकर ग़रीब बीमार लोगों को अपनी सेवाएं मुफ़्त में देनी होंगी। ऐसा करते-करते पांच वर्ष निकल गए। इस दौरान प्रांतीय प्रशासन व शेन्यांग मिलिट्री रीजन को वस्तुस्थिति का हवाला देते हुए ली वान ने सैकड़ों ख़त लिख डाले।
छठे वर्ष की शुरुआत में अन्ततः उसके मामले की सुनवाई हुई। तमाम छानबीन के बाद यह साबित हुआ कि वह क्रान्ति का दुश्मन और गद्दार नहीं है, उस पर लगे तमाम आरोप बेबुनियाद और पूर्वाग्रहों से युक्त हैं। उसे बाइज़्ज़त वहां से वापस शहर में बुलाया गया। उसकी जो संपत्ति जब्त की गई थी, उसे लौटा दी गई। हालांकि इन पांच वर्षों में उसकी मोटरसाइकिल की वह गत हुई थी कि वह स्टार्ट भी न हो सकी। इसी तरह कैमरे का लेंस टूट चुका था और दोनाली बन्दूक की एक नाली फूट चुकी थी।
इसके बावजूद वह मुनाफ़े में ही रहा। इन पांच वर्षों में बैंक में जमा उसकी पूंजी मय सूद उसे सुपुर्द कर दी गई। साथ ही देहात में उसने पाँच वर्षों तक जो मुफ़्त की डॉक्टरी की थी, बेकसूर साबित होने के बाद इस अवधि को उसकी नौकर में शामिल किया गया और एकमुश्त पांचों वर्ष की तन्ख्वाह दी गई। अर्थात् उसकी पूंजी एकाएक दोगुनी हो गई। जिस दिन उसने उस राशि को बैंक में जमा किया, उसी दिन से वहां का क्लर्क पूरे शहर में घूम-घूमकर इस बात की मुनादी-सा करने लगा कि उसके नाम कुल जमा-पूंजी दस हज़ार से भी ऊपर चली गई है। इस प्रकार वह ‘हज़ारी’ से ‘दस हज़ारी’ हो गया। “कौन कहता है कि ईश्वर के घर में देर ही देर है...” लोग-बाग कहने लगे, “...बताइए कि महीने भर खटने के बाद एक आम आदमी जितना कमा पाता है, यह दस हज़ारी तो बिना कुछ किए-धरे उससे ज़्यादा सूद पा लेता है, यह अंधेर नहीं तो और क्या है!”
मुक़दमा जीतने के बाद ली वान ने पूरे शहर को लानत भेजी। उसने नई मोटरसाइकिल ख़रीदी और मेड-इन-शांघाई का नया कैमरा भी। उसने शिकार पर जाना छोड़कर मछली मारने का नया शग़ल पाल लिया। इसके लिए उसने स्टील की दो बंसियां ख़रीदी और नायलॉन का जाल भी। इन दिनों वह रबड़ की नैया भी ख़रीदने की सोच रहा है। पुराने दिनों की ही तरह ही वह किसी से राब्ता नहीं रखता है—न किसी को अपना कैमरा उधार देता है और न किसी को मोटरसाइकिल छूने देता है। अब भी उसे सब्ज़ी-ठेले वालों से हील-हुज्जत व मोल-भाव करते देखा जा सकता है। लोग-बाग उसकी कंजूसी के क़िस्से सुनाते हैं और मन ही मन दूसरी किसी क्रान्ति के होने की राह ताकते हैं।