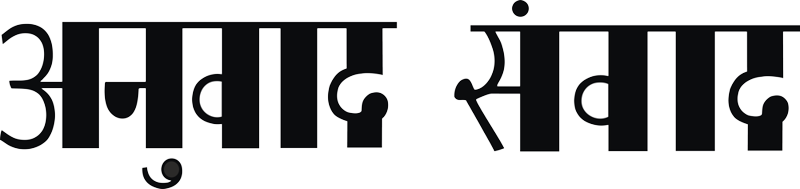Listen to this story
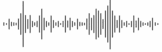
पटचित्र: https://www.facebook.com/sharjeelusmanifb?mibextid=ZbWKwL
अनुवाद: अंकुल बड़ौनियाँ
स्त्रोत: Firstpost
मौत डरावनी हो सकती है।
जिस संस्था की जिम्मेदारी ही क़ानून और न्याय व्यवस्था को स्थापित करना हो उसके द्वारा इरादतन या गैर-इरादतन हत्या दिल दहला देने वाली है।
अगर आरोपी संस्था द्वारा हुई मौत सिर्फ इरादतन ही नहीं सांप्रदायिक भी हो तो यह कुछ और नहीं सिर्फ उत्पीड़न है।
हाल ही में जिला अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश में 22 वर्षीय रिजवान अहमद की मौत कथित रूप से पुलिस की पिटाई से हो गई। इस तरह की घटनाएं हमें भारतीय मुसलमान और पुलिस के बीच के रिश्ते के चरित्र को जानने के लिए और जद्दोजहद करने पर मजबूर करती हैं।
यह कहा जाता है कि लोकतंत्र में ताकत जनता के पास रहती है। रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत सरकार (2003) मामले में चीफ जस्टिस वी.एन. खरे के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय जजों की बेंच ने इस बात पर जोर डाला, “हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ा कार्यालय जनता का है, यह केवल कहने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अमल में भी लाना होगा।” लोकतंत्र में सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि कहावत में सबसे बड़ी अफसर ‘जनता’ को शांति, सम्पन्नता और न्याय प्रदान करे। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सरकार कानून के कायदों का पालन करती है, जिन्हें प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है।
समाज में कानून का पालन करवाना और व्यवस्था बनाये रखना इन एजेंसियों की अहम जिम्मेदारी होती है। सरकार और जनता के बीच संपर्क के प्रथम बिंदु होने के कारण यह जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पुलिस महकमे के ऊपर आती है, जब तक कि स्थिति बेकाबू ना हो जाए। “गुप्त” बॉम्बे पुलिस मैन्युअल (1959) के बारवें अध्याय में शीर्षक “ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों का व्यवहार” के अंतर्गत पुलिसवालों को हिदायत दी गई है कि वे खुद को जनता का सेवक समझें तथा उनके रक्षक के रूप में कार्य करें, और कानून का पालन करने वाले सभी नागरिकों से बिना उनके ओहदे को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से धैर्य, शिष्टाचार और समझदारी से बर्ताव करें।
सांप्रदायिक तनाव के दौरान पुलिस की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्र में पुलिस का किरदार सिर्फ संवेदनशील ही नहीं, बल्कि तनाव को कम करने या बढ़ाने में निर्णायक होता है। 1 अक्टूबर 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने मुख्यमंत्रियों को लिखे गए पत्र में कहा था, “अगर वे (पुलिस अधिकारी) सक्षम और सही समझ वाले हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर वे सक्षम नहीं हैं और असामाजिक व सांप्रदायिक तत्वों के साथ घाल-मेल कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल, दिक्कतें आना लाज़मी हैं।”
उस समय शायद नेहरु यह नहीं देख पाए कि जो नौकरशाही चलाने के लिए ढांचा उन्होंने अंग्रेजों के जमाने से उठाया है, वह संविधान की “विधिक-तार्किक” व्यवस्था पर निर्भर है। इसके बारे में आगे विस्तार से बात की जाएगी।
***
शुरुआत में, भारतीय पुलिस बल की धार्मिक-जातीय संरचना पर ध्यान देना हिदायत भरा है। ओमर खालिदी अपनी किताब ‘खाकी एंड एथनिक वायलेंस इन इंडिया’ में लिखते हैं कि भारतीय राज्य ने सशस्त्र बल, पुलिस और अर्धसैनिक बल में भरती के लिए अल्पसंख्यकों (खासकर मुसलमान) के साथ भेदभाव किया है। किताब के पहले भाग में वह इसके लिए अहम दलील देते हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती नस्लीय/जातीय आधार पर होती है, ना कि क्षेत्रीय जनसंख्या के आधार पर।
नस्लीय/जातीय सिधांतो के अनुसार, कुछ नस्ले/जातियां (जिन्हें लड़ाकू प्रजातियां भी कहा जाता है) सशस्त्र बलों में नौकरी के लिए ‘गैर लड़ाकू प्रजातियों’ से ज्यादा उपयुक्त होती हैं, इसलिए भरती केवल लड़ाकू प्रजातियों के लिए ही आरक्षित होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, सिख और गोरखा जैसे समुदाय जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा प्रतिनिधित्व पाते है तथा मुसलमान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जनसंख्या के अनुपात में बेहद कम प्रतिनिधित्व रह जाता है। खालिदी बताते है कि 2004 में दस लाख से ज्यादा सैनिक और अफसर वाली भारतीय सेना में कुल 29,093 ही मुसलमान थे।
लड़ाकू प्रजातियों की अवधारणा अंग्रेज सैन्य अधिकारीयों द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद लाई गई। इसके पीछे यह विचार था कि हर समुदाय को लड़ाकू और गैर-लड़ाकू में वर्ग्रीक्रत कर दिया जाए और फिर सिर्फ लड़ाकू समुदायों की सेना में भर्ती करें, क्योंकि ‘वे बहादुर हैं और लड़ने में ज्यादा सक्षम हैं।’ गैर-लड़ाकू समुदायों को उनकी जीवनशैली के कारण शारीरिक रूप से कमजोर देखा गया और लड़ने में अक्षम माना गया। यह अवधारणा वैदिक हिन्दू धर्म के जाति और वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत से बिल्कुल मिलती जुलती है, जो लोगों को चार वर्णों में बांटती है, जिसमें एक वर्ण है क्षत्रिय या योद्धा।
आजादी के बाद 1 फ़रवरी, 1949 को प्रेस सूचना ब्यूरो की विज्ञप्ति के अनुसार, भारत सरकार ने सेना में “निश्चित प्रतिशत के आधार पर वर्ग संरचना” को समाप्त कर दिया है तथा सेना में भर्ती “सभी वर्गों के लिए खोल दी गई है”। हालांकि, सभी वर्गों के लिए खोली गई भर्ती का मतलब यह नहीं कि उनको उनकी जनसंख्या के सही अनुपात में भर्ती में प्रतिनिधित्व मिले। वास्तव में औपनिवेशिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। स्टीवन विलकिंसन अपनी किताब ‘आर्मी एंड नेशन’ में कहते हैं कि आज़ाद भारत औपनिवेशिक तरीकों से ही भर्ती करता रहा है। उन्होंने अपनी जांच-पड़ताल से यह बताया कि 1970 के शुरुआती सालों तक “लड़ाकू वर्ग की इकाइयां दुगनी हो गई थीं।”
पुलिस महकमे की संरचना की चर्चा करने से पहले यह बताना जरूरी है कि प्रवर्तन संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव का क्या कारण है? चूंकि पुलिस प्रशासन प्रदेश सरकार के अधीन आता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को समझने के मुख्यतः दो कारण हैं: पहला कि आबादी के हिसाब से यह सबसे बड़ा प्रदेश है, दूसरा यह भारत में सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित प्रदेशों में से एक है।
बंटवारे से पहले के भारत में मुसलमानों को पुलिस प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता था। बंटवारे के समय मुसलमान उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे की 40 प्रतिशत संख्या में थे। कुछ दशकों के अंतराल के बाद मुसलमानों की संख्या कम होती गई। 1990 तक उनकी संख्या मात्र 5 प्रतिशत ही रह गई। द इलेक्टोरल ओरिजिंस ऑफ़ एथनिक वायलेंस: हिन्दू मुस्लिम रायट इन इंडिया नामित अपने शोध में येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीवन विलकिंसन ने बताया कि 1981 तक मुसलमानों का पुलिस महकमे में प्रतिनिधित्व- वरिष्ठ (गजेटेड) अधिकारियों में 3 प्रतिशत, इंस्पेक्टरों में दो प्रतिशत और सब इंस्पेक्टरों में चार प्रतिशत था। बाकी प्रदेशों में भी अगर इससे घटिया नहीं तो इतने ही बुरे हाल हैं। 2006 में पेश की गई सचर कमेटी की रिपोर्ट भी पुलिस महकमे में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के बुरे हाल उजागर करती है।
***
नेहरूवादी नौकरशाही संरचना की बात करें तो इस व्यवस्था में “तर्कहीन” राजनेता और “तर्कसंगत” नौकरशाह के संबंधों पर ध्यान दिया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और लेखक के.एस. सुब्रमण्यम ने अपनी पुस्तक पोलिटिकल वायलेंस एंड पुलिस इन इंडिया में बताया “मौजूदा वास्तविकताओं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हकीकत से बिल्कुल अलग-थलग होने के कारण यह व्यवस्था पूर्णतः भटकी हुई नजर आती है।” अंग्रेजों से अपनाई गई नेहरूवादी नौकरशाही संरचना एक विधिक-तार्किक प्रणाली थी, जो इस विचार पर आधारित थी कि राज्य शासन का क्षेत्र है और उससे सम्बंधित बातचीत कानूनी और औपचारिक ढांचे में की जाएगी।
यह व्यवस्था अंग्रेजों के लिए कारगर रही होगी, पर भारत जैसे “राजनीतिक समाज” में राज्य और जनता के बीच बातचीत राजनीतिक दलों, विद्यार्थी आंदोलनों और अलग तरह के अनौपचारिक माध्यमों से बहुत अस्त-व्यस्त तरीके से होती है। एक और महत्वपूर्ण कमी, जो इस व्यवस्था में पाई जाती है और जो गलती नेहरु ने भी की, वह यह कि नौकरशाह और पुलिस अधिकारियों की “तर्कसंगतता” पर काफी ज्यादा विश्वास किया गया।
भारत जैसे बहु-प्रजातीय देश में, जिसकी सामाजिक संरचना इतनी जटिल है कि जहां जाति-आधारित मतभेद, धर्म आधारित वर्गीकरण, क्षेत्रीय अंतर, परम्पराओं में भिन्नता तथा 130 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली 500 भाषाओं और बोलियों आदि से पहचान बनती है, यह असंभव-सा काम है कि नौकरशाहों को इन सभी पहचानों से मुक्त करवाया जा सके, क्योंकि इन सारी पहचानों के समाज में अपने अलग ओहदे हैं, जिनको वरीयता मिली हुई है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन दि एलिमिनेशन ऑफ आल फॉर्म्स ऑफ रेशीयल डिस्क्रिमिनेशन (ICERD) के अंतर्गत 14 सामायिक रिपोर्ट में भारत सरकार ने माना है कि “बहुत बड़ी आबादी के लिए जाति व्यवस्था आज भी उनकी पहचान और सामाजिक रिश्तों को निर्धारित करती है।”
सरल शब्दों में कहें तो ‘पिछ्ड़ी जाति’ का व्यक्ति बड़ा अधिकारी हो सकता है, पर उसका सामाजिक ओहदा अपने से निचले स्तर के अग्रणी जाति के अधिकारी से कम होगा। यह “विधिक-तार्किक” कानून व्यवस्था इस सामाजिक ऊंच-नीच से होने वाले भेदभाव को नहीं सुलझा पाई।
वकील और संविधान विशेषज्ञ ए. जी. नूरानी अपने निबंध “मुस्लिम्स एंड पुलिस” में पॉल ब्रास द्वारा संपादित किताब “रायट्स एंड पोग्रोम्स“ के दो योगदान-कर्ताओं के हवाले से बताते हैं, “लेखकों को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रादेशिक सुरक्षा बल की वर्दी उतार लेने के बाद वह पूरी तौर से हिन्दू हैं। वह ग्रामीण भारत की पारंपरिक, लोक संस्कृति से पूरे ओत-प्रोत हैं। कांस्टेबल का प्रशिक्षण उनको कुछ हद तक व्यावसायिकता में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उनकी कट्टर हिन्दू पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हिन्दू पहचान बुरे समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य के व्यक्तित्वहीन साधन की उसकी व्यावसायिक पहचान पर भारी पड़ती है।”
पुलिस अधिकारियों को दी गई खुले हाथ और गैरजवाबदेही वाली ताकत अल्पसंख्यकों, ख़ासकर मुसलमान और निचले सामाजिक तबके के लोगों को बड़ी दयनीय स्थिति में डाल देती है। स्थिति इतनी भयानक है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिलने वाली 60 प्रतिशत शिकायतें सिर्फ पुलिस के द्वारा ताकत का दुरुपयोग और मानव अधिकारों के उल्लंघन की हैं।
1960 के बाद से उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई दंगा हो, जहां प्रेस, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानव अधिकार समूहों ने PAC का किरदार मुसलमान विरोधी और पक्षपात पूर्ण न माना हो। इकबाल अंसारी द्वारा सम्पादित कम्युनल रायट्स एंड द पुलिस के अनुसार, 1972 और 1973 में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर PAC द्वारा श्रंखलाबद्ध तरीके से अत्याचार किए गए—5 जून 1972 को अलीगढ़, 16 जून 1972 को फिरोजाबाद और बनारस, 21 सितम्बर को दादरी, 15 नवम्बर को नोनारी, 12 दिसंबर को सजनी, 29 दिसंबर को रानिमाऊ, 23 जनवरी 1973 को दुर्गाजोत और 14 फ़रवरी 1973 को गोंडा में।
कम्युनल वायलेंस एंड पुलिस में गिरीश माथुर द्वारा लिखी एक रिपोर्ट बताती है: “फिरोजाबाद, बनारस, आजमगढ़ और बस्ती में हुए उपद्रव वास्तव में सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, बल्कि वे सशस्त्र कांस्टेबलों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ की गई आक्रामक कार्यवाही थी।” PAC का पक्षपात भरा रवैया मुरादाबाद दंगे (1980), मेरठ दंगे (1982) और हाशिमपुरा हत्याकांड में खुले तौर पर सामने आया।
***
हाल ही में मुसलमानों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के और भी उदाहरण है, जिन पर आगे चर्चा की जाएगी, पर अभी “दंगों” और “नरसंहार” के बीच का फर्क स्पष्ट करना होगा। सही शब्दों में व्याख्या की जाए तो जब दो समुदाय या जातीय/नस्लीय समूह के बीच हिंसात्मक टकराव हो तो वह दंगा कहलाता है। वहीं सरकारी मशीनरी की मदद के साथ योजनाबद्ध तरीके से एक समुदाय, ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं को “नरसंहार” कहते हैं। पुरस्कार विजेता लेखक और ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने फॉरेन पॉलिसी के एक इंटर्वूय में कहा, ”नरसंहार एक ख़ास किस्म के दंगे होते हैं, जहां पर सिर्फ दो भीड़ या समुदायों के बीच टकराव नहीं रहता। बल्कि, पुलिस एक पक्ष के साथ मिलकर या तो उनकी करतूतों को अनदेखा करती है या कई बार खुद हिंसा में शामिल होती है या उसे बढ़ावा देती है।” वह आगे कहते हैं, “दंगों और नरसंहार के बीच का मुख्य अंतर राज्य के रवैये, खासकर पुलिस के व्यवहार से दिखता है।”
“दंगों” और “नरसंहार” के बीच के अंतर पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि शब्दावली का धूर्तता से किया गया प्रयोग हिंसा का इल्जाम राज्य की जगह मारे गए समुदाय पर डालता है। राजनीतिक मानव विज्ञानी इरफान अहमद अपने जानकारी भरे और समयोचित लेख में “नरसंहार” की जगह “दंगे” शब्द के प्रयोग के पीछे की राजनीति के बारे में बतलाते है कि यह जानबूझ कर भारतीय हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच के ताकत के इतने बड़े अंतर को बेहद कम दिखाने के लिए किया गया है। सरल शब्दों में, उनका मतलब है कि एक “नरसंहार” को “दंगा” कहने से जिम्मेदारी और बोझ दोनों पक्षों के कंधों पर आ जाता है—और भारत में सांप्रदायिक दंगों के मामले में यह हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों पर आता है। इससे राज्य का नरसंहार कराने में योगदान भी ढक जाता है और पुलिस की मिलीभगत पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं बचता।
हाल ही में हुई दिल्ली हिंसा से यह भी समझ आया कि कैसे शब्दों की राजनीति से लोगों को दो खेमों में बांटा जा सकता है। जिन लोगों ने हिंसा को “दंगा” कहा वे अच्छे और जिन्होंने उसे “नरसंहार” कहा, वे “उग्रवादी”। बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों के विरुद्ध हिंसक घटनाओं में ऐतिहासिक रूप से पुलिस की सहभागिता को अंकित किया है और घटनाओं के वर्णन में धूर्तता पूर्ण शब्दावली के इस्तेमाल पर प्रश्न उठाए हैं। लेकिन आम लोगों की सोच और मुख्यधारा की मीडिया में यह बातें अभी तक नहीं मानी गई हैं। खैर, मुसलमानों के विरुद्ध पुलिस का संस्थागत दोहरा रवैया कभी-कभी लोगों के सामने आ ही जाता है।
***
सन् 1997 के नवंबर माह के आखिर से दिसम्बर माह के पहले हफ्ते के बीच कोयंबतूर में सांप्रदायिक हिंसा हुई। तीन दिनों तक चले उपद्रव में हत्या, आगजनी, लूट और पुलिस के द्वारा गोलीबारी हुई, जिसमें 18 मुसलमान और 2 हिन्दुओं के मारे जाने की खबर आई। यह भी सांप्रदायिक हिंसा का “सामान्य” मामला हो सकता था, जो कि भारत में अक्सर होता रहता है, परन्तु इसमें मुसलमानों के खिलाफ “पुलिस वालों का विद्रोह” शामिल था। फ्रंटलाइन ने सूचना दी, “जब हिंसा शुरू हुई तो हिन्दू और मुसलमान आमने-सामने खड़े थे और पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ गोलीबारी शुरू कर दी।” दस मुसलमान नौजवान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। फ्रंटलाइन ने यह भी उजागर किया कि “पुलिस के द्वारा बगावत करने के बाद अराजक हो रही स्थिति को रोकने के लिए तमिल नाडू सरकार ने सेना और रैपिड एक्शन फ़ोर्स को बुलाया।” तत्कालीन पुलिस डायरेक्टर जनरल एफ सी शर्मा को सामने आकर इन इल्जामों को खारिज करना पड़ा कि “कोयंबतूर में पुलिस सांप्रदायिक है।”
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) और भारत के क्विल फाउंडेशन ने मिलकर 2018 में एक शोध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि मुसलमान नागरिकों के प्रति पुलिस के बर्ताव को भारतीय लोग किस नजरिए से देखते हैं। यह शोध उजागर करता है कि “तीन पुलिस प्रमुखों ने वर्ष 2013 में पुलिस प्रमुखों की वार्षिक कांफ्रेंस में दंगों के दौरान पुलिस के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय पुलिस को ‘सांप्रदायिक, पक्षपाती, असंवेदनशील, जाहिल और भ्रष्ट’ मानते हैं।” शोध यह भी बताता है कि वह रिपोर्ट कभी सार्वजानिक नहीं की गई।
हालांकि पुलिस मुसलमानों के खिलाफ अपने पूर्वाग्रहों को नहीं मानती, पर बहुत-सी राष्ट्रीय कमेटियां और न्यायालय के निर्णयों ने इस ओर इशारा किया है। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने PAC के 17 पूर्व कर्मियों को 1987 में हुए हाशिमपुरा नरसंहार में हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूतों को मिटाने के लिए भारतीय दंड संहिता के अनुरूप अपराधी ठहराया। अदालत ने अपने निर्णय में इसे निहत्थे और असहाय लोगों पर किए गए नरसंहार को योजनाबद्ध हत्या की परिभाषा दी।
सबूत यह भी दर्शाते हैं कि पुलिस का व्यवहार सिर्फ सांप्रदायिक दंगों के दौरान ही पूर्वाग्रहों से नहीं भरा रहता है, बल्कि हिंसा के बाद इन घटनाओं की विवेचना के दौरान भी यही हाल रहता है। 18 फ़रवरी 1983 की सुबह मध्य असम के नोवगोंग जिले के नेली और 13 अन्य मुसलमान बाहुल्य गांवों में 1800 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। यह घटना नेली नरसंहार के नाम से जानी जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी और राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने नेल्ली गांव के सरकारी स्कूल में बनाए गए शरणार्थी कैंप का दौरा भी किया था और उचित मुआवजे और हिंसा की जांच का वादा किया था।
खैर, कुल दर्ज की गई 688 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में से पुलिस ने सिर्फ 299 में आरोप दाखिल किए, जिनमें से एक भी सिद्ध नहीं हुआ। उसी साल तिवारी कमीशन का गठन मामले की जांच करने के लिए हुआ। कमीशन ने 1984 में अपनी रिपोर्ट जमा की लेकिन उस रिपोर्ट पर कभी चर्चा नहीं की गई। मृत हुए व्यक्ति के रिश्तेदार को 5000 तथा घायलों को 2000 रुपये का वादा किया गया “उचित” मुआवजा मिला।
इस साल फ़रवरी में हुई दिल्ली हिंसा के दौरान, कई तथ्य-खोजी रिपोर्टों ने पाया कि पुलिस ने हिंसा के आयोजन में पक्षपाती रवैया अपनाया। दंगाइयों द्वारा “जय श्री राम” की उद्घोषणा के साथ “दिल्ली पुलिस जिंदाबाद” के नारे के विडियो भी इन्टरनेट पर पाए गए, जो दंगाइयों को पुलिस से मिले समर्थन को दर्शाता है। यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन (YHRD) ने अपनी तथ्य-खोजी रिपोर्ट में बताया कि हिंसा के खत्म होने के कुछ समय बाद ही पुलिस ने 654 मुक़दमे दर्ज किए और 1820 लोगों को या तो थाने में रखा या गिरफ्तार किया। इन में अधिकतर मुसलमान थे।
1992-93 के मुंबई दंगों पर श्रीकृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस आम तौर पर मुसलमानों के खिलाफ पक्षपाती रवैया अपनाती है और पुलिस को “गैर-सांप्रदायिक” बनाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, जैसे कि अल्पसंख्यक समाज से और लोगों की पुलिस में भर्ती करना। ऊपर उल्लेखित CHRI और क्विल फाउंडेशन द्वारा किए गए शोध में 25 सेवानिवृत्त मुसलमान पुलिस अधिकारियों के किए गए इंटरव्यू से यह बात सामने आई कि “पुलिस फोर्स के भीतर भी मुसलमानों को अपनी पहचान के आधार पर पक्षपात का सामना करना पड़ता है, जो कि संस्थागत पक्षपात को दर्शाता है।”
***
पिछले साल 13 दिसंबर, 2019 की दोपहर को एस.एस.पी. आकाश कुल्हाड़ी के नेतृत्व में 50 पुलिस कर्मियों ने 10,000 विद्यार्थियों के समूह को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट पर रोक लिया। ये विद्यार्थी, जो कि ज्यादातर मुसलमान थे, अलीगढ़ जिला मुख्यालय की तरफ हाल ही में पारित किए गए CAA कानून के विरोध में रैली कर रहे थे। एस.एस.पी. ने विद्यार्थियों को संबोधित किया और उन्हें चेतावनी दी कि शहर की कानून व्यवस्था न बिगाड़ें।
उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, “संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से किए गए विरोध प्रदर्शन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे तो मुझे जरूरी कार्यवाही करनी पड़ेगी।” विद्यार्थियों ने जिला मुख्यालय को घेरने के अपने निर्णय को बदल दिया और विद्यार्थी नेताओं ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ही अपने भाषण दिए। एस.एस.पी. का विद्यार्थियों को दिया गया भाषण थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो गया।
वह रैली उस समय एक हफ्ते तक चलने वाले आन्दोलन का हिस्सा थी, जो CAA और NRC के विरोध में 7 दिसम्बर को शुरू हुआ था। विद्यार्थियों की बड़ी संख्या CAA और NRC को मुसलमानों को भारतीय समाज में भागीदारी से बेदखल करने का माध्यम मान रही है। रैली के एक दिन पहले सामाजिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव और डॉ. कफील खान ने विद्यार्थियों को धरना प्रदर्शन की जगह पर संबोधित किया। सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद योगेन्द्र यादव के साथ आने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर न आ पाने के कारण उन्होंने उनकी जगह खान को बुलाने का सुझाव दिया।
11 दिसम्बर को जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता शरजील इमाम और अफरीन फातिमा दो और बहुजन कार्यकर्ताओं के साथ अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के समर्थन में अलीगढ़ आए। जिस दिन शरजील पहुंचे, उस दिन मेरे पिता को एस.एस.पी. द्वारा यूनिवर्सिटी के उप-कुलपति तारिक मंसूर की मौजूदगी में बुलाया गया। उन्हें मुझे ‘काबू’ में करने के लिए बोला गया और मुझे आंदोलन से पीछे हटने की हिदायत दी गई। अगर यह बात नहीं मानी गई तो एस.एस.पी. ने चेतावनी दी कि मुझ पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्यवाही होगी।
15 दिसम्बर की शाम के 6:15 बजे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की अत्यधिक निगरानी से लेस लाइब्रेरी कैंटीन में दिल्ली में हुई जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थियों पर पुलिस बर्बरता पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। उनमें से ज्यादातर उत्तेजित थे और धरने की मांग कर रहे थे। अगले 45 मिनट में हजारों विद्यार्थी यूनिवर्सिटी गेट पर दिल्ली पुलिस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में नारे लगाते हुए जुड़ गए।
अगले 15 मिनट में पुलिस ने असाल्ट राइफल और पेलेट गन से विद्यार्थियों पर हमला बोल दिया और उनके ऊपर आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड की बौछार कर दी। पुलिस और रैपिड एक्शन फ़ोर्स मिल कर चार घंटे तक यूनिवर्सिटी परिसर के अन्दर विद्यार्थियों पर हमला करते रहे। इस हमले में साठ से भी ज्यादा विद्यार्थी कई तरह की चोटों और सदमे का शिकार हुए। क्विल फाउंडेशन और HRLN द्वारा जारी की गई तथ्य-खोजी रिपोर्ट में इस घटना को “शांतिप्रिय ढंग से विरोध कर रहे अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के सामने चौंका देने वाली पुलिस बर्बरता का प्रदर्शन” माना है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पुलिस की कार्यवाही सिर्फ निर्दयी ही नहीं, बल्कि बदले की भावना से भी भरी थी, जिसका उद्देश्य “(मुसलमान) विद्यार्थियों को उनकी जगह दिखाना था।”
AMU आने के कुछ ही दिन बाद कफील खान के खिलाफ मुकदमा जारी कर दिया गया। 29 जनवरी को मुंबई में उत्तर प्रदेश टास्क फ़ोर्स द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दो हफ्ते बाद उन पर भयावह NSA का मुकदमा थोक दिया गया। यह भी ध्यान देने की बात है कि यादव ने खान के साथ ही विद्यार्थियों को संबोधित किया था, पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक पुलिस वाले ने मेरे मित्र को बताया कि “हम को खान से कोई मतलब नहीं है। वो तो बाबा (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हुए) ने आदेश दिया, इसलिए उसको गिरफ्तार किया।”
15 दिसम्बर की हिंसा के बाद मुझे मेरे मित्रों द्वारा पुलिस से बचने के लिए सचेत किया गया। इसके कारण मैंने चार अन्य साथियों के साथ अलीगढ छोड़ दिया। एक हफ्ते बाद मैंने अपनी फोटो आज तक पर देखी, जहां एंकर चित्रा त्रिपाठी बता रहीं थीं कि अलीगढ एस.एस.पी. ने मुझे अलीगढ़ हिंसा का मास्टरमाइंड घोषित किया है। अलीगढ में पूर्व छात्र और जाने-माने सामाजिक कार्यकर्त्ता मोहम्मद आमिर मिंटी और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जारी रहा। 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आमिर को अस्पताल में गरीबों को खाना बांटते समय गिरफ्तार कर लिया। उन्हें और मुझे भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 153, 188, 189, 307, 332, 336, 504 और धारा 506 आदि के तहत आरोपी बनाया गया। वर्तमान में मुझ पर 3 अलग-अलग मुकदमों में 70 धाराएं लगाई गईं हैं।
***
मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की पड़ताल करने के लिए बनी जस्टिस राजिंद्र सच्चर के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने मुसलमानों के विरूद्ध पुलिसिया पक्षपात को इन शब्दों में बयान किया है: ”मुसलमानों के प्रति पुलिस का मनमाना रवैया चिंतनीय है। मुसलमान एक हीन भावना के साथ रहते है, क्योंकि ‘हर दाड़ी वाला व्यक्ति ISI एजेंट माना जाता है’; जब भी कोई हादसा होता है, तुरंत पुलिस द्वारा मुसलमान लड़के उठा लिए जाते हैं। मुसलमानों के एनकाउंटर तो आम बात है।”
उक्त उल्लेखित क्विल और CHRI के शोद्ध में शोधकर्ताओं ने माना कि “यह आम धारणा सामने आई है कि पुलिस मुसलमान इलाकों को आपराधिक या आतंकवादी गतिविधि के गढ़ के रूप में देखती है, जो समुदाय के तरफ निरंतर संदेह और अविश्वास को कायम रखता है। हमने जितने भी शहरों का दौरा किया, उन सब में बार-बार मुसलमान क्षेत्रों को 'छोटे पाकिस्तान' के रूप में चित्रित करने की शिकायत सुनी, जिससे पता चलता है कि मुसलमान समुदाय की समझ क्या है और उसे पुलिस द्वारा कैसे देखा जाता है। यह अपराध-पीड़ित इलाके से आने के रूप में देखे जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन इलाकों से आए लोगों को संभावित रूप से राष्ट्र-विरोधी के रूप में देखा जाता है, मुख्यधारा से अलग और इस एहसास के साथ कि आपका इलाका हमेशा संदिग्ध है।”
28 दिसम्बर को मेरठ एस.पी. अखिलेश नारायण कैमरे पर CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को ‘पाकिस्तान जाने’ की धमकी देते हुए पकड़े गए थे। उसी समय दर्जनों मासूम मुसलमानों की हत्या हुई, इतने ज्यादा की सबका अलग-अलग नाम लिखना भी यहां संभव नहीं है, हजारों गिरफ्तार कर लिए गए और एक लाख से ज्यादा मुख्यतः मुसलमानों पर CAA और NRC का विरोध करने के ‘जुर्म’ में उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज हुए, जिसके विरोध में नागरिकों के समूहों ने राष्ट्रीय राजधानी में धरना प्रदर्शन किया।
इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस कांस्टेबल को एक लड़की द्वारा शांति के चिह्न के रूप में गुलाब दिए जाने वाला ‘मार्मिक’ फोटो वायरल हो गया। हालांकि वह एक दयालु भाव था, पर साथ ही मानव अधिकार का उल्लंघन करने को शांत रूप से सहमती भी थी। पुलिस कांस्टेबल, जिसे वो गुलाब मिला, अकेला व्यक्ति है, जबकि पुलिस एक संस्था है। बात यह है कि पुलिस एक संस्था के रूप में अपने व्यवहार में सांप्रदायिक और मुसलमान विरोधी है। जब यह माना जाएगा तभी पुलिस संस्था में जरूरी सुधारों के बारे में सोचा जा सकता है।