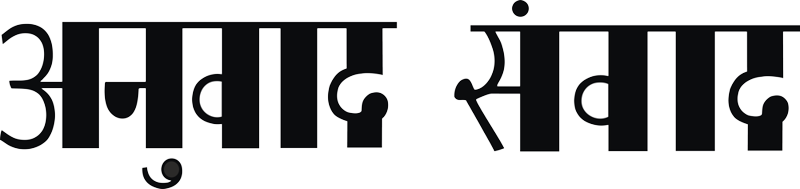Listen to this story
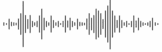
पटचित्र: पीआ अलिजी हजारिका
अनुवाद: अक्षत जैन और अंशुल राय
स्तोत्र: The Caravan
मेरी पैदाइश और परवरिश हिन्दी भाषी समाज में हुई। मेरे माता-पिता, भाई-बहन, कज़िन और दोस्त वगैरह सब हिन्दी भाषी थे। बिहार के एक छोटे से कस्बे की दलित बस्ती में, जहां मैंने अपना बचपन गुज़ारा, वहां भी सब हिन्दी भाषी ही थे। आज भी उन सबसे मैं सिर्फ हिन्दी में बात करता हूं। दस वर्षों तक मैंने बिहार स्टेट बोर्ड की पाठ्यचर्या पर चलने वाले हिन्दी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की। पटना में दो साल इंटरमीडिएट कोर्स करने के बाद मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए कोस्टल कर्नाटक के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां क्लास अंग्रेजी में लगती थी और कैंपस में छात्र उसी भाषा में बात करते थे। स्थानीय लोग कन्नड या तुलु भाषाओं में बात करते थे। मुझे दोनों ही भाषाएं ठीक से नहीं आतीं थीं। अपने आपको यूं असहाय पाकर मैं अपनी अंग्रेजी सुधारने पर कड़ी मेहनत करने लगा।
मेरी उम्र 28 वर्ष की हो गई थी जब मैंने डॉक्टर अंबेडकर की किताब जाति प्रथा का उन्मूलन अंग्रेजी में पढ़ी। उनके काम के साथ यह मेरा पहला परिचय था। उन्होंने बड़ी बेबाकी से उस जातिगत अपमान को व्यक्त किया और समझाया, जिसको जिंदगी भर मैंने खुद भोगा और देश भर में पत्रकारिता करते हुए दूसरे दलितों को भोगते देखा। मैंने अंबेडकर का लिखा सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ा है, जिस भाषा में वह लिखते भी थे। और यह अंग्रेजी ही है, जिसमें मैंने ज्योतिराव फुले, पेरियार और मैल्कम एक्स के बारे में भी जाना है। इन्हीं जैसे लोगों के कारण मैं जाति-विरोधी विचारधारा, प्रगतिशील पॉलिटिक्स और असमानता के खिलाफ होने वाले संघर्ष के इतिहास को समझ पाया और अपने जेहन में उतार पाया।
हर थोड़े दिनों में हिन्दी लादने को लेकर जब छिटपुट विवाद उठते हैं तब मुझे याद आता है कि मैंने कौन-सी भाषा में क्या सीखा है। इस बार हंगामा ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बरपा, जिसके तहत हिन्दी, अंग्रेजी और एक अन्य क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करना देश में सभी छात्रों के लिए अनिवार्य किया जाना है। गैर-हिन्दी राज्यों में जबरन हिन्दी पढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध उठने के कारण सरकार को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। अब इस ताज़े झगड़े के विजेता घुसपैठ के खतरे को खदेड़ कर खुशी से आराम फरमा रहे हैं, लेकिन मैं उनके जश्न में शामिल नहीं हो सकता। मुझे अभी भी उन सैकड़ों लोगों की चिंता है, जो हिन्दी भाषा में जीते-सोचते हैं, आखिर उनके पास हिन्दी के अलावा क्या विकल्प है?
एक वक्त था जब मैं आश्चर्य से सोचा करता था कि हिन्दी के माध्यम से मेरे अंदर जागरूकता पैदा क्यों नहीं हो सकी। लेकिन उस भाषा के बारे में मुझे जितनी ज्यादा जानकारी मिलती है, उतना मेरा आश्चर्य कम होता जाता है। मुझे अब इस बात का इल्म है कि हिन्दी भाषा के साथ बड़े होने के कारण मेरी सिर्फ अंबेडकर से भेंट ही विलंबित नहीं हुई, बल्कि हिन्दी ने मुझे इंसाफ और बराबरी जैसी अवधारणाओं को भी समझने से रोका। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को हिन्दी के माध्यम से समझना बिल्कुल नामुमकिन है—आखिर अंबेडकर का हिन्दी अनुवाद हुआ है और कुछ लेखक एवं चिंतक हिन्दी में ही सामाजिक न्याय के बारे में लिखते भी हैं। बात यह है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में हिन्दी भाषी शिक्षा के साथ हिन्दी भाषी घर में बड़े होने के कारण मेरे लिए अंबेडकर या अन्य सामाजिक न्याय पर लिखने और विचार करने वालों को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। ये संयोग की बात नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे, हिन्दी भाषा किसने और किस उद्देश्य से ईजाद की, किसने और किस नियत से विकसित की और फैलाई और उसके ऊपर आज भी किसकी छाप सबसे गहरी है।
आज हम जिसे हिन्दी साहित्य कहते हैं उसके प्रारम्भिक लेख ब्रज, बुन्देली, अवधि, कन्नौजी, खड़ी बोली, मारवाड़ी, मगही, छत्तीसगढ़ी और इस तरह की कई भाषाओं में लिखे गए। इनमें से अधिकतर भाषाएं अब हिन्दी में समाहित हो चुकी हैं। नागरी लिपि में लिखी हुई जिस भाषा को आज हम हिन्दी के नाम से संबोधित करते हैं, उसका आविष्कार हाल ही में हुआ है। आधुनिक हिन्दी साहित्य के पितामह के रूप में प्रसिद्ध कवि भारतेन्दु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था।
इतिहासकार सुमित सरकार ने अपनी किताब आधुनिक भारत: 1885–1974 में लिखा है कि साहित्यिक हिन्दी ‘हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन से बारीकी से जुड़ा कृत्रिम आविष्कार है।’ सरकार बताते हैं कि भारतेन्दु ने ‘स्वदेशी सामग्री को इस्तेमाल करने, गौ-हत्या पर रोक लगाने और प्रशासन में उर्दू के एवज हिन्दी का उपयोग करने की दलीलों को जोड़कर पेश किया था।’ उसी अवधि में इतिहासकार और भाषाविद् शिवप्रसाद एक दूसरी संपर्क भाषा को बढ़ावा दे रहे थे, जिसका नाम था हिन्दुस्तानी। जहां भारतेन्दु की हिन्दी में संस्कृत शब्दों का जोर था, वहीं शिवप्रसाद ऐसी भाषा की वकालत कर रहे थे जो उस समय में प्रचलित भाषाओं के करीब हो। हिन्दी के पक्षपातियों को हिन्दुस्तानी से खास चिढ़ इसलिए थी क्योंकि उसमें उर्दू के बहुत से तत्व शामिल थे।
शुरुआत से ही हिन्दी में ब्राह्मणवादी और सांप्रदायिक प्रवृत्तियां रहीं हैं। बाद में हिन्दी को प्रमुखता देने की मांग राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा उठाई गई। हालांकि तब भी यह मांग निहायती विवादास्पद थी। वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया, जो महाराष्ट्र के महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में अध्यापक रह चुके हैं, बताते हैं कि भारतेन्दु की भाषा का विस्तार इसलिए हो सका, क्योंकि वह ब्राह्मण प्रभुत्व में उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन और प्रशासन को बहुत पसंद आई। उनका कहना है कि प्रभुत्व रखने वाली जातियों को इस संस्कृत से प्रभावित हुई भाषा में ऐसा साधन नजर आया जिससे वे समाज में अपना वर्चस्व बढ़ा सकें। बेशक संस्कृत का पहले भी बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल किया गया था। चमड़िया ने हिन्दी को ‘वर्चस्व की धारा’ के रूप में वर्णित किया। उनका कहना है कि आज हमारे समाज में उन्हीं लोगों का प्रभुत्व है जो हिन्दी को नियंत्रित करते हैं।
स्कूल में हमको मोहनदास गांधी के बारे में विस्तार से बताया गया और उनकी आत्मकथा भी पढ़वाई गई। उससे हम शाकाहार और ब्रह्मचर्य जैसे ब्राह्मणवादी मूल्यों को सफलता की कुंजी मानने लगे। अंबेडकर का बस हमारी सामान्य ज्ञान की कक्षाओं में कुछ पंक्तियों में जिक्र हुआ और वह भी केवल संविधान निर्माता के तौर पर।
नए नोट्स शुरू करते समय विद्यार्थियों का नोटबुक के पन्ने के शीर्ष पर ‘श्री गणेश’ लिखना आम बात थी। ऐसा इसलिए, क्योंकि हिन्दू अपनी मान्यताओं में गणेश को शुभारंभ का भगवान मानते हैं। बसंत पंचमी में हम अपनी नोटबुकों को सरस्वती के चरणों में रख देते। हमारा विश्वास था कि ज्ञान की देवी हमारा होमवर्क करने में मदद करेगी। हमने स्कूल में ज्ञान को आस्था के बराबर मानना और ताकत के सामने नतमस्तक होना सीखा। जब भी मैं देर से सोकर उठता तो मेरे पिता मुझे स्कूल में सिखाई गई कविता याद दिलाते: ‘उठो सवेरे, रगड़ नहाओ / ईश विनय कर शीश नवाओ / रोज बड़ों के छूओ पैर / कभी किसी से करो ना बैर।’
प्राथमिक विद्यालय में मेरे हिन्दी के अध्यापक उपाध्याय थे, एक ब्राह्मण। उच्च विद्यालय में पाठक, वे भी ब्राह्मण। उपाध्याय सर पेशेवर पुजारी भी थे और बसंत पंचमी के दिन हमारे स्कूल में सरस्वती की पूजा कराते थे। पाठक सर ने हमें बताया कि संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है और त्रिकोणमिति वैदिक काल में ब्राह्मणों ने ईजाद की थी, जो त्रिकोणीय हवन कुंडों का इस्तेमाल करते थे।
हमको पढ़ाया जाता था कि गुप्त काल में समाज वर्णाश्रम धर्म के आधार पर स्थापित था, जिसका मतलब है कि लोगों का श्रेणीकरण जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत में होता था। हमें बताया गया कि यह भारत का स्वर्ण युग था। कुंवर सिंह एक जमींदार था, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विरोध किया और जिसके नाम पर भारत में 1970 और 80 के दरमियान जमींदारों ने विद्वेषपूर्ण लोक सेना बनाई। हमारे स्कूल में इस व्यक्ति को हीरो की तरह पेश किया गया। जबकि अंग्रेजों के खिलाफ 1780 के दशक में लड़ने वाले आदिवासी नेता तिलका मांझी का कभी जिक्र तक नहीं किया गया।
बाबरी विध्वंस के बारे में हिन्दी मीडिया ने मेरे आस-पास के सभी लोगों को विश्वास दिलाया कि विवाद असल में राम की जन्मभूमि का ही है। मैं भी उस वक्त भगवा झंडा पकड़े जुलूस में शामिल होने के लिए सड़क पर उतर आया था, उस हिन्दू धर्म की गर्व से रक्षा करने, जिसने मुझे और मेरी कौम को अछूत का दर्जा दिया। मेरे दिमाग में यह सवाल उठा ही नहीं कि आखिर मैं बस्ती में क्यों रहता था, जबकि जुलूस का नेतृत्व करने वाले—जैसे कुर्मी ओबीसी, बाभन ब्राह्मण, ठाकुर राजपूत—बड़े घरों में रहते थे। मेरे आस-पड़ोस में ताड़ी निकाल कर बेचने वाले पासी और कपड़े धोने वाले धोबी रहते थे, जो कपड़े ढोने के लिए गधे रखते थे।
प्रभुत्व रखने वाली जातियों के लोग हम को ‘नीच जात’ या हरिजन या हिन्दी में पाए जाने वाले सैकड़ों अपशब्दों से संबोधित करते और यह सब हम मृदुलता से स्वीकार कर लेते। हर होली पर स्थानीय म्यूजिक इंडस्ट्री में अछूतों को गाली देने वाले नए गाने बनाए जाते। हमारे मोहल्ले के यादव, कुर्मी, ठाकुर और ब्राह्मण इन गानों को कान फाड़ वॉल्यूम पर बजाकर नाचते और मटका फोड़ने के लिए पिरामिड बनाते।
ज़िंदगी के शुरुआती समय में हिन्दी साहित्य पढ़ने से मेरे भीतर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हिन्दी साहित्य के अधिकतर दिग्गज प्रभुत्व रखने वाली जातियों के मर्द थे और आज भी हैं। एक लेखक हैं, जिनका नाम बार-बार यह दलील देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हिन्दी साहित्य में भी जाति उत्पीड़न और सामाजिक अन्याय के ऊपर चर्चा हुई है। प्रेमचंद की कई कहानियां मैंने स्कूल में पढ़ीं और बहुत सारी स्कूल के बाद, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उनसे मेरा या किसी और का सशक्तिकरण हो सकता है।
प्रेमचंद, जो कि कायस्थ थे, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रारंभिक सदस्य थे। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शरद जैसवाल ने प्रेमचंद द्वारा स्थापित की गई साहित्यिक पत्रिका हंस की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह ‘सामाजिक न्याय की आवाज़’ है। प्रेमचंद की कहानी ‘ठाकुर का कुआं’ को खासा जाती-विरोधी माना जाता है। उस कहानी में एक बीमार दलित पुरुष को स्वच्छ पानी की जरूरत होती है और उसकी पत्नी गंगी के पास ठाकुर के कुएं से पानी लाने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता। जब गंगी छिपते-छिपाते ठाकुर के कुएं से पानी ले रही होती है तब ठाकुर के घर का दरवाजा खुल जाता है और वह बिना पानी लिए ही दबे पांव घर भाग आती है। इस कहानी से ना तो व्यवस्थित उत्पीड़न के बारे में कुछ समझ आता है और ना ही इसको पढ़ के उत्पीड़ितों को विरोध करने की कोई प्रेरणा मिलती है। ठाकुर को व्यक्तिगत तौर पर बुरा आदमी बताया गया है, ना कि ऐसे समाज का अभिन्न हिस्सा जो उत्पीड़ित जातियों के शोषण पर टिका है। प्रेमचंद दलित जोड़े को बदनसीब बताता है क्योंकि वे ठाकुर के कुएं से पानी नहीं ले पाए।
‘कफन’ प्रेमचंद की एक और कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दलित उत्पीड़न को दर्शाती है। इसके नायक दो बेतहाशा गरीब चमार हैं, बाप और बेटा। एक रात वे अपने घर के बाहर भुने हुए आलू खा रहे होते हैं जबकि बहु घर के अंदर प्रसव में छटपटा रही होती है। देखभाल के अभाव में औरत सुबह तक मौत के घाट उतर जाती है। बाप और बेटा मैयत के लिए गांव के ज़मींदार और साहूकारों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसकी शराब पी जाते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं—‘यह तो उनकी प्रकृति थी।’ मेरी समझ में तो कहानी दलितों के बारे में उन्हीं धारणाओं को बढ़ावा देती है जो आम तौर पर प्रभुत्व वाली जातियों में पाई जाती है: कि दलित बेवड़े, अक्षम, आलसी और लालची होते हैं।
चमड़िया और जैसवाल प्रेमचंद पर बनी मेरी समझ से असहमत हैं। चमड़िया ने दलील पेश की कि प्रेमचंद ने हिन्दी साहित्य में सकारात्मक भूमिका निभाई, खासकर अपनी अवधि, या 20वीं सदी की शुरुआत के बौद्धिक परिवेश के संदर्भ में। जैसवाल ने जोड़ा कि आर्थिक वर्ग और सामाजिक न्याय को अपनी लेखिका का आधार बनाने वाले वामपंथी लेखक 1960 और 1970 के दशकों तक ही आए। इसके बावजूद चमड़िया ने माना कि हिन्दी साहित्य में दलित और आदिवासी आवाजों को ना के बराबर जगह मिली है।
चमड़िया ने दलित कवि हीरा डोम का उदाहरण दिया। उनकी भोजपुरी में लिखी कविता, अछूत की शिकायत, सरस्वती नामक पत्रिका में 1924 में प्रकाशित हुई। इस कविता को दलितों पर लिखी जाने वाली पहली कुछ कविताओं में से एक माना जाता है। चमड़िया का कहना है कि वह कविता असामान्य है; जिस तरह की लिखाई को वह दर्शाती है, वह कभी हिन्दी साहित्य की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाई और ना ही उसकी अलग शैली विकसित हो पाई।
अछूत की शिकायत का एक अंश है:
हडवा मसुइया के देहइया है हमनी कै,
ओकरे के देहिया बभनो के बानि।
ओकरा के घरे-घरे पुजवा होखत बाजे,
सगरे इलकवा भईले जजमानी।
हमनी के इनरवा के निगिचे न जाइले जा,
पांके में से भरि भरि पिअतानी पानी
पनही से पिटी-पिटी हाथ गोड तुडि दैलें
हमनी के इतनी काहे के हलकानि!
(ब्राह्मण का शरीर भी हमारे जैसा ही मांस और हड्डी का बना है, लेकिन जहां उसकी हर घर में पूजा होती है क्योंकि पूरा इलाका उसकी खातिर करता है, वहीं हमें कुएं के पास भी जाने को नहीं मिलता और मिट्टी से हमें पीने का पानी निकालना पड़ता है।)
हाल में राजनीति में प्रवेश करने वाले हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार शहनवाज़ आलम बताते हैं कि हिन्दी साहित्य गांवों के रोमानीकरण में डूबा है। उनका कहना है कि वामपंथ के प्रसिद्ध कवि सुमित्रनंदन पंत की लिखाई में भी ‘ग्राम्य जीवन सादा और सरल होता है’ की तरह के वाक्य खूब मिलते हैं। ब्राह्मण होने के नाते पंत को कभी दलितों के जैसे गांव के बाहर नहीं रहना पड़ा होगा, रोजमर्रा की ज़िंदगी हिंसा के डर में नहीं गुज़ारनी पड़ी होगी और ना ही कभी किसी ने उसे सामूहिक कुंओं या सड़कों को इस्तेमाल करने से रोका होगा, जैसे कि आज भी बहुत जगहों पर दलितों को रोका जाता है।
पत्रकारिता कॉलेज में पहली बार मुझे यह बताया गया कि अंबेडकर का लिखा संविधान गंभीर अध्ययन के योग्य है, हालांकि अंबेडकर खुद वहां भी इस योग्य नहीं माने गए। इससे मेरे दिमाग का एक द्वार तो खुला—मुझे समझ आया कि ज्ञान का संबंध सिर्फ धर्म से ही नहीं बल्कि विवेक और तार्किकता से भी हो सकता है। फिर भी, मेरी दुनिया की समझ कच्ची होने के कारण संविधान पढ़कर सरकार की अच्छाई और शासन कला पर मेरा भरोसा और दृढ़ हो गया। कश्मीर पर कोई भी विवाद छिड़ने पर मैं सरकार और सेना की तरफदारी करना अपना धर्म मानता। तर्क के तौर पर मैं वही चीजें जस की तस दोहराता जो न्यूज चैनलों और अखबारों में देखता-पढ़ता। मुझे सच में विश्वास था कि सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट माओवादियों को मारने के लिए चलाया था। आदिवासी ज़िंदगियों पर उसका कितना भयंकर असर पड़ा उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर शैलेश कुमार दिवाकर ने उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के अपने निजी संघर्ष का उदाहरण दिया। बिहार और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में पढ़ते वक्त उनका भी कभी अंबेडकर या अम्बेडकरवादी विचारधारा से सामना नहीं हुआ। यह सिर्फ तब बदला जब वह 2000 के दशक की शुरुआत में जेएनयू में मास्टर्स की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे। एक प्रोफेसर ने उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरवादी आंदोलन पर ऑप्शनल पेपर शुरू किया। उसके बाद दिवाकर ने जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुस्तकालयों में अंबेडकर की किताबों को ढूंढा मगर उनके हाथ कुछ ना लगा। उनको अपने एक दोस्त से कहकर अंबेडकर की किताबें महाराष्ट्र से मंगवानी पड़ीं, चूंकि वहां वे ज्यादा आसानी से मिल जाती थीं। स्वयं दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक बनने के बाद जब दिवाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रम का संशोधन करने वाली कमिटी के सदस्य बने, तो उन्होंने अंबेडकर के विचारों पर पेपर शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उनकी दलील थी कि गांधी को व्यापक रूप से अलग-अलग शाखाओं में पढ़ाया जा रहा है लेकिन अंबेडकर के ऊपर ना के बराबर ध्यान दिया गया। कमिटी से अपना प्रस्ताव स्वीकार करवाने के लिए उन्हें आंदोलन करने की धमकी देनी पड़ी।
हैदराबाद में कम्यूनिटी रिपोर्टर और भुवनेश्वर में क्राइम रिपोर्टर का काम करते-करते मेरा सरकार से धीरे-धीरे विश्वास उठता गया। दलितों से भरी बस्तियों के विकास के लिए जारी फंड हेरा फेरी करके प्रभुत्व वाली जातियों के लोगों से भरे अमीर इलाकों में खर्च दिए जाते। अधिकतर दलित और आदिवासी ही हैं जिनको पीटा जाता है, जिनका बलात्कार और कत्ल होता है, जो धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, जिनको अपने घर और ज़मीनों से वांछित कर दिया जाता है, जो पुलिस स्टेशनों, न्यायालयों और मानवाधिकार आयोगों में खड़े होकर मिन्नतें मांगते हैं। जाति आधारित अत्याचार बाकी किसी भी और अन्याय से ज्यादा होते हैं लेकिन फिर भी इनकी कहानियां सबसे कम रिपोर्ट की जाती हैं और इनकी चर्चा भी सबसे कम होती हैं। लेकिन सरकार और दुनिया पर विश्वास के टूटने से मैं और ज्यादा अस्त-व्यस्त हो गया, क्योंकि मैं वास्तविकता के सारे अलग-अलग बिंदुओं को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देख पा रहा था।
जनवरी 2016 में पीएचडी कर रहे दलित छात्र रोहित वेमुला को जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, तब आखिरकार मैंने जाति को समझने का गंभीर प्रयास शुरू किया। भुवनेश्वर में मुझे अंबेडकर की किताब जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं मिली। हैदराबाद से एक दोस्त को भेजनी पड़ी। आखिरकार, अंबेडकर ने उन सब चीजों का मतलब स्पष्ट किया जो मैंने देखीं और सही हैं। उनको पढ़ने के बाद मैं उन कश्मीरियों का दर्द समझ सका जिनको हथियार से लेस सेनानियों की निगरानी में ज़िंदगी काटनी पड़ती है। मैंने उन आदिवासियों की पीड़ा समझी जिनको अपनी ज़मीनों से अर्धसैनिक बलों द्वारा खदेड़ दिया जाता है। मैंने जाति व्यवस्था का दूसरा पहलू जाना। मुझे ज्ञात हुआ कि गुप्त साम्राज्य के समय बौद्धिक धर्म के ऊपर हिंसक ब्रह्मणवाद अपना वर्चस्व जमा रहा था। मुझे लगा कि काश यह सब मुझे स्कूल और कॉलेज में सिखाया गया होता।
दिल्ली में अम्बेडकरवादी किताबों की दुकान के मालिक सुल्तान सिंह गौतम को यह जानकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि अंबेडकर की लिखी हुई या अंबेडकर के बारे में लिखी हुई किताबें ढूंढने के लिए मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा। गौतम ने मुझे बताया कि अंबेडकर के ऊपर हिन्दी में लिखी गई पहली किताब 1946 में रामचन्द्र बनौधा नाम के दलित ने प्रकाशित की थी। अगले कुछ दशकों में कुछ और किताबें निकलीं, लेकिन उनका प्रसार चंद दलित बुद्धिजीवियों तक ही सीमित रहा। 1970 के दशक में महाराष्ट्र की सरकार ने अंबेडकर के सैकड़ों अप्रकाशित भाषणों और लेखों को मूल अंग्रेजी में निकालना शुरू किया तो अंबेडकर की विरासत को थोड़ा बढ़ावा मिला। अंबेडकर की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आखिरकार 1991 में केन्द्रीय सरकार ने उस संकलन का हिन्दी सहित 13 हिन्दुस्तानी भाषाओं में अनुवाद करवाने का निर्णय लिया। लेकिन, गौतम ने बताया कि यह करने का दारोमदार किसी प्रकाशक ने नहीं लिया, फिर चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक। यहां तक कि केन्द्रीय सरकार के खुद के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। आखिर में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी ली, और 1990 के दशक के मध्य में अंबेडकर के लेख और भाषण का पहला संकलन हिन्दी में प्रकाशित हो सका।
इन अनुवादित संस्करणों को न तो पुस्तकालयों में आसानी से जगह मिली और ना ही किताबों की दुकानों में। गौतम ने बताया कि लाइब्रेरियन और दुकानदार इन किताबों को ऐसी जगह रखते थे, जहां वे किसी को न मिल सकें, जिससे कि बिक्री और पाठकों के ऑडिट करते समय यह संदेश मिले कि इन किताबों में किसी की रुचि नहीं है। इस आधार पर उपलब्ध संस्करण हटा दिए गए और नई कॉपियां एवं प्रकाशन कभी ऑर्डर ही नहीं किए गए।
मेरी तरह दिवाकर को भी यही लगता है कि हिन्दी में शिक्षा पाने के कारण उनको सामाजिक न्याय का इल्म बड़ी देर से हुआ। उन्होंने यह भी दलील दी कि हिन्दी मूल तौर पर जातिवादी, नस्लवादी और वर्चस्ववादी भाषा है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक गाने के बारे में बताया जो उनकी बेटी घर पर गुनगुनाया करती थी: नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। दिवाकर ने बताया कि हिन्दी में चोरों का काला होना जरूरी था।
हिन्दी अभिशप्त विरासत की देन है। ज़ाहिर है कि और भी बहुत सी भाषाएं ऐसी ही हैं। अंग्रेजी का इतिहास उपनिवेशवाद से अभिशप्त है, और वह भाषा खुद भी वर्चस्ववाद और जातिवाद का साधन रह चुकी है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी मुझे ऐसी चीजें दिखा पाई जो हिन्दी मुझसे छिपा कर रखती है, क्योंकि जो लोग हिन्दी को नियंत्रित करते हैं, जो उसके इतिहास, शब्दावली, साहित्य और पाठ्यक्रम को आकार देते हैं, वे अंग्रेजी का उस हद तक नियंत्रण नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी हिन्दी का स्थान ले, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं नहीं चाहता कि हिन्दी किसी और भाषा का स्थान ले। लेकिन हर भाषा तब ही अपना काम श्रेष्ठता से कर रही होती है जब वह दिमाग बंद नहीं करती बल्कि खोलती है। एक दिन हिन्दी भी उन सैकड़ों करोड़ों लोगों के दिमाग खोलने में सक्षम हो पाएगी जो उसको बोलते, उसमें सोचते और उसी में अपना जीवन काटते हैं। अगर यह हमें सच करना है तो हमें हिन्दी के अतीत और वर्तमान का ईमानदारी से आकलन करना पड़ेगा और यह सवाल उठाना पड़ेगा कि हम उससे भविष्य में क्या चाहते हैं?
(इस लेख को एडिट करने में शहादत खान ने मदद की है)