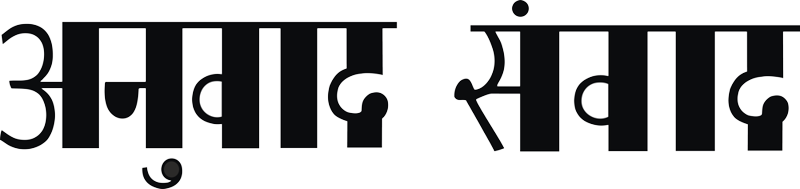Listen to this story
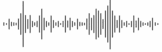
पटचित्र: Smithsonian Institute
अनुवाद: मज़ाहिर हुसैन
स्त्रोत: The Nation
क्रिसमस, 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद का पहला दिन।
मैं मजबूरी की भावना को अपने अंदर समेटे खिड़की से बाहर एकटक देख रही हूं। तभी एक दोस्त और साथी फ़नकार मुझे छुट्टियों की बधाई देने के लिए कॉल करता है। वह मुझसे पूछता है, “तुम कैसी हो?” और मैं साधारणतः दिए जाने वाले जवाब—“हां, मैं ठीक हूं, और तुम?” के बजाए सच बोल देती हूं: “मैं ठीक नहीं हूं, मैं केवल अवसादग्रस्त ही नहीं हूं, मुझसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा है, मैं लिख नहीं पा रही हूं: ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सुन्न हो गई हूं, जो उपन्यास मैंने शुरू किया था उसमें आगे कुछ लिख ही नहीं पा रही हूं। इससे पहले मैंने कभी भी इस प्रकार की मनोदशा का सामना नहीं किया, लेकिन यह चुनाव....” तब जब मैं अपनी बात को उसके सामने और विस्तार से रख ही रही थी, उसने मेरी बात काट दी और तेज़ आवाज़ में मुझसे कहा: “नहीं! नहीं! यही वो वक़्त है जब फ़नकारों को काम पर लग जाना चाहिए। तब नहीं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब जब खौफ बरपाया जा रहा हो। यही हमारा काम है!”
बाकी बची सुबह मैं अपने आपको मूर्ख महसूस करती रही, खासकर तब जब मैंने उन सारे फ़नकारों को याद किया जिन्होंने अपना काम गुलाग, जेल और अस्पतालों में जारी रखा था; जो तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद अपना काम करते रहे थे—तब जब उनका पीछा किया गया, उनको देश से निकाल दिया गया, गालियां दी गईं और मलामत किया गया। मैंने उनको भी याद किया जो फांसी पर लटकाए गए थे।
यह लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि इसमें केवल बीती शताब्दी के लोग ही नहीं बल्कि उससे पहले की शताब्दियों में रहे फ़नकार भी शामिल हैं। इन फ़नकारों के एक छोटे सैंपल में पॉल रोब्सन, प्रीमो लेवी, आई वेवेई, ऑस्कर वाइल्ड, पाब्लो पिकासो, डैशिएल हैमेट, वोले सोईंका, फ़्योदोर दोस्तोयेव्स्की, अलेक्जेंडर सोल्झेनित्सिन, लीलियान हेल्लमन, सलमान रुश्दी, हेरटा मुल्लर और वाल्टर बेंजामिन शामिल हैं। ऐसे सैकड़ों फ़नकार इस प्रकार की सुविस्तृत लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं।
आमतौर से क्रूर तानाशाह अपने शासन की शुरुआत में और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कला का सुविचारित और सुनियोजित विनाश करते हैं: अराजक गद्य वाली किताबों का जलाया जाना और सेंसर किया जाना, चित्रकारों, पत्रकारों, कवियों, नाटककारों और लेखकों का उत्पीड़न और उन्हें कैद किया जाना, इसी विनाशलीला का अभिप्राय है। यह उस तानाशाह द्वारा लिया पहला कदम है, जिसके द्वेषपूर्ण कार्य केवल बुद्धीहीनता और दुष्टता का परिचायक ही नहीं होते बल्कि उनके साथ एक बोध भी जुड़ा होता है। ऐसे तानाशाह एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि उनके द्वारा चलाई जाने वाली शोषण की कूटनीति शोषक वर्ग की शक्ति को बढ़ावा देने का काम करती रहेगी। उनकी योजना बहुत सरल है:
1. रोष को विवाद और यहां तक कि जंग में तब्दील करने के लिए माकूल दुश्मन—किसी “दूसरे”—का चुनाव करना।
2. कला द्वारा प्राप्त होने वाली कल्पना और इसी के साथ बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की समालोचनात्मक सोच को सीमाबद्ध करना या मिटा देना।
3. खिलौनों से, लूट के सपनों से और अतीत में हुए आघातों और अपमानों के खिलाफ बुने श्रेष्ठतर धर्म या दिलेर राष्ट्रवादी गौरव के मुद्दों से जनता को भटकाए रखना।
1930 के जर्मनी, 1940 के स्पेन, 2014 के सीरिया या श्वेतवादी दक्षिण अफ्रीका में द नेशन (पत्रिका) का पनपना तो दूर उसका अस्तित्व में आना भी मुश्किल होता। इसका कारण एकदम साफ है। इस पत्रिका का जन्म लिंकन की हत्या के साल 1865 के अमरीका में उस समय हुआ जब देश में राजनीतिक विभाजन अपने चरम पर था, या जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि जब खौफ बरप रहा था। लेकिन कोई भी राजकुमार या राजा या तानाशाह ऐसे किसी देश में सफलता से और निरंतर दखल नहीं दे सकता, जो प्रेस की स्वतंत्रता को सच में बेशकीमती माने। इसका यह मतलब नहीं कि उस समय कलम और ज़बान दोनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास करने वाले तत्व मौजूद नहीं थे, लेकिन ऐसे तत्व अपने प्रयासों में जीत हासिल नहीं कर पाए। पिछले 150 सालों से द नेशन अपने धमाकेदार, जांच-पड़ताल, समझदारी भरे लेखों के साथ समीक्षा, कविता, नाटक और कला आलोचना के क्षेत्र में लगातार काम करता आया है।
इस समकालीन दुनिया में, जिसमें हिंसात्मक आंदोलन, विनाशकारी युद्ध और खाद्य पदार्थों और अमन के वास्ते उठती चीखें आम हो गई हैं, अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बचाते ख़ौफ़ज़दा विस्थापित लोगों को शरण देने के लिए पूरे के पूरे निर्जन शहर बना दिए जा रहे हैं, सवाल उठता है कि हम (जो अपने आप को सभ्य मानते हैं) क्या करें?
इसका हल सेना बल द्वारा हस्तक्षेप या नज़रबंदी और हत्याओं की और झुकता नज़र आता है। इस दौर के भ्रष्ट राजनीतिक माहौल में किसी भी अन्य कार्रवाई को निर्बलता का प्रतीक समझा जाता है। मैं आश्चर्य से यह सोचती हूं कि “कमजोर” कहलाना इंतहाई और नाकाबिल-ए-माफी गुनाह कैसे हो गया है। क्या इसका कारण यह है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम दूसरों से, अपने देश से और अपने देश में बसे नागरिकों से कुछ इस प्रकार भयभीत हो गए हैं कि असली कमजोरियों को पहचान नहीं पा रहे हैं: जैसे बंदूकों की हर जगह और युद्ध की कहीं भी मांग करने में जो कायरता है? यह कैसा बड़प्पन, कैसा पुरुषार्थ है, जो अबोर्शन चिकित्सकों, स्कूल जाने वाले बच्चों, फुटपाथ पर चलने वाले लोगों और अपनी जान बचाते भागते काले युवाओं को गोलियों का शिकार बनाता है? अपनी जेब में, अपनी कमर पर, अपनी गाड़ी के ग्लव कम्पार्टमेंट में हत्या करने योग्य हथियार को रखने से किस प्रकार की शक्तिशाली या ज़ोरावर भवन का एहसास होता है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों में केवल आदत, बनावटी डर या राष्ट्रीय अहंकार के चलते युद्ध की धमकियां देना किस प्रकार के लीडर को शोभा देता है? क्या यह सब काबिल-ए-रहम नहीं है? काबिल-ए-रहम इसलिए, क्योंकि हमें कहीं न कहीं तो यह जरूर पता होता है कि हमारे आक्रामक व्यवहार का कारण और स्त्रोत सिर्फ डर नहीं है। इसका पीछे पैसे का भी हाथ है: शस्त्र उद्योगों की मुनाफाखोरी और इसी के साथ सैन्य-औद्योगिक संकुल द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहयोग, जिसके बारे में राष्ट्रपति आईज़ेनहोवर ने हमें चेतावनी दी थी।
जब उसके नागरिकों की ज़िंदगी असंतोष से भरी हो या जब उसके नागरिक ऐसी शक्तिहीनता की भावना का अनुभव कर रहे हों, जिसे हिंसा से आसानी से शांत किया जा सके, तो किसी भी राष्ट्र को हिंसात्मक होने पर मजबूर करना आसान होता है। जब राजनीतिक विमर्श ऐसे गहरे अविवेक और नफरत से भर गया हो कि गालियां सामान्य लगने लगें, तब अनिष्ठा राज करती है। हमारे पब्लिक डिबेट बच्चों की लड़ाइयों से भी ज़्यादा गए-गुजरे हो गए हैं: एक दूसरे को बुरा भला कहना, तू-तड़ाक करना, गालियां देना, चुगली करना, खींसे निकालना; हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि कभी कभार तो ऐसा लगता है कि शासन व्यवस्था सचमुच बच्चे ही चला रहे हैं।
पिछले पांच शताब्दियों में अफ्रीका को हमेशा गुर्बत का आईना समझा गया है। जबकि तथ्यात्मक रूप से अफ्रीका तेल, सोने, हीरों, कीमती धातुओं इत्यादि का खज़ाना रहा है। किन्तु इस खजाने का विशेषाधिकार अफ्रीका के मूलनिवासियों के बजाए पश्चिमी ताकतों के पास है। इसी कारणवश पश्चिम की नज़र में अफ्रीका अवहेलना, रंज और नि:संदेह लूटमार का पात्र हैं। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि उपनिवेशवाद एक प्रकार का युद्ध था और अभी भी है। एक ऐसा युद्ध, जिसका उद्देश्य दूसरे देशों के संसाधनों —यानि पैसे—पर कब्जा करना और उनको काबू में रखना है। हम अपने आपको इस भ्रम में भी रख सकते हैं कि दूसरे देशों को सभ्य और शांत करने के सारे प्रयत्नों का पैसे से संबंध नहीं है। गुलामी हमेशा पैसे के बारे में ही थी: मालिकों और उद्योगों के लिए मज़दूरों से मुफ़्त में पैसों का उत्पादन करने के लिए। समकालीन समय के “कामकाजी गरीब” और “बेरोजगार गरीब” भी उस “गूढ़ औपनिवेशिक अफ्रीका” की निष्क्रिय दौलत की तरह ही हैं—जिनसे मजदूरी और संपत्ति लूटी जा सकती है और जिनको उन विश्वव्यापी कॉरपोरेशनों द्वारा खरीदा जा चुका है, जो असहमत आवाजों को कुचल देती हैं।
इसमें से कुछ भी भविष्य के लिए आशावादी नहीं दिखता। फिर भी, मुझे अपने दोस्त का क्रिसमस के अगले दिन कॉल पर चिल्लाना याद है: नहीं! यही वह समय है जब फनकारों को काम पर लग जाना चाहिए। निराशा के लिए समय नहीं है, आत्मतरस के लिए जगह नहीं है, चुप्पी की जरूरत नहीं है, डर के जीने की कोई वजह नहीं है। हम बोलते हैं, हम लिखते हैं और हम भाषा के साथ कार्य करते हैं। इसी तरह से सभ्यताएं अपने घाव भरती हैं।
मुझे पता है कि दुनिया इस वक़्त चोटिल है और उसके घावों से खून रिस रहा है। हालांकि उसके दुख-दर्द को नज़रअंदाज़ न करना महत्वपूर्ण है, उसके द्वेष के आगे घुटने नहीं टेकना भी उतना ही जरूरी है। विफलता की तरह अव्यवस्था में भी ऐसी जानकारी सम्मिलित होती है, जो हमें ज्ञान की ओर ले जा सकती है—यहां तक कि विवेक की ओर भी। बिलकुल कला की तरह।