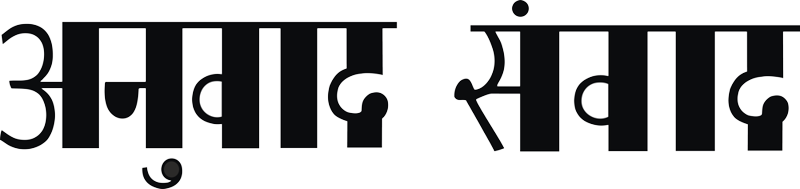Listen to this story
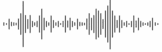
अनुवादक: चन्दन पाण्डेय
मैं सौभाग्यशाली था। मैं सही सलामत आंखों, पैरों और हाथों के साथ अपने घर जीवित लौटा। मैं जला नही था और न ही पागल हुआ था। कायदे से यह लड़ाई हमारी नहीं है, इसका एहसास हमें शुरू में ही हो गया था पर हमने तय किया कि खुद को जीवित रखते हुए इसे खत्म करते हैं और घर चलते हैं। फिर इसके अच्छे-बुरे पहलुओं पर सुनने-गुनने के लिए हमारे पास पूरा समय रहेगा।
मैं अफगानिस्तान जाने वाले पहले सैन्य-दस्ते में था। हमारे पास आदर्श नहीं, आदेश थे। आदेशों पर चर्चा नहीं करते—अगर आदेशों को चर्चा का विषय बनाया जाए तो सेनाओं की उम्र संदिग्ध हो जाएगी। एंगेल्स का कथन आप जानते ही होंगे? ‘सैनिक उस गोली की तरह होते हैं जो चलने के लिए हर-पल तैयार रहती है।’ यह कथन मैंने अपने भीतर जज्ब कर लिया था। युद्ध में आप हत्या करने के लिए ही जाते हैं। हत्या करना मेरा व्यवसाय ह—मुझे इसी की ट्रेनिंग भी मिली है।
क्या मैं डरा हुआ था? मैने दरअसल यह मान लिया था कि बाकी लोग भले मारे जाएं, मैं नहीं मरने वाला। दरअसल आप अपने मरने की सम्भावना को सोच भी नही सकते। और यह भी न भूलें कि जब वहां गया तो मैं बच्चा नही था, तीस का हो चुका था।
वहां मैंने जीवन के उद्दात आशय को समझा। बेधड़क कहूं तो यह कि वो मेरी उम्र के सर्वश्रेष्ठ वर्ष थे। यहां (रूस में) जीवन धूसर और संकीर्ण है: दफ्तर–घर, घर–दफ्तर। वहां हमें खुद के लिए खुद ही सब कुछ करना होता था और यह पौरुष के इम्तिहान सरीखा था।
वहां काफी कुछ आकर्षक भी था: सूनी घाटियों में भोर वाली धुन्ध धुएं के परदे की मानिन्द लहर लेती हुई उठती थी, या वो बरूबखैकी—लम्बी पाल वाले चमकीले अफगानी ट्रक—और लाल धारी वाली बसें जिनमें भेड़, गाय और इंसान बेतरतीबी ढंग से भरे रहते थे, और वो पीली टैक्सियां... कई जगहें ऐसी होती हैं जो अपने लौकिक दृश्य में चांद की याद दिलाते हैं। आप इस महसूसियत से पूरे-पूरे भर रहे होते हैं कि उन अजर-अमर पहाड़ों में जीवन का एक रेशा तक नही हैं, चट्टानों से अलग वहां कुछ भी नहीं है—तब तक ये एहसास आप में बना रहता है जब तक वो चट्टानें आप पर गोली नहीं दागने लगती हैं! आप समझ जाते हैं कि प्रकृति भी आप से शत्रुता रखने लगी है।
अपनी हस्ती जीवन और मृत्यु के बीच फंसी थी, और हम अपने हाथों में दूसरों के जीवन-मृत्यु के धागे थामे हुए थे। क्या इससे भी शक्तिशाली कोई भाव सम्भव है क्या? हम फिर कभी उस तरह नहीं चलेंगे, उस तरह प्रेम नही करेंगे और न ही हमसे कोई वैसा प्रेम करेगा जैसा अफगानिस्तान में हमने कर लिया। मृत्यु की सर्वत्र नजदीकी ने हर चीज को अनूठी उंचाई दे रखी थी: मृत्यु हर पल और हर क्षण में व्यापी हुई थी। जीवन साहसिक कारनामों का कारखाना हो गया था: मैने खतरे की गंध पहचानना सीख लिया—अब मेरे लिए यह एक अतिरिक्त इंद्रिय अनुभव हो चुका है। यूं तो इसे ‘अफगान सिन्ड्रोम’ कहा जाता है पर यह सच है कि हममें से बहुत सारे लोग वहां वापस जाना चाहते हैं।
हमने सही–गलत के खांचे में सोचने की जहमत कभी नहीं उठाई। अपनी-अपनी ट्रेनिंग के अनुसार हमने सारे आदेश पालन किए। बेशक, अब अतीत तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर पूरे अफगानिस्तान युद्ध पर पुनर्विचार हो रहा है पर दस वर्ष पूर्व समय ऐसा नहीं था। उन दिनों हमारे सामने दुश्मन की छवि स्पष्ट थी—किताबों, स्कूल और सिनेमा के माध्यम से बनी छवि। जैसे, मान लीजिए ‘द ह्वाईट डेजर्ट सन’ नाम की फिल्म। उस फिल्म को पांच बार तो कम-अज-कम देखा ही होगा। अभी हम इस शिकायत से दो-चार हो ही रहे थे, हम दूसरी जंग-ए-अजीम के बाद की पैदाइश हैं कि यूरेका! वाले अन्दाज में एक रेडीमेड युद्ध हमारे क्षितिज पर टांग दिया गया। हम जंगों और इंकलाबों से प्रेरणा पाते हुए बड़े हुए।
तो मैं बता रहा था कि अफगानिस्तान जाने वाले पहले सैन्य-दस्ते में हम थे। छावनी, सैन्य-क्लब और कैंटीन की नींव रखते हुए हम बेहद खुश थे। हमें टीटी-44 पिस्तौलें तवील की गईं थीं, जिन्हें आपने पुरानी फिल्मों के राजनयिक अधिक्षकों को झुलाते हुए देखा होगा। उन बन्दूकों का इससे पेश्तर कोई इस्तेमाल न था कि उससे खुद को ही गोली मार ली जाए या फिर उन्हें बाजार में बेच दिया जाए। हमें जो हाथ लग जाए जैसे पजामा या वर्दी, वही पहनकर बाजारों में घूमते थे। मुझे ‘श्वैक’ नाम वाले भले फौजी का दर्जा मिला था। तापमान पचास डिग्री हो तो भी हमारे अधिकारी हमसे टाई समेत पूरी वर्दी पहनने की अपेक्षा रखते थे।
शुरू में मुर्दाघरों में कटे-पिटे मानव शरीर और मांस के लोथ देखे जो किसी झटके से कम नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि हम सिनेमा देख रहे होते और पर्दे के पीछे अगर गरजते हुए गोले बरस रहे हों तो भी हम सिनेमा में मशगूल रहते... या फिर हम वॉली-बॉल खेल रहे होते थे और अगर बमबारी शुरू हो जाए तो पल भर के लिए रुक कर यह देखते कि बम किस दिशा में बरस रहे हैं और फिर अपने खेल में रम जाते। जो फिल्में हमें भेजी जाती थीं उनमें या तो युद्ध होते थे या लेनिन या फिर पतियों के साथ बेवफाई रचती स्त्रियां। मैं तो खुशी-खुशी उन स्त्रियों को भून डालता जो अपने पतियों की गैरमौजूदगी में पराये मर्दों के साथ बिस्तर साझा करती थीं। हम सब हास्य फिल्में चाहते थे लेकिन साहबों ने एक न भेजी। दो से तीन चादरों को सीलकर परदा बनाया गया था और हम दर्शक बालू पर बैठकर फिल्में देखते थे।
सप्ताह में एक दफे हमें स्नान और मयनोशी का मौका मिलता था। भर बोतल वोदका की कीमत तीस ‘चेकी’ होती थी, इसलिए हम अपने वतन से ही लेकर आते थे। सीमा शुल्क के नियमानुसार वोदका के दो बोतल, वाईन की चार बोतल और बीयर की अनगिन बोतलें ला सकते थे, इसलिए हम बीयर की तमाम बोतलों को खाली कर उसमें वोदका भर लेते। अन्यथा तो पीने का पानी भी चालीस डिग्री वाला मिलता। नशे के लिए लोग हवाई जहाज के लिए इस्तेमाल किया हुआ किरोसिन या हिमनिरोधी (एंटीफ्रीज) पी लेते थे। नये रंगरूटों को हम हिमनिरोधी पीने से मना करते थे, कहते थे और चाहें जो कुछ पी लो, पर कुछ ही दिन में ये रंगरूट अस्पताल में अपनी क्षरित खाद्यनली के साथ मिलते।
हम चरस पीते थे। अपने एक साथी ने एक दिन ऐसी चरस चढ़ा ली कि युद्ध मैदान में चल रही सभी गोलियों पर उसे अपना ही नाम लिखा हुआ लग रहा था। दूसरे ने एक रात इतनी चरस पी ली कि वो परिवार के साथ होने के दु:स्वप्न में फंस गया और अपनी पत्नी को चूमने भी लगा। कुछ को सिनेमा की तर्ज पर सारे रंग नजर आने लगते थे। पहले तो व्यापारियों ने इसे हमें बेचा फिर हमें मुफ्त ही देने लगे, कहते, ‘लगे रहो, रस्कियों, तुम्हारी ही मौज है!’ बच्चे हमारे पीछे दौड़ते और इसकी पुड़िया हमारी मुट्ठियों में फंसा देते।
न जाने कितने मेरे मित्र मारे गए। एक की एड़ी से ‘माईन बम’ के नंगे तार दब गए, उसने बम के छल्ले खुलने की आवाज भी सुनी और जैसा कि होता है, बेहद हड़बड़ी में जमीन पर लेटने के बजाय गहन अचम्भे में आवाज की उस जगह को देखने लगा। वह दर्जनों कील और बारूद के घावों से मरा। दूसरी किसी जगह एक टैंक इस कदर भयावह रूप से फटा कि उसका निचला तल्ला ‘जैम’ की शीशी के मानिन्द खुल गया और इसके पट्टे में छिपी इल्लियां बेतहाशा उड़ने लगीं। चालक ने भागने की कोशिश की थी, हमने देखा कि उसका एक हाथ बाहर झूल रहा था और बस इतना ही—वो अपने ही टैंक में जल गया था। इधर छावनी में कोई भी उसके बिस्तर पर सोना नहीं चाहता था। एक दिन एक नया रंगरूट आया और हमने उसे वही बिस्तर दिया, यह कहते हुए कि ‘तुम तो उसे जानते भी नहीं थे यार, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है।’
सर्वाधिक उदासी हमें उनकी मौत पर होती थी जिनके बच्चे थे, बच्चे जो अब पिता की अनुपस्थिति में ही बड़े होंगे। दूसरी तरफ यह ख्याल भी हमें घेरकर मारता था कि उनका क्या जिनके पीछे कोई नहीं, वो तो ऐसे मर गए जैसे वो कभी रहे ही न हों?
यह युद्ध लड़ने के लिए हमें तनख्वाह बेहद मामूली मिलती थी: कहने को तो हमें मूल वेतन का दोगुना मिलता था पर उसमें से टैक्स, सदस्यता राशि और नाहक के कुछ खर्चे काट लिए जाते थे। और मिलता भी क्या था: 270 अफगानी मुद्रा। वो भी नगद नहीं, रसीद मिलती थी। उन दिनों सुदूर उत्तर में काम करने वाले सिपाहियों को 1500 मुद्राएं मिल रही थी। ‘सैन्य सलाहकार’ हमसे दसेक गुना अधिक कमा रहे थे। यह अंतर तब और विकराल दिखता था जब हम सीमा पार कर रहे होते: हमारे पास दो-एक जोड़ी जिंस और एक टेप रिकॉर्डर होता था। वहीं उत्तर से आने वालों के पास दर्जन भर भारी बक्से होते थे, जिन्हें खींचने वाले भी परेशान हो जाते।
सोवियत संघ, यानी ताश्कन्द की हमारी वापसी भी आसान न थी।
‘अफगान से आए हो? लड़की चाहिए? मेरे यार, तुम्हारे लिए मेरे पास एक जब्बर माल है, महुए के फूल सरीखी नर्म...’
‘ना। मैं छुट्टियों पर हूं और घर जाना चाहता हूं। पत्नी के पास। मुझे टिकट चाहिए।’
‘टिकट पैसे से मिलते हैं, बाबूजी... क्या तुम यह इतालवी चश्मा बेचना चाहोगे।’
‘यही तरीका है।’
स्वेर्डलोवस्क तक की हवाई यात्रा के लिए मुझे 100 रूबल के साथ अपना इतालवी चश्मा, जापानी लुरेक्स स्कार्फ और एक फ्रांसीसी मेक अप किट खर्चना पड़ा। टिकट की कतार में मुझे पता चला कि चीजें कैसे काम करती हैं: ‘यहां कतार में दिनों-दिन खड़े रहने की क्या जरूरत मियां? अपने रोजगरिया पासपोर्ट में चालीस रसीदें डालकर आगे बढ़ाओ और अगले दिन घर पहुंच जाओ।’
तो भी मैं टिकट-खिड़की तक पहुंचता हूं, ‘ स्वेर्डलॉवस्क का एक टिकट।’
‘टिकट नहीं हैं। आंखे फाड़कर ऊपर देख, सूचना लिखी हुई है।’
मैं चालीस रसीदें बढ़ाता हूंऔर फिर कोशिश करता हूं, ‘स्वेर्डलॉवस्क के लिए एक टिकट मैडम, प्लीज।’
‘मैं दुबारा पता करती हूं। ओह्हो! आप बहुत भाग्यशाली हैं, देखिए अभी-अभी कोई अपना टिकट वापस कर गया है।’
अपने वतन लौटते हुए आप नितांत दूसरी दुनिया में उतरते हैं—परिवार की दुनिया। पहले कुछ दिन तक आप उनका कुछ भी कहा हुआ सुन नहीं पाते। आप बस उन्हें देखते हैं, उनका स्पर्श महसूस करते हैं। इतना सब कर गुजरने के बाद अपने बच्चों के सिर सहलाने का एहसास कैसा होता है, यह मैं बता नहीं सकता। सुबह के कॉफी और पैन-केक की महक... सुबह के नाश्ते के लिए बीवी की पुकारती हुई आवाज... बस, मैं बता नहीं सकता, ये एहसास कैसे हैं?
एक महीने में आपको वापस जाना होता है। वजह और जगह—दोनों नहीं पता। आप इस बारे में सोचते ही नहीं—कायदे से सोचना भी नहीं चाहिए। आप इतना भर जानते हैं कि आपको जाना है। किसी रात अपनी पत्नी के ढीले आगोश में पड़े हुए आपके दांतों में अफगानिस्तान की नर्म रेत का स्वाद फैल जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही तो आप उस रेत में अपनी सैन्य-टुकड़ी के साथ लेटे हुए थे... आप जागते हैं और बिस्तर से कूद पड़ते हैं—आप खुद को याद दिलाते हैं, आज आप घर पर हैं। कल सुबह आपको लाम पर जाना है।
आज पिताजी ने सूअर-कशी के लिए मुझे बुलाया। अतीत के ऐसे बुलाओं पर मैं कान पर हाथ रखकर भाग जाता था, जिससे मैं मरते सूअर की चीख भी न सुन सकूं। पर आज मैं पिता से कहता हूं, ‘थमिए जरा, ऐसे नहीं पकड़ते, सीधे दिल पर निशान साधिए, ऐसे’ और मैं चाकू के एक ही वार से उसे मार डालता हूं।
शुरू में मुर्दाघरों में कटे-पिटे मानव शरीर और मांस के लोथ देखे जो किसी झटके से कम न थे। लेकिन यह प्रक्रिया थमने नहीं जा रही हैं, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि पहले अपना खून न बहे। एक बार की बात है, कुछ सैनिक बैठे थे और वहां से एक बूढ़ा आदमी अपने खच्चर के साथ गुजर रहा था। अचानक ही एक सैनिक ने मोर्टार उठाया और खच्चर और उस बुजुर्ग को मार गिराया।
‘अबे ओ! पागल हो गए हो तुम लोग? इस बुजुर्ग और खच्चर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था?’
‘कल ऐसे ही एक बूढ़ा अपने खच्चर के साथ गुजरा और जैसे ही वो गुजरे हमने देखा कि अपना एक साथी यहां मरा हुआ पड़ा है।’
‘लेकिन यह भी हो सकता है कि ये दूसरे रहे हों?’
खून बहाने वाला पहला आदमी बनने की सबसे बड़ी दुर्दशा यह है कि आप जीवन भर अतीत के बुजुर्ग और अतीत के ही खच्चर को गोली मारते रहते हैं।
हमने वह युद्ध किया, जीवित रहे और घर लौटे। अब वह माकूल समय है कि हम कोशिशों के बल पर उस समूचे युद्ध से कोई मतलब निकालें।