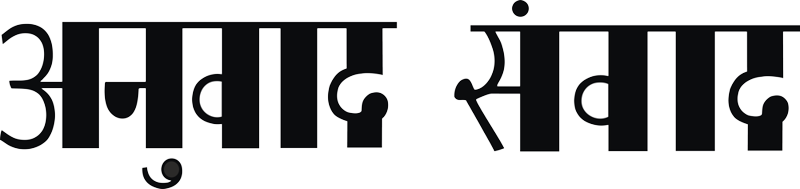Listen to this story
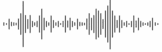
अनुवादक: शहादत
स्त्रोत: The leaflet
सुधीर मिश्रा की ‘अफ़वाह’ और सुदीप्तो सेन की ‘द केरल स्टोरी’ एक ही दिन रिलीज़ हुईं, इन दोनों फिल्मों में समान मुद्दों के बारे में समान दर्शकों को संबोधित किया गया, लेकिन दोनों फिल्मों में दिखाई गई ‘सच्चाइयां’ एक-दूसरे के विपरीत थीं। दोनों सवर्ण फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों के ज़रिये सहधर्मी हिंदुओं को संबोधित करते हुए उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि वे किस तरह के हिंदू बनना चाहते हैं, ऐसा हिंदू जिसको हर मुसलमान के अंदर एक छुपा हुआ इस्लामिक स्टेट ऑफ़ सीरिया एंड इराक (आईएसआईएस) का ऑपरेटिव दिखता है या उस तरह का जो हर मुसलमान की मानवता को समझने की क्षमता रखता है।
अगर ‘द केरल स्टोरी’ हिंदुओं को इस बात के लिए सावधान करती है कि मुसलमान सामान्य रूप से हिंदुओं और विशेष रूप से हिंदू महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, तो ‘अफ़वाह’ हिंदुओं से आत्मचिंतन करने और यह देखने के लिए कहती है कि वे खुद के साथ क्या कर रहे हैं? जबकि दोनों फिल्में हिंदू महिलाओं पर केंद्रित हैं, ‘द केरल स्टोरी’ हिंदू महिलाओं को इतनी भोली और मंदबुद्धि दिखाती है कि उन्हें केवल उनके सतर्क भाइयों, पिताओं और पतियों द्वारा ही संरक्षित किया जा सकता है। दूसरी ओर, ‘अफ़वाह’ में महिलाओं को अपने लिए सोचने और जरूरत पड़ने पर ‘अपने’ पुरुषों के खिलाफ जाने के लिए बताया गया है।
सिनेमाघरों में दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों फिल्में अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी हद तक सफल रही हैं। ‘द केरल स्टोरी’ देखने के बाद एक अनजान अधेड़ उम्र का आदमी मुझसे और मेरे मुस्लिम दोस्त (जिसकी आमतौर पर हिंदुओं द्वारा गलत पहचान की जाती है, क्योंकि वह अपने हाथ में कड़ा पहनता है) से बात करने लगा कि कैसे “हम हिंदुओं को जागने की जरूरत है, वरना वे (संभवतः मुसलमान) हमारी बेटियों और बहनों को हमसे ऐसे ही दूर करते रहेंगे।”
जब वह यह बात कह रहा था तो बगल में खड़ी उसकी पत्नी को उसके इस कथन से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हमें क्षमाप्रार्थी नज़रों से देखते हुए वह उसे शांत और चुप रहने के लिए कह रही थी। फिल्म में उस स्त्री के लिए कुछ नहीं था। उसे एक बेवकूफ इंसान के रूप में पेश किया गया था, जो आसानी से ब्रेनवॉश किए जाने और किसी के भी द्वारा खिलौने की तरह चलाए जाने के लिए मानो तैयार बैठी है। फिल्म के लिए लक्षित दर्शक उसका पति था और ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहा था जैसा कि फिल्म निर्माता उससे चाहता था।
‘अफ़वाह’ फिल्म खत्म होने के बाद हमने किसी भी तरह की उग्र प्रतिक्रिया नहीं देखी। लेकिन हमने एक और अधेड़ उम्र के जोड़े के बीच हो रही बातचीत सुनी। साड़ी पहने, बिंदी लगाए एक महिला अपने पति से कह रही थी, “लेकिन यह सच है, नहीं? ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड आजकल कुछ भी कहते रहते हैं।”
जहां एक फिल्म ने हिंदू पुरुष को ‘अपनी’ महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित कर दिया, वहीं दूसरी फिल्म ने हिंदू महिला के ज़हन में सोशल मीडिया पर परोसी जा रही चीजों की सत्यता के बारे में सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन यह माना गया कि दोनों फिल्में हमारे समय की ‘सच्चाई’ दिखाती हैं।
‘द केरल स्टोरी’ स्पष्ट रूप से दावा करती है कि वह “कई सच्ची कहानियों से प्रेरित है।” यहां तक कि फिल्म में उन वास्तविक लड़कियों या उन लड़कियों के रिश्तेदारों के इंटरव्यू के फुटेज भी दिखाए गए है जिनकी कहानियों के आधार पर फिल्म बनाई गई है। हालांकि ‘अफ़वाह’ सच होने का स्पष्ट दावा नहीं करती, फिर भी समाचार रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और सच्ची घटनाओं को दर्शाने के ज़रिये वह यह सुनिश्चित करती है कि हमें समझ आ जाए कि वह हमारी हक़ीक़ी दुनिया से संबंधित है।
जहां एक फिल्म ‘लव जिहाद’ की हकीकत दिखाने का दावा करती है, वहीं दूसरी फिल्म यह दिखाने का दावा करती है कि कैसे ‘लव जिहाद’ की अफवाहें कुटिल राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए हमारे दिमाग में बैठा दी हैं। एक मायने में ‘अफ़वाह’ हमें दिखाती है कि हमारे लिए ‘द केरल स्टोरी’ की ‘सच्चाई’ पर विश्वास करने के लिए कैसे पृष्ठभूमि तैयार की गई है। दूसरी तरफ ‘द केरल स्टोरी’ हमें दिखाती है कि कैसे ‘अफ़वाह’ जैसी फिल्में हमसे सच्चाई छिपाती हैं, जिससे हम अनर्थकारी साजिशों में आसानी से फंस जाते हैं।
‘अफ़वाह’ हमें बताती है कि ‘द केरल स्टोरी’ जैसी फिल्में उस तरह का प्रोपेगेंडा है जो हमें नफरत और आत्म-विनाश के रास्ते पर ले जाती है। जबकि ‘द केरल स्टोरी’ बताती है कि ‘अफवाह’ जैसी फिल्में उस तरह का प्रोपेगेंडा है जो हमें शालीनता और आत्म-विनाश के रास्ते पर ले जाती है।
एक दर्शक के तौर पर हम कैसे तय करें कि कौन-सी फिल्म सच है और कौन-सी प्रोपेगेंडा? हम कैसे तय करें कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं? मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब तक पहुंचने का एक तरीका यह पहचानना है कि सत्य और प्रोपेगेंडा के बीच का अंतर ही झूठा है। यह केवल इसलिए बना और टिका हुआ है क्योंकि लोकप्रिय बोलचाल में प्रोपेगेंडा को नकारात्मक अर्थ दिया गया है। लेकिन प्रोपेगेंडा का नकारात्मक होना जरूरी नहीं है।
एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में प्रोपेगेंडा को जनता की राय को प्रभावित करने के लिए सूचना-तथ्यों, तर्कों, अफवाहों, अर्ध-सत्य या झूठ के प्रसार के रूप में परिभाषित किया गया है। फिल्म निर्माण और कला की प्रकृति एक विशेष उद्देश्य के लिए विशेष दृष्टिकोण से वास्तविकता को दर्शाना है।
फिल्म और कोई भी कला कृति लोगों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर एक युक्ति का निर्माण है। डब्ल्यूईबी डू बुआ अपने लेख ‘क्राइटएरिया ऑफ नीग्रो आर्ट’ में लिखते हैं, “सारी कला कृतियां प्रोपेगेंडा हैं और हमेशा रहेंगी।” इसके बाद वह हमें बताते हैं कि प्रोपेगेंडा के रूप में ब्लैक आर्ट की क्या सकारात्मक क्षमताएं हैं। वास्तव में ब्लैक पॉलिटिकल सोच में एक पुरानी परंपरा है जो प्रोपेगेंडा की सकारात्मक क्षमता पर जोर देती है।
जबकि प्रोपेगेंडा पर अधिकांश आधुनिक कार्य ने प्रोपेगेंडा की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है—विशेष रूप से अधिनायकवादी और सत्तावादी शासन (हिटलर से मोदी तक) द्वारा इसके उपयोग के ऊपर—क्रांतिकारियों और लोकप्रिय आंदोलनों के नेताओं के लिए भी प्रोपेगेंडा ही एकमात्र उपकरण उपलब्ध है।
1902 में प्रकाशित ‘व्हाट इज़ टू बी डन’ में व्लादिमीर इलिच लेनिन ने जनता को आंदोलन के लिए शिक्षित, प्रबुद्ध और तैयार करने के तरीके के रूप में प्रोपेगेंडा पर जोर दिया। कम्युनिस्टों के लिए अधिकारों के लिए किए गए आंदोलनों में प्रोपेगेंडा जरूरी था। वहीं से हमें ‘एगिटप्रॉप’ शब्द मिलता है। डॉ अंबेडकर के आह्वान ‘शिक्षित करें, संगठित हों, आंदोलन करें’ में ‘शिक्षित’ करने का वही मतलब है जो कम्युनिस्टों के लिए प्रोपेगेंडा का मतलब है, कि जनता को सूचित करना और वह मंच बनाना जिस पर वे संगठित होकर आंदोलन कर सकें।
प्रोपेगेंडा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। जैसा कि डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना था, प्रोपेगेंडा की अच्छाई या बुराई का निर्णय सिर्फ यह देख कर किया जा सकता है कि वह किस लक्ष्य के लिए किया जा रहा है। ऐसे में हमारे लिए यह मायने नहीं रखता कि कौन-सी फिल्म ‘सच्चाई पर आधारित’ है और कौन-सी फिल्म ‘सच्चाई पर आधारित’ नहीं है। बल्कि सिर्फ यह मायने रखता है कि कौन-सी फिल्म अच्छा प्रोपेगेंडा है और कौन-सी फिल्म बुरा प्रोपेगेंडा है। इसे समझने के लिए हमें फिल्मों को उनके लक्ष्यों के गुणों के आधार पर आंकना होगा।
अच्छा प्रोपेगेंडा और बुरा प्रोपेगेंडा
तर्क बनाम भावनाओं का आह्वान
समय के साथ हमने अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श की समझ विकसित की है। चूंकि स्पर्श व्यक्तिगत होता है, इसलिए अच्छे और बुरे स्पर्श को पहचानने के मानदंड भी पूरी तरह से व्यक्तिगत होते हैं। अच्छा स्पर्श वह है जो व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करवाता है, जबकि बुरा स्पर्श वह है जो व्यक्ति को असुरक्षित और डरा हुआ महसूस कराता है। चूंकि प्रोपेगेंडा हमें सामाजिक स्तर पर प्रभावित करता है, इसलिए हमें प्रोपेगेंडा को आंकने के लिए सामाजिक मानदंड विकसित करने होंगे।
यह देखते हुए कि हम संवैधानिक गणतंत्र में रहते हैं, जहां लोकतंत्र को सर्वोच्च मूल्यों में से एक माना जाता है, हम मजबूती से यह दावा कर सकते हैं कि हमारे समाज में लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाला प्रोपेगेंडा अच्छा है, जबकि लोकतंत्र को बदनाम करने वाला प्रोपेगेंडा बुरा है। या, इसे दूसरे तरीके से व्यक्त करें तो अच्छे प्रोपेगेंडा का उद्देश्य लोकतांत्रिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है, जबकि बुरे प्रोपेगेंडा का उद्देश्य लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई को उकसाना है।
जबकि सभी प्रोपेगेंडा जनमत को आकार देने के लिए भावनाओं को उत्तेजित करने पर निर्भर हैं, लोकतंत्र केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता से चलता है। लोकतंत्र को बहिष्कृत राष्ट्रों, वर्गों और लिंगों तक विस्तारित करने के लिए दिए जाने वाले तर्क हमेशा प्रत्येक मानव की समान तार्किक क्षमता को उल्लिखित करते हैं। इसके विपरीत, जिन लोगों ने दूसरों पर शासन किया है—चाहे जाति, नस्ल या लिंग के निर्माण के माध्यम से—उन्होंने हमेशा अपने शासन को इस आधार पर सही ठहराया है कि गुलामों में तर्क करने की क्षमता नहीं होती है।
हम दावा कर सकते हैं कि विवेक की क्षमता विकसित करना हमेशा स्वतंत्रता आंदोलनों और क्रांतियों का महत्वपूर्ण घटक रहा है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि वह प्रोपेगेंडा लोकतांत्रिक है जो विवेक को बढ़ाता है और वह प्रोपेगेंडा लोकतंत्र-विरोधी है जो विवेक को कुंद करता है।
यह देखते हुए कि ‘द केरल स्टोरी’ और ‘अफ़वाह’ दोनों उपदेश देने वाली फिल्में हैं, हम डॉ किंग की व्याख्या का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि अच्छे प्रोपेगेंडा को एक ‘संवेदनशील उपदेश’ की तर्ज पर समझा जा सकता है। एक अच्छा उपदेश वह है जो श्रोताओं की भावनाओं को भावनाओं के माध्यम से विवेक के उपयोग तक ले जा सके।
वहीं असंवेदनशील उपदेश वह है, जो दर्शकों को उन्माद की लहर में उड़ा देता है और उन्हें उस उत्तेजित भावनात्मक स्थिति से कार्य करने के लिए उकसाता है। एक संवेदनशील उपदेश कुछ ऐसा होगा जो डॉ किंग अश्वेत लोगों को सविनय अवज्ञा के लिए प्रेरित करने के लिए देंते हैं; जबकि असंवेदनशील उपदेश कू क्लक्स क्लान के नेताओं द्वारा एक लिंचिंग के लिए गोरे लोगों को भड़काने के लिए दिया जाता है।
हमारे संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी के भाषण और अनुराग ठाकुर के भाषण में यही अंतर है। हम कह सकते हैं कि जहां बुरा प्रोपेगेंडा केवल दर्शकों की भावनाओं के साथ खेलता है, वहीं अच्छा प्रोपेगेंडा बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए भावनाओं का उपयोग करता है।
इस फर्क को दोनों फिल्मों में लगभग समानांतर सीन के जरिए दिखाया गया है। दोनों फिल्मों में महिला द्वारा उपदेश दिया जाता है। यह उपदेश दर्शकों के लिए भी उतना ही है जितना कि स्क्रीन पर उनके श्रोता के लिए।
‘अफ़वाह’ फिल्म में एक कॉलेज स्टूडेंट रहब अहमद (नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी) और निवी सिंह (भूमि पेडनेकर) से पूछता है कि उन्हें इतने विस्फोटक और दंगा-प्रभावित समय में क्यों भागना पड़ा। जिस पर निवी सिंह उन्हें उपदेश देते हुए कहती हैं कि कैसे उन्हें सोशल मीडिया पर आने वाली किसी भी चीज पर यकीन करने से पहले उसकी पड़ताल करनी चाहिए और अपना खुद के दिमाग का इस्तेमाल करके फैसला लेना चाहिए। वह उसे कहती है कि उसे सोशल मीडिया कैंपेन पर अंध-विश्वास नहीं करना चाहिए।
‘द केरल स्टोरी’ में निमाह मैथ्यूज (योगिता बिहानी) पुलिस के पास जाती है और केरल की हजारों लड़कियों (32,000) के बारे में निराधार तथ्य बताना शुरू करती है। उसके हिसाब से इन लड़कियों का ब्रेनवॉश किया गया और केरल के स्थानीय मुसलमानों द्वारा आत्मघाती हमलावर बनने, अफगानिस्तान और सीरिया में आईएसआईएस के गुलाम बनने के लिए उनका अपहरण कर लिया गया।
पुलिस अधिकारी सिनेमा में बैठे फिल्म देख रहे सभी लोगों को निराश करता हुआ (स्पष्ट रूप से असंवेदनशील) तथ्य प्रस्तुत करता है कि कानून के प्रतिनिधि के रूप में उसे कार्रवाई करने के लिए ठोस सबूतों कि जरूरत है। जिस पर निमाह फट से एक चुभने वाले सवाल पूछती है (यहां दर्शक उसके लिए तालियां बजाते हैं): ‘क्या वह केरल के इस्लामिक राज्य में बदल जाने पर भी सबूत मांगता रहेगा, या वह उठेगा और देश को बचाने के लिए कुछ करेगा?’
निमाह मूल रूप से यह कह रही है कि हमें सतर्क न्याय देने के लिए अपनी भावनाओं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कठिन साक्ष्य एकत्र करने और कानून का उपयोग करने की प्रक्रिया बहुत बोझिल और समय लेने वाली है। जबकि निवी हमें निर्णय लेने से पहले साक्ष्य एकत्र करने के लिए कह रही है, वहीं निमाह हमें इसके विपरीत करने के लिए कह रही है।
जहां एक फिल्म विवेक के उपयोग और तर्कसंगतता को पूरी तरह से खारिज करती है और हमें भावनाओं में बहकर काम करने के लिए उकसाती है, वहीं दूसरी फिल्म बताती है कि भावनाओं के साथ तर्क और तर्कसंगतता भी होनी चाहिए। ‘अफ़वाह’ प्रोपेगेंडा के उस रूप में कार्य करती है जिसे लोकतांत्रिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है—प्रति-प्रोपेगेंडा के रूप में जो हमें यह दिखाने के लिए भावनाओं का उपयोग करता है कि विवेक को छोड़ना हमारे लिए बुरा क्यों है।
जटिल बनाम सरल इंसान
अच्छे प्रोपेगेंडा को बुरे प्रोपेगेंडा से अलग करने का एक और तरीका है—हमारे सामने पेश किए गए मामले की जटिलता को आंकना। क्या लोगों को जटिल प्रेरणाओं वाले पूर्ण मानव के रूप में दर्शाया जा रहा है, या उन्हें केवल एक एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए कैरिकेचर किया जा रहा है?
डु बोइस के हिसाब से लोकतांत्रिक प्रोपेगेंडा लोगों के नैतिक क्षितिज का विस्तार करता है, जिससे उन्हें दुनिया और उसमें उनकी जगह के बारे में व्यापक दृष्टिकोण मिले। किसी के नैतिक क्षितिज का विस्तार करने का अनिवार्य पहलू पहचान और विचारों के मतभेदों को समझना और उनका सम्मान करना है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए यह जरूरी भी है।
हम अपने प्रतिनिधियों को चुनने में सिर्फ इसलिए एक-दूसरे को भाग लेने की अनुमति देने को तैयार हैं, क्योंकि हम एक-दूसरे को समझते हैं और सम्मान करते हैं। जबकि ‘अफ़वाह’ हमें मुसलमानों (और हिंदुओं) को समझने और उनका सम्मान करने के लिए कहती है, ‘द केरल स्टोरी’ हमें यह बताकर अपने साथी नागरिकों के लिए सम्मान और समझ को कम करने का प्रयास करती है कि हम मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वे हमारे कितने भी करीब क्यों न हों, क्योंकि कोई भी मुसलमान एक गुप्त आईएसआईएस एजेंट हो सकता है। (‘द केरला स्टोरी’ के अनुसार, हम हिंदू लड़कियों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बहुत आसानी से ब्रेनवॉश किया जाता है)।
भले ही दोनों फिल्में मुस्लिम दर्शकों के लिए नहीं बनी हैं, फिर भी मुसलमान दोनों फिल्मों की कहानियों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ‘अफ़वाह’ में हम तरह-तरह के मुसलमान देखते हैं। हमारे पास राहब अहमद जैसा लिबरल मुस्लिम है, जो अमीर, शहरी और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, जिसने एक हिंदू महिला से इस्लाम में परिवर्तित हुए बिना शादी की है। उसने आखिरी बार कब नमाज़ पढ़ी थी, यह भी उसे याद नहीं है।
उच्च जाति का एक मुस्लिम परिवार (सिद्दीकी) है, जिसके पिता का हिंदू-मुस्लिम दुश्मनी को भड़काने वाले राजपूत राजनेताओं के साथ ‘समझौता’ है और जिसने राहब के रिश्तेदारों में से एक के साथ शादी को भी अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि राहब का परिवार निम्न-जाति (बढ़ई) से है।
एक खुशमिजाज मुस्लिम ट्रक ड्राइवर है, जो इस बात की परवाह किए बिना कि एक हिंदू श्रेष्ठतावादी ने उससे लिफ्ट ली है, अपने व्यवसाय के बारे में बात किए जा रहा है। फिर असहाय मुसलमान हैं, जो हिंदू दंगाइयों द्वारा कुचल दिये जाते हैं। फिल्म में कम से कम चार अलग-अलग तरह के मुसलमान हैं, जो कई अलग-अलग भूमिकाओं में दिखते हैं- अच्छा-बुरा, अमीर-गरीब, अशरफ-अजलाफ, उदार-रूढ़िवादी, आदि।
‘द केरल स्टोरी’ में बोलने वाली भूमिका वाला हर मुसलमान अपरिवर्तनीय और अमानवीय रूप से भावहीन है, उसके पास बेइंतिहा कैश है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है और कितने भी लोगों कि ज़िंदगियां बर्बाद कर सकता है। ऐसा लगता है कि उनका कोई परिवार या दोस्त भी नहीं है, जो संभवतः उनसे अलग सोच सके या उनकी ज्यादतियों पर लगाम लगा सके।
यहां तक कि अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान के बीच के विवादास्पद अंतर को भी नकार दिया गया है। साथ ही प्यार का उपदेश देने वाले और नफरत का उपदेश देने वाले इस्लाम के बीच के अंतर को भी मिटा दिया गया है। अगर कोई फिल्म में दिखाई गई कहानी पर यकीन करता है तो उसे लगेगा कि सभी मुसलमान हमेशा बुरे होते हैं और इस्लाम हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं सिखाता।
ऐसे मुसलमानों के साथ लोकतांत्रिक समाज कैसे संभव है? हम इन मुसलमानों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो हमेशा इस्लाम के बारे में अत्यंत विकृत दृष्टिकोण से सृजित नापाक मंसूबा रखते हैं? यदि वे लोकतांत्रिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे मुस्लिम हैं और इस्लाम लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं देता है, तो फिल्म के हिसाब से यह उनकी गलती है और उनके साथ अलोकतांत्रिक तरीके से पेश आना न केवल सही है बल्कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य भी है।
मुसलमानों का खलनायकीकरण निरंतर चलता है और फिल्म में ऐसा करने के लिए हर छोटे से छोटे मौका का उपयोग किया गया है। एक बिंदु पर हमें शालिनी उन्नीकृष्णन (अदा शर्मा) के साथ छेड़छाड़ करते मुस्लिम व्यक्ति के कमरे में एक पोस्टर दिखाया गया है, जिसमें लिखा है, ‘राष्ट्रवाद हराम है, हम मुस्लिम समुदाय हैं।’
जिस स्थान पर हिंदू महिलाएं कट्टरपंथी बनने के लिए जाती हैं उसे इस्लामिक स्टडी सेंटर कहा जाता है [स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) या इसी नाम के काल्पनिक ‘मदरसा’ का संदर्भ बनाने की कोशिश की गई है]।
एक अन्य दृश्य में जब शालिनी पहली बार अपने नर्सिंग कॉलेज के कैंपस में एंट्री करती है तो वह उसकी दीवारों पर अल्लाहु-अकबर के साथ ‘आज़ाद कश्मीर’ की ग्रैफिटी देखती है और फिर उसकी आंखें और कैमरा बुरहान वानी और ओसामा बिन लादेन के चेहरों की ओर घूमते हैं।
फिल्म में कश्मीरी स्वतंत्रता-सेनानियों को, जो अपनी आज़ादी के लिए राष्ट्रवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक वैश्विक इस्लामी नेटवर्क का हिस्सा बना दिया गया है, जो विश्व व्यवस्था को बदलना चाहता है। यहां संकेत दिया गया है कि मुसलमानों के भीतर बारीकियां या मतभेद संभव नहीं हैं। संयोग से फिल्म में अल-कायदा और आईएसआईएस के बीच ‘संघर्ष’ का संदर्भ दिया गया है, लेकिन इस कोण को अनदेखा छोड़ दिया गया है।
इस मुकाम पर यह आपत्ति दर्ज की जा सकती है कि यहां पानी की तुलना दूध से की जा रही है। ‘द केरल स्टोरी’ मुसलमानों की आलोचना करती है, जबकि ‘अफ़वाह’ हिंदुओं की आलोचना है। इसलिए हमें ‘अफ़वाह’ में हिंदुओं के चित्रण को देखना चाहिए कि क्या ऐसी जटिलता वहां भी है।
अगर ‘द केरल स्टोरी’ को मुसलमानों की आलोचना करने के लिए उन्हें कैरिकेचर के रूप में पेश करने की जरूरत है तो क्या ‘अफ़वाह’ ने हिंदुओं के साथ भी ऐसा ही किया है? क्या किसी समुदाय की प्रभावी ढंग से आलोचना करने के लिए कैरिकेचर बनाना आवश्यक है? ‘अफ़वाह’ में हिंदुओं के बहुस्तरीय चित्रण को देखते हुए ऐसा नहीं लगता।
फिल्म में हिंदू एक-दूसरे से उतना ही लड़ रहे हैं और एक-दूसरे को उतना ही मार रहे हैं जितना कि मुसलमानों को (जबकि ‘द केरल स्टोरी’ में मुसलमानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं दिखाया गया है)। यहां तक कि ‘अफ़वाह’ में हिंदुवादी राजनीतिक नेता और उसके गुंडों को भी जटिल चरित्र दिए गए हैं। वे अपने आपसे लगातार सवाल करते हैं और इस बारे में चिंता करते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। फिल्म में दिखाए गए सबसे खलनायक हिंदू के भीतर भी आंतरिक संघर्ष है—अच्छाई और बुराई की ताकतें, जो उसे अपनी ओर खींच रही हैं।
विक्की सिंह (निवी के मंगेतर और कहानी के केंद्रीय खलनायक के रूप में सुमित व्यास) को हिंदू-मुस्लिम हिंसा को उकसाते हुए दिखाया गया है, लेकिन केवल इसलिए कि उसे हिंदू-बहुसंख्यक पार्टी के समर्थन की जरूरत है, वह खुद एक पल के लिए भी किसी भी तरह की कट्टरता में विश्वास नहीं करता।
हालांकि, उसके समर्थक भी उसी नाव में सवार प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनके मन में भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है, वे सिर्फ ऊपर से आए आदेश का पालन कर रहे हैं। विक्की सिंह का प्रमुख गुंडा चंदन सिंह (शारिब हाशमी) फिल्म में एकमात्र चरित्र है जो वास्तव में मुस्लिम विरोधी है। लेकिन वह भी एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर से दोस्ती करता है और उसकी मृत्यु के बाद सम्मानपूर्वक उसे दफनाता है।
‘द केरल स्टोरी’ में मुसलमानों के प्रति यह बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं दिखाया गया है, जो न केवल हिंदुओं का बल्कि साथी मुसलमानों का भी मर्डर और बलात्कार करते हैं। सबसे खराब परिस्थितियों में भी उनमें पछतावा या संदेह का एक अंश भी नहीं दिखाया गया है। एक ट्रक ड्राइवर का अच्छा व्यवहार एक कट्टर हिंदू गुंडे के दिल में मानवता जगाता है, लेकिन ‘द केरल स्टोरी’ में महिलाओं का गहरा प्यार भी युवा मुसलमानों में संदेह का एक अंश पैदा करने में सक्षम नहीं है।
‘अफ़वाह’ में प्रमुख संघर्ष एक राजपूत परिवार के भीतर है। यह अच्छे हिंदू और बुरे हिंदू के बीच का संघर्ष है। जबकि बुरे हिंदू—जो वास्तव में मुसलमानों से नफरत करते हैं या राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों से नफरत करने का दावा करते हैं—की निंदा की गई है, अच्छे हिंदू को सराहा गया है। फिल्म यह नहीं कहती है कि सभी हिंदू बुरे हैं और हमें उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है (‘द केरल स्टोरी’ के विपरीत, जो हमें कोई अन्य समाधान नहीं देती—यदि सभी मुसलमान बुरे हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता है तो आपको उनके साथ क्या करना चाहिए? या तो घरवापसी/शुद्धि या हत्या या जबरन प्रवास—किसी भी तरह से नरसंहार)।
‘अफ़वाह’ का कहना है कि हिंदू धर्म के भीतर भ्रष्टाचार का इलाज खुद हिंदू ही कर सकते हैं। अच्छे हिंदू अपने पूरे समुदाय को सुधारने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इसका भार हिंदू महिला निवी सिंह पर डाला गया है, जो अपने मंगेतर और पिता को तब छोड़ देती है जब वह उन्हें धार्मिक कट्टरता में डूबते हुए देखती है और अंत तक उनसे लड़ती है, यहां तक कि अपने मंगेतर की मृत्यु का कारण भी बनती है।
वह परिवार की वफादारी के ऊपर सही काम करने का विकल्प चुनती है और हिंदुओं से कहती है कि वे भी ऐसा ही कर सकते हैं (शायद ‘अफ़वाह’ फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की पत्नियों, गर्लफ्रेंड, बेटियों और बहनों से निवी के जरिये अपने कट्टर हिंदुवादी पुरुषों को छोड़ने के लिए कह रही है)। जाति-विरोधी दृष्टिकोण से देखे जाने पर अच्छे हिंदू और बुरे हिंदू के बीच यह अंतर स्वयं समस्याग्रस्त है (लेकिन यह एक अलग विषय है)।
लोकतंत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले और फिल्म देखने वाले बेवकूफ हैं या समझदार?
लोकतंत्र जिन चीजों पर निर्भर करता है उनमें से एक यह विश्वास है कि हमारे आस-पास के लोग समझदार हैं और उनमें स्वतंत्र और तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है। ऐसी समझ के बिना लोकतंत्र कभी भी संभव नहीं होगा। वास्तव में, जैसा कि फ्रांसीसी दार्शनिक जैक रौंसीयर के काम से पता चलता है, लोकतंत्र-विरोधी विचारधाराओं की पहचान ही यह है कि उनके हिसाब से लोग या ‘भीड़’ बेहद मूर्ख है और नहीं जानती कि उनके लिए क्या अच्छा है, और इसीलिए उनका मार्गदर्शन करने और उनकी रक्षा करने के लिए किसी और (निश्चित रूप से उनसे अधिक बुद्धिमान) की ज़रूरत है। इसी तर्क का इस्तेमाल गांधी ने अछूतों के खिलाफ, श्वेत वर्चस्ववादियों ने अश्वेत समुदायों के खिलाफ, पुरुषों ने महिलाओं के खिलाफ, और ‘परोपकारी’ राजाओं और औपनिवेशिक ताकतों ने अन्य सभी लोगों के खिलाफ किया था।
यहां हम दोनों फिल्मों के लोकतांत्रिक और लोकतंत्र-विरोधी रुख के बीच अंतर करने के तीसरे तरीके पर आते हैं। हालांकि दोनों ही फिल्मों में सभी महिलाएं उच्च जाति की हैं, समृद्ध हैं और लगभग हमउम्र हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें दुनिया के बारे में बहुत अलग-अलग किस्म की जानकारी है।
फिल्म में जिस हद तक बेवकूफ दोनों हिंदू औरतों—शालिनी और गीतांजलि (सिद्धि इदानी)—को दर्शाया गया है, वह देखकर तो ‘द केरल स्टोरी’ मुस्लिम विरोधी होने से ज्यादा हिंदू-महिला विरोधी प्रतीत होती है। न केवल उनका अपने ऊपर कोई काबू नहीं है, क्योंकि उनको कोई भी ‘ब्रेनवॉश और प्रोग्राम करके रीमोट कंट्रोल से संचालित कर सकता है’, फिर वे किसी भी तरह के बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन से कोसों दूर भी हैं।
आज के इंटरनेट युग में ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी उस कॉलेज की तस्वीरें नहीं देखीं जिसमें वे पढ़ने जा रही थीं। दोनों महिलाएं केरल के शहरों में अपनी ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक नर्सिंग कॉलेज पहुंचती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे पहले कभी उनका किसी ईसाई या मुस्लिम से सामना नहीं हुआ है।
केरल में मजबूत समकालिक परंपरा और हिंदू धर्म के विभिन्न रूपों के साथ दोनों धर्मों के सह-अस्तित्व की लंबाई को देखते हुए ऐसा कुछ संभव नहीं लगता है। लड़कियों को आश्चर्य होता है जब उन्हें पता चलता है कि ईसाइयों और मुसलमानों में स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। यह कहे जाने पर उनकी भयावह प्रतिक्रिया को देखते हुए कि अगर वे इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुए तो वे नरक में चले जाएंगे, ऐसा लगता है कि उनके पास पांच साल के बच्चों का दिमाग है न कि कॉलेज जाने वाले वयस्क स्टूडेंट का।
वे नर्सिंग स्टूडेंट हैं, लेकिन वे लगभग अनजान लड़कों द्वारा अचिन्हित प्लास्टिक के पैकेट में अचिह्नित गोलियां स्वीकार करती हैं और उन्हें खाना शुरू कर देती हैं। वे इस हास्यास्पद तर्क के बाद हिजाब पहनने के लिए सहमत हो जाती हैं कि हिजाब पहनने वाली कोई भी लड़की कभी किसी पुरुष द्वारा परेशान नहीं की जाती है, क्योंकि अल्लाह उसकी रक्षा करता है। क्या उन्होंने कभी न्यूज नहीं देखी? क्या वे इस छोटी-सी चीज को गूगल भी नहीं कर सकतीं? वे अपनी नंगी तस्वीरें अपने बॉयफ्रेंड को भेजना शुरू कर देती हैं, वे गर्भवती हो जाती हैं, वे भूल जाती हैं कि अबॉर्शन का विकल्प उपलब्ध है, वे अपने मरते हुए पिता पर थूकती हैं क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, वे अपनी विधवा मां को त्याग देती हैं और खलीफा के लिए सीरिया में लड़ने चले जाती हैं। उनका मानना है कि कासरगोड में उनके अलावा हर लड़की हिजाब पहनती है। उनकी इस तरह की मूर्खता की सूची अनंत है।
जबकि गीतांजलि के अंदर एक दिन अचानक बुद्धि आ जाती है, शालिनी की आंखें तब खुलती है जब अफगानिस्तान में उसके पति द्वारा उसका बलात्कार किया जाता है। यहां आश्चर्य होता है कि अगर वह इतनी बेवकूफ है और अपने दिमाग़ या इंटरनेट का उपयोग करना भी नहीं जानती है तो वह नर्सिंग कॉलेज में भर्ती कैसे हुई?
फिल्म के हिसाब से ये लड़कियां इतनी भोली कैसे बनी? यह बताने के लिए एक ईसाई लड़की की मदद ली गई है। मुस्लिम लड़की आसिफा (सोनिया बलानी) ईसाई निमाह को अपने चंगुल में फ़ंसाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ईसाइयों को उनके परिवारों द्वारा धर्म और परंपरा सिखाई जाती है, जो उन्हें मुस्लिम प्रोपेगेंडा से बचते हैं। दूसरी ओर, हिंदू लिबरल और कम्युनिस्ट बन गए हैं, वे अपनी परंपराओं को भूल गए हैं, या उन्होंने अपनी परम्पराएं त्याग दी हैं। इस कारण हिंदू महिलाओं को कोई भी राह चलता मुसलमान अपना शिकार बना लेता है, क्योंकि वह उनके जीवन में धार्मिक शून्य को भरने में कामयाब होता है।
इस कथात्मक तर्क के तहत हादिया जैसी लड़की मुस्लिम पुरुष से इसलिए शादी नहीं करती क्योंकि वह उसे चाहती है या उससे प्यार करती है, बल्कि सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसे उसके ब्रेनवाशिंग का मुकाबला करने के लिए उपाय नहीं बताए गए हैं। चूंकि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में धकेलने के लिए हिंदू पिता जिम्मेदार हैं, इसलिए फिल्म उन्हें हिंदू धर्म अपनाने और बहुत देर होने से पहले अपनी लड़कियों को नियंत्रित करने के लिए कहती है।
महिलाओं हर किसी से तो बेवकूफ बन ही रही हैं, साथ ही इससे बचने के उपाय में भी उनकी कोई भूमिका नहीं है। लव जिहाद का शिकार बनने से रोकने के लिए उन्हें अपने पिता, भाइयों और पतियों का संरक्षण स्वीकार करना होगा। उन्हें हिंदू धर्म को स्वीकार करना होगा, जो निश्चित रूप से पुरुषों को उनके जीवन और कामुकता पर नियंत्रण देता है। महिलाएं बेवकूफ बनी रहेंगी। यह हिंदू पुरुषों पर निर्भर है कि वे उन्हें चालाक मुसलमानों से बचाएं।
फिल्म आसानी से इस तथ्य को नजरअंदाज कर देती है कि 2016 और 2018 के बीच केरल से अफगानिस्तान गई चार ज्ञात लड़कियों में से तीन—सोनिया सेबेस्टियन, मेरिन जैकब और राफेला—ईसाई थीं और केवल एक निमिशा हिंदू लड़की थी। या यह कि जिस लड़के से निमिषा ने शादी की वह ईसाई था, जो उसके साथ ही इस्लाम में परिवर्तित हुआ था।
हालांकि, अगर इन तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाए तो फिल्म हिंदुओं को अधिक धार्मिक बनने के लिए जो तर्क दे रही है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस समय एक और सवाल उठाया जा सकता है, अगर ये लड़कियां निर्दोष साबित हुई हैं लेकिन अभी भी अफगानिस्तान की किसी जेल में बंद हैं तो भारत सरकार ने उन्हें घर वापस लाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? हो सकता है कि ये लड़कियां फिल्म में दिखाई गई लड़कियों से ज्यादा समझदार हों और उनका बिल्कुल भी ब्रेनवॉश नहीं किया गया हो। हो सकता है कि वास्तव में उन्होंने जो रास्ता चुना है, वे उस पर विश्वास करती हों। कम से कम भारतीय जांच एजेंसियों ने काबुल में इन चार लड़कियों से पूछताछ के दौरान यही पाया था।
‘अफ़वाह’ भी एक हिंदू नायिका के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन इस बार उसके पास एक विवेकशील मस्तिष्क है और उस मस्तिष्क का स्वतंत्र उपयोग करने की क्षमता है। फिर चाहे उसे अपने पिता और मंगेतर का या पूरी दुनिया का विरोध ही क्यों न करना पड़े। इन दोनों फिल्मों को देखकर हमें चुनना ही होगा कि हम महिलाओं को कैसे देखना चाहते हैं—असहाय पीड़ितों के रूप में या समझदार मनुष्यों के रूप में। हम क्या चाहते हैं कि हमारे समाज में औरतों का दर्जा क्या हो—वे अपने पतियों और पिताओं द्वारा संरक्षित की जाएं या वे स्वतंत्र नागरिक की तरह रह पाएं जो खुद की रक्षा कर सकें (यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वयं के पतियों और पिताओं से भी खुद को बचा सकें)।
जहां एक फिल्म महिलाओं को पितृसत्तात्मक ढांचे की ओर वापस जाने के लिए कहती है, वहीं दूसरी फिल्म तर्क देती है कि स्वतंत्र और बुद्धिमान महिलाओं में न केवल खुद को बचाने की क्षमता होती है, बल्कि समाज को बदलने की क्षमता भी हो सकती है। एक फिल्म का तर्क है कि महिलाएं स्वतंत्रता के लायक नहीं हैं, जबकि दूसरी फिल्म का तर्क है कि केवल महिलाओं द्वारा अपने विवेक के स्वतंत्र प्रयोग करने से ही समाज को बचाया जा सकता है। जहां तक स्त्री प्रश्न का संबंध है, यह देखना मुश्किल नहीं है कि कौन-सी फिल्म बुरा प्रोपेगेंडा है और कौन-सी फिल्म अच्छा प्रोपेगेंडा है।
एक फिल्म महिलाओं को मुक्त करना चाहती है, जबकि दूसरी फिल्म उन्हें ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के दायरे में गुलाम बनाए रखना चाहती है। ‘लव जिहाद’ का हौव्वा केवल भय पैदा करके हिंदू महिलाओं को वापस ‘उनके’ पुरुषों के चंगुल में भेजने का तरीका है।
हिंदुओं को मुसलमानों की उतनी परवाह नहीं है जितनी उन्हें जाति व्यवस्था को बनाए रखने की परवाह है। हिंदू धर्म के लिए मुसलमानों से नफरत करना जरूरी नहीं है, लेकिन महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करना हिंदू धर्म के लिए जरूरी है। मुसलमानों से घृणा और लव जिहाद की भयावहता, जिसे ‘द केरल स्टोरी’ में दिखाया गया है, अंततः मुसलमानों पर लक्षित नहीं है, बल्कि हिंदू महिलाओं पर लक्षित है; हर हिंदू महिला जो अपनी जाति के बाहर शादी करती है, जाति व्यवस्था को कमजोर करती है और इस प्रकार, हिंदू धर्म को भी कमजोर करती है। यही कारण है कि फिल्म हिंदू महिलाओं पर केंद्रित है, भले ही तथ्य यह हो कि ज्यादा ईसाई महिलाएं इस्लाम में परिवर्तित हुईं और अफगानिस्तान चली गईं।
अच्छा प्रोपेगेंडा ‘दिखावटी अनभिज्ञता’ के खिलाफ क्रियान्वित होने का आह्वान है
लोकतांत्रिक प्रोपेगेंडा लोकतंत्र-विरोधी विचारधाराओं के खिलाफ भी होता है और हमें उस तरह की विचारधाराओं को त्यागने पर मजबूर करता है। डॉ किंग के हिसाब से अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की एक केंद्रीय समस्या श्वेत नरमपंथियों की राजनीतिक निष्क्रियता थी। इसीलिए उनके ‘संवेदनशील उपदेश’ का एक उद्देश्य उन लोगों के पाखंड को दर्शाकर उनके अंदर शर्म की भवन पैदा करना था।
श्वेत नरमपंथियों ने अश्वेत समुदाय की मदद करने के लिए बहुत सारे वादे तो किए लेकिन उनके लिए कोई भी जोखिम उठाने से इनकार कर दिया। बर्मिंघम जेल से लिखे अपने पत्र में डॉ किंग ने उन्हें उनकी ‘दिखावटी अनभिज्ञता’ के लिए लताड़ा और उन्हें बताया कि वे अपने खुद के किए हुए वादों से मुकर रहे हैं।
दरअसल, किंग का कहना था कि या तो श्वेत नरमपंथी अपनी दी गई ज़बान पर खरे उतरें या फिर साफ-साफ कह दें कि वे अश्वेतों के खिलाफ हैं। जैसा कि डॉ अंबेडकर ने इससे अलग संदर्भ में कहा था, “खुले दुश्मन विश्वासघाती दोस्तों की तुलना में कहीं बेहतर हैं”।
जबकि ‘अफ़वाह’ और ‘द केरल स्टोरी’ दोनों फिल्में नरमपंथी और लिबरल हिंदुओं की राजनीतिक निष्क्रियता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, ‘द केरल स्टोरी’ शर्म को नहीं बल्कि उनके डर को उभारती है। वह लिबरल हिंदुओं को डराती है कि अगर वे कट्टर हिंदू नहीं बने तो उनकी बहन-बेटियों के साथ कुछ भी हो सकता है। फिल्म चाहती है कि हिंदू इस डर की भवन के साथ कार्य करें। यह ठीक वही प्रतिक्रिया है जो इस लेख की शुरुआत में उल्लिखित फिल्म के दर्शक से मिली थी। वह शर्म में नहीं बल्कि डर और गुस्से में उबलता हुआ सिनेमा से बाहर निकला था।
दूसरी ओर, ‘अफ़वाह’ लिबरल हिंदुओं को उनके पाखंड के लिए शर्मिंदा करना चाहती है। फिल्म के आख़िर में, राहब नाहरगढ़ किले में इस विश्वास के साथ पहुंचता है कि साहित्यिक उत्सव में भाग लेते लिबरल हिंदू उसे कट्टरपंथी हिंदू से बचाएंगे। लेकिन उसे यहां बड़ा झटका लगता है। लिबरल हिंदू उसे अंदर आने कि अनुमति देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है। वे उसकी पत्नी से भी पूछते हैं, जो उत्सव में भागीदार है, कि वह कैसे सुनिश्चित हो सकती है कि राहब लव जिहाद में शामिल नहीं है। लिबरल हिंदुओं की इस कार्रवाई के कारण राहब को अनावश्यक रूप से चोट पहुंचाई जाती है।
घटनाओं का यह क्रम स्पष्ट रूप से लिबरल हिंदुओं को यह बताने के लिए है कि उनकी चरमपंथियों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की कमी के कारण अंततः मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिल्म उन्हें बता रही है कि वे पाखंडी हैं—राहब की पत्नी नंदिता ऐसा खुद कहती है—शांति और सद्भाव और फासीवाद के खतरों के बारे में अच्छी-अच्छी बातें करने के अलावा वे मुसलमानों को बचाने के लिए ज़मीन पर कुछ नहीं करते।
यह फिल्म नरमपंथी हिंदुओं को मुसलमानों के साथ सहानुभूति रखने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें अपनी खुद की मिलीभगत के लिए शर्मिंदा होने के लिए कहती है। फिल्म उनसे कह रही है कि अगर वे आज के भारत में अल्पसंख्यकों को बचाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं रखते, तो वे हिन्दू चरमपंथियों से ज्यादा अलग नहीं हैं। जबकि ‘द केरल स्टोरी’ अपने दर्शकों में अतिसतर्कता को सही ठहराने के लिए डर पैदा करती है, वहीं ‘अफ़वाह’ लोकतांत्रिक कार्रवाई की मांग करने के लिए उन्हें शर्मसार करती है।
संक्षेप में, ‘अफ़वाह’ अच्छा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि यह विवेक के उपयोग को बढ़ावा देती है, नैतिक क्षितिज का विस्तार करती है और लोकतांत्रिक राजनीतिक कार्रवाई को प्रेरित करती है। वहीं ‘द केरल स्टोरी’ खराब प्रोपेगेंडा है, क्योंकि यह विवेक के उपयोग को कम करती है, नैतिक क्षितिज को संकुचित करती है और अलोकतांत्रिक अतिसतर्कता को प्रेरित करती है।
‘अफ़वाह’ फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का काउंटर है, क्योंकि वे दोनों दर्शकों के एक ही समूह को संबोधित करती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या वे ‘द केरल स्टोरी’ जैसी फिल्मों पर विश्वास करके दुनिया के विक्की और चंदन बनना चाहते हैं, या फिर वे शर्म महसूस करके विक्की और चंदन के खिलाफ प्रतिबद्ध राजनीतिक रुख अपनाना चाहते हैं।
क्या बुरे प्रोपेगेंडा को बैन करना चाहिए?
इस मोड़ पर हमारे सामने एक और सवाल है। फिल्मों, वृत्तचित्रों, किताबों और चित्रों आदि पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी पक्षों के लोगों द्वारा नियमित रूप से किया जाता रहा है। कुछ लोग ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहेंगे, क्योंकि यह भड़काऊ फिल्म है, वहीं कुछ लोग भारत माता (मदर इंडिया) के कथित अपमान के कारण ‘पठान’ फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकते हैं।
हेट स्पीच और प्रोपेगेंडा के लिए ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान भी किया गया। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गईं। दोनों कोर्ट ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित किया गया है, इसलिए अदालत द्वारा इसे चुनौती देना अनुचित होगा।
जो भी हो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कानून व्यवस्था को होने वाले खतरे का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। जबकि तमिलनाडु सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि तमिलनाडु थिएटर और मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने इसे मल्टीप्लेक्स में न दिखाने का फैसला किया। इस बीच, मध्य प्रदेश ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, “फिल्म सभी को देखनी चाहिए।”
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ममता बनर्जी द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी सच्चाई से डरती हैं। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। नरेंद्र मोदी ने तर्क दिया था कि यह डॉक्यूमेंट्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और उस मामले में ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर सच्चाई से डरने का आरोप लगाया था।
बात यह है कि अदालतों ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले में कार्रवाई नहीं की, न ही उन्होंने ‘द केरल स्टोरी’ मामले में कार्रवाई की। दोनों प्रतिबंध राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित हैं। उन्हें कमजोर आधारों पर भी उचित ठहराया गया, जिसे अदालतों ने भी चुनौती नहीं दी। इस पर या उस पर प्रतिबंध लगाना राजनीतिक दलों के हित में हो सकता है, मगर यह न तो जनता के हित में है और न ही कानून के शासन के लिए अच्छा है।
हेट स्पीच और बुरे प्रोपेगेंडा के संबंध में कानूनी परिभाषाएं धुंधली हैं। जबकि कानून-निर्माताओं ने संविधान में जानबूझकर इन परिभाषाओं को अस्पष्ट रखा हो सकता है, जिससे उपयुक्त अधिकारियों को गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक घटना से निपटने की अनुमति दी जा सके, इस मामले का तथ्य यह है कि ज़्यादातर वक्त अधिकारी इन अस्पष्टताओं का दुरुपयोग करते हैं। वे जो उन्हें पसंद नहीं है (ज्यादातर उनकी नीतियों और राजनीति के खिलाफ आलोचना) उस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देते हैं। मगर अन्य भाषण और अभिव्यक्ति की अनुमति देते हैं जो ‘घृणास्पद’ हो सकती है लेकिन उनके राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करती है।
इस सब कुछ के बावजूद, ‘द केरल स्टोरी’ में जो दिखाया गया है, केरल हाईकोर्ट यह कहने में सक्षम है कि फिल्म में किसी विशेष धर्म के खिलाफ कोई आलोचनात्मक रवैय्या नहीं है, क्योंकि फिल्म केवल आईएसआईएस के खिलाफ कुछ दावे करती है। हालांकि फिल्म भय और क्रोध की भावनाओं को जन्म दे सकती है, लेकिन यह सीधे तौर पर हिंसा की वकालत नहीं करती।
कोर्ट के लिए गलत मिसाल कायम किए बिना ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल होगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित है और यदि ‘भाषण’ सीधे तौर पर हिंसा को प्रोत्साहित करता है या सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शालीनता और भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देता है तो अनुच्छेद 19(2) के तहत इसे सीमित किया जा सकता है। यह तर्क देना बहुत मुश्किल होगा कि ‘द केरल स्टोरी’ ऐसा कुछ भी करती है, और अगर यह तर्क दिया जाता है तो फिर कौन कह सकता है कि दीपिका पादुकोण के भगवा बिकनी पहनने से सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शालीनता को कोई खतरा नहीं है? क्या ‘द केरल स्टोरी’ को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, धारा 295ए और धारा 298 के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जैसा कि केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह ‘साबित’ करना असंभव है कि फिल्म सामान्य रूप से मुसलमानों के बारे में है और केवल आईएसआईएस के बारे में नहीं। आईएसआईएस के खिलाफ शत्रुता को भड़काना और उन्हें बदनाम करने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना भारत में काफी हद तक छद्म देशभक्ति का खेल बन चुका है।
तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें फिल्मों और किताबों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करनी चाहिए? मेरी राय में, जब तक कि वे सीधे हिंसा की वकालत न करें, कला के सभी प्रकारों को खुले तौर पर प्रसारित करने की अनुमति देना सबसे अच्छा होगा।
पहले तो आज की डिजिटल दुनिया में किसी भी चीज को लोगों से दूर रखना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो इसका मतलब यह कि किसी चीज को बैन करना व्यर्थ है क्योंकि उस बैन को लागू करना संभव ही नहीं है। और तो और, बैन करने से चीज लोगों के लिए अधिक आकर्षक बन जाती है और उसे अधिक लोग देखने को उत्सुक हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज को लोग न देखें, तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम उसे नजरंदाज करें या फिर उसकी आलोचना कर उसके उद्देश्य को नाकाम करें।
दूसरा, भले ही हम सहमत हों कि कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, हम बेहतर और स्पष्ट कानूनों के बिना ऐसा नहीं कर सकते। अच्छी तरह से परिभाषित कानूनों की अनुपस्थिति में सत्ता में रहने वाले लोग अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस तरह की मनमानी सत्ता लोकतांत्रिक कामकाज के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में खुली चर्चा और बहस जरूरी है।
उदाहरण के लिए, पिछले साल कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बनी शॉर्ट फिल्म ‘एंथम फॉर कश्मीर’ पर प्रतिबंध लगाए गए, जबकि उसी समय रिलीज हुई ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म पर सरकार ने न केवल कोई प्रतिबंध लगाया, बल्कि लोगों से इसे देखने का खुले तौर पर आग्रह करके सक्रिय रूप से इसका समर्थन किया। इसी तरह सरकार ने ‘द केरल स्टोरी’ को सक्रिय रूप से समर्थन करते हुए इस वर्ष बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
बुरे प्रोपेगेंडा को अधिक से अधिक प्रसारित किया जाना चाहिए, जिससे इसकी आलोचना की जा सके। इस पर प्रतिबंध लगाकर इसे सिर्फ भूमिगत किया जा सकता है, जहां इस पर खुलकर बहस नहीं हो सकती। इसके अलावा, बैन लगने पर इन फिल्मों के निर्माता उत्पीड़न का दावा करने लगते हैं, जिससे इनके प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ जाती है। ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘द केरल स्टोरी’ जैसी फिल्में वैसे भी ऐसी कहानियों के रूप में पेश की गई हैं, जिन्हें मुख्यधारा के बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने जानबूझकर छुपाया है। बैन लगने पर उनका यह दावा और मजबूत हो जाता है।
उनकी तमाम समस्याओं के बावजूद, ‘द केरल स्टोरी’ जैसी फिल्में इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि समाज का एक खास तबका उन्हें देखता है और खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। इन फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने और उन लोगों के साथ बातचीत करने से इनकार करने के बजाय, इन फिल्मों का इस मामले पर बात करने के अवसर के रूप में उपयोग करना सबसे अच्छा होगा।
उदाहरण के लिए, फिल्म देखने के कारण मैं इस लेख में बता पाया कि कैसे यह फिल्म बुरा प्रोपेगेंडा है, जो लोकतंत्र को कमजोर करती है और हिंसा को बढ़ावा देती है। मानस फिराक भट्टाचार्जी जैसे कुछ लेखकों ने लिखा है कि फिल्म पर बहस व्यर्थ है, क्योंकि यह “एक-दूसरे के राजनीतिक उद्देश्यों पर आरोप लगाते हुए दो पक्षों में सिमट जाएगी।”
मैं समझता हूं कि यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम साझा मूल्य और साझा आधार तलाशें, जिस पर सार्थक बहस हो सके। मैंने यहां लोकतंत्र को सामान्य मूल्य बनाने की कोशिश की है और उस मूल्य के आधार पर फिल्मों का विश्लेषण किया है। इस तरह के सामान्य मूल्यों का लगातार निर्माण किए बिना केवल ऐसा नहीं है कि हम बहस नहीं कर सकते, बल्कि हम एक समाज भी नहीं हो सकते।
इसलिए मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक ताकतों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधों के खिलाफ होना सबसे अच्छा है, चाहे उन्हें कोई कलाकृति पसंद हो या न हो। चयनात्मक रुख अपनाने से हमें ही नुकसान होता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तो हम तार्किक विसंगतियों में पड़ जाते हैं, जिनका हमारे विरोधियों द्वारा हमारे ही खिलाफ उपयोग किया जा सकता है।
किसी भी मामले में, चूंकि देश पर अलोकतांत्रिक ताकतों का शासन है, इसलिए किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति उनके हाथ में है और किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी आह्वान किसी और चीज़ पर प्रतिबंध लगाने के उनके निर्णय को आसान बना देता है, क्योंकि हम सैद्धांतिक आधार पर प्रतिबंध का विरोध करने का अधिकार खो देते हैं।
दक्षिणपंथी जो कलाकृतियां बना रहे हैं, उसकी खुले तौर पर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए और उसकी आलोचना की जानी चाहिए। हमें हर चीज पर मनमाने प्रतिबंध के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिससे हम जो रचना कर रहे हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाना कठिन हो। लोकतंत्र-विरोधी प्रोपेगेंडा पर रोक लगाने की अपेक्षा लोकतांत्रिक प्रोपेगेंडा को प्रतिबंधित होने से रोकना अधिक महत्वपूर्ण है। बुरे प्रोपेगेंडा को प्रतिबंधित करने के बजाय अच्छे प्रोपेगेंडा से लड़ना ज्यादा आसान और आवश्यक है।