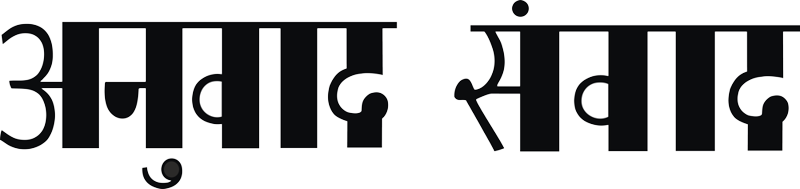Listen to this story
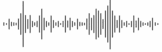
यह लेख पहली बार 6 नवंबर 2010 को http://kashmir solidarity.wordpress.com पर प्रकाशित हुआ था।
प्रिय कश्मीरी साथियों,
मैं यह खत न्यूयॉर्क से लिख रहा हूं। एक ऐसी जगह जो दूर होकर भी कितने करीब है।
आपसे वास्तविकता को छिपाकर यह शहर आपको सब भुला सकता है। लेकिन एक दूसरी वास्तविकता के करीब लाकर, दूसरों के कष्ट और पीड़ा के माध्यम से यह आपको लगातार वही सब याद भी दिलवाता है। यहां दुनिया के कोने-कोने से आए निर्वासित लोग रहते हैं (हां, अधिकतर वही जिनको अमरीका आने की अनुमति मिली)। यहां अकाल और युद्धों से भागे हुए आयरिश और ग्रीक लोग हैं। उत्पीड़न के बावजूद जीवित बचे जर्मनी के यहूदी हैं और रूस के जर्मन। एल साल्वाडोर, पेरू, ग्वाटेमाला और बोलीविया के लैटिन हैं, जो पश्चिम-समर्थित तानाशाही हुकूमतों के कारण अपने देशों से 70 और 80 के दशक में भाग आए थे। अफ्रीकी हैं, जो दक्षिण सूडान में हुए नरसंहार में बाल-बाल बचे। तुर्कीय के कुर्द हैं और उत्तर अफ्रीका के बरबर, जो सालों से चल रहे संघर्ष के कारण अपनी ज़मीनों से खदेड़ दिए गए। फिर अफ्रीकी-अमरीकी हैं, जिनको गोरे मालिकों की गुलामी के लिए सदियों पहले जबरन लाया गया था, जो आज भी अमरीका के ‘उत्तर-नस्लवादी’ बन जाने के दावों के बावजूद, आर्थिक-सामाजिक तौर पर सबसे निम्न स्तर पर सड़ रहे हैं। ये सारी कहानियां समान निष्कर्ष पर पहुंचती हैं: दुनिया छोटी राष्ट्रीयताओं और शक्तिहीन अल्पसंख्यकों के लिए सिकुड़ रही है।
अधिक क्षेत्र पर काबू पाने—और हिंसा करने के निर्विरोध अधिकार—की इच्छा रखने के कारण बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र छोटे और कमजोर लोगों के वैध अधिकारों को कुचल देते हैं। जो स्थायी “अपवाद की स्थिति” का दावा करते हैं, उन्होंने उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा दी, जिनके तहत “छोटे और बड़े” दोनों ही तरह के राष्ट्रों को आत्म-निर्णय के अधिकार की गारंटी मिलती है। मानवाधिकारों को कायम रखने के लिए की गई कई घोषणाओं के बावजूद दुनिया भर में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न जारी है। शक्तिशाली देश इन घोषणाओं का इस्तेमाल अपने संकुचित लक्ष्यों को पाने के लिए मन-मुताबिक करते हैं। कई सदियों से सार्वभौमिक मानव सभ्यता का झंडा उठाने का दावा करने वाला यूरोप आज फिर से नफरत के शिकंजे में फंसा हुआ है और ख़ुद को एक और नरसंहार के लिए तैयार कर रहा है; ऐसा ही अमेरिका में भी हो रहा है, जिसके नागरिकों को वहां के नस्लवादी, जाहिल और हिंसक राष्ट्रवादी राजनेता उन्माद की स्थिति में लाकर छोड़ दे रहे हैं। इस दौरान मुसलमान देशों को एक के बाद एक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक गलतफहमी और नफरत के विषय तो वे पहले से ही थे। अब वे प्रबुद्ध, सक्रिय और स्पष्ट प्रतिक्रिया देने में भी विफल साबित हो रहे हैं। वे या तो अल-क़ायदा जैसे उग्रवादी दलों की विनाशकारी हिंसा को बढ़ावा देते हैं, या फिर दुबई जैसे शोषण के उत्तम उदाहरण का निर्माण करते हैं; दोनों ही किसी न किसी तरीके से दूषित हुए पश्चिमी तर्कवाद के चरम रूप पर आधारित हैं और अधिकतर मुसलमानों के जीवित अनुभव और उनकी दीन के सार से कोसों दूर हैं।
इस सबके बीच आशा की गुंजाइश कहां से पैदा हो सकती है? हाल ही में बने राज्यों के साम्राज्यवादी प्रभुत्व के सपनों एवं धार्मिक-राष्ट्रवादी देशाहंकार के दलदल में फंसे अनेक, संघर्षरत, छोटे राष्ट्रों में से एक हैं कश्मीरी—जिनकी पीड़ा के लंबे इतिहास को सैन्य उत्पीड़न दिन पर दिन और बढ़ाता जा रहा है। हम खुद को कहां खड़ा रख सकते हैं? हम एक नई ज़िंदगी की कल्पना, सोच और योजना कैसे बना सकते हैं?
पहले मुझे यह कहने दीजिए: दुनिया भर के उत्पीड़ित लोगों सहित कश्मीरियों का दृढ़ता से अस्तित्व में बने रहना अपने आपमें इस बात का संकेत है कि संघर्ष जारी है: लाचार सैन्यकृत वास्तविकता और मुक्त कल्पना की शक्ति के बीच, दूसरों पर हावी होने के कठिन परिश्रम और विरोध की सुंदरता के बीच, शक्ति की टेक्नॉलजी और कर्ता के आलोचनात्मक अभ्यास के बीच, गणना और करुणा के बीच, पितृसत्तात्मक नफरत और न्याय के प्रति प्यार के बीच, राष्ट्रीय फासीवाद और राष्ट्रीय मुक्ति के बीच, धातु और दिल के बीच, गोली और जख्म के बीच, मृत्यु की छाया और ज़िंदगी के शामियाने के बीच संघर्ष जारी है। आशा सबसे पहले इसी संघर्ष से उभर कर आती है; हमें यह याद रखने की जरूरत है कि यह संघर्ष राष्ट्रों, संस्कृतियों या सभ्यताओं के बीच नहीं हो रहा है बल्कि उनके भीतर हो रहा है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा ख्याल है कि हमें अपने संघर्ष के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। हमारा संघर्ष कश्मीर और हिंदुस्तान का संघर्ष नहीं है, जो स्थिर राष्ट्रीय पहचान वाली क्षेत्रीय इकाइयां हैं। जाहिर तौर पर यह संघर्ष मुसलमान और गैर-मुसलमान का भी नहीं है, और न ही यह पूरब और पश्चिम का संघर्ष है। दरअसल, हमारा संघर्ष विरोध को अनिवार्य बनाने वाली नैतिक विचारधारा और दूसरे पर किए गए सैन्य उत्पीड़न को सही ठहराने वाले अपारदर्शी औचित्य के बीच का है। संघर्ष का यह पुनर्गठन हमें व्यापक रूप से खोल देता है: हम अज्ञात और अनजान दूसरों, ज़िंदगी को देखने के नए तरीकों और अनिर्धारित भविष्य की तरफ खुल जाते हैं। यह संघर्ष हमारे उन दूसरों के साथ, जिनकी पीड़ा हमारे लिए अदृश्य है और जिनकी यातना-भरी आवाजों को हम सुन नहीं पा रहे हैं, गठजोड़ बनाने के कर्तव्य का आह्वान करता है। इसकी मांग है कि नए जीवन की योजना न तो किसी मॉडल पर आधारित हो और न ही खुद मॉडल बने। हालांकि, अनिर्धारित भविष्य का मतलब यह नहीं है कि भविष्य का रास्ता अनियोजित और अस्त-व्यस्त हो। वैसे भी अनियोजित और अस्त-व्यस्त रास्ते पर कोई योजना बनाना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण (और व्यर्थ) होगा। इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य के कश्मीर को आज़ाद और स्वतंत्र बने रहना है और आज़ादी के क्षण को लगातार जीते रहना है तो वह पहले से मौजूद सामाजिक-आर्थिक ढांचे में नहीं ढल सकता (खासकर उन ढांचों में जो वर्चस्ववादी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था हमारे सामने रखती है), और न ही वह उस खंडित लोकतंत्र को स्वीकार कर सकता है जो लगभग व्यंग्य के रूप में भारतीय सरकार कश्मीरियों पर हर कुछ साल में थोपती है।
इसका मतलब यह भी है कि हम उन लोगों को चुनौती दें जो ‘इस्लामी राज्य’ बनाने के खोखले आह्वान करते हैं। हमें उनके ऐतिहासिक और तार्किक रूप से अनुचित दावों का खंडन करना होगा और उनकी सोच के रूपात्मक पहलुओं को विस्थापित करना होगा, लेकिन उसके साथ ही, अगर संभव हो तो, हमें इस्लाम[1] के नैतिक मूल को (जो कि बहुत गहराई से दफन है और अक्सर महत्वहीन बना दिया जाता है) पुनः प्राप्त करना होगा, क्योंकि इस्लाम का नैतिक मूल सार्वभौमिक एकजुटता और सामाजिक न्याय का आह्वान करता है। धार्मिक विचारधारा के आधार पर राज्य का निर्माण करने के बजाय (जो कि मूल तौर पर भारत, पाकिस्तान, ईरान, इज़राईल या अमेरिका से बहुत अलग नहीं दिखेगा और हमेशा अलगाववादी होगा), हमें एक-दूसरे पर विश्वास और भरोसे के आधार पर स्वतंत्र एवं आज़ाद समाज का गठन करना है। इस विश्वास और भरोसे का अर्थ होगा कि हम एक-दूसरे से डरना और एक-दूसरे पर संदेह करना बंद कर देंगे। इसका नतीजा यह होगा कि हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे, जिसमें हर किसी को हर किसी के ऊपर नजर रखने की जरूरत महसूस नहीं होगी, जिसके कारण हम निगरानी और निगरानी करने वाले जासूसों दोनों से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि यह पारस्परिक विश्वास एक-समान होने के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि सभी व्यक्तियों और सांस्कृतिक गुटों का एक-दूसरे के विशिष्ट रूप से अलग होने को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना ही इसका आधार होगा। हमें याद रखना होगा कि हमने एक-दूसरे की संगति स्वतंत्र रूप से चुनी है और हम सभी इस तरल और सदैव बनते हुए समाज के संपूर्ण और सार्थक सदस्य हैं। हम वैसे नहीं सोच सकते जैसे भारतीय राष्ट्रवादी सोचते हैं: कि हम कश्मीरी के तौर पर एक हैं; कि ‘कश्मीरियत’ नाम की कोई चीज है जो—किसी तरह के केमिकल या जेनेटिक पदार्थ या खून के जैसे—हमारे सभी के शरीरों में है। एक होने के बजाय हमें साथ होने के आधार पर सोचना होगा।
हमारे साथ होने का आधार स्वतंत्रता, लोकतंत्र और गरिमा है। मैं अक्सर इन तीन विचारों के बारे में एक साथ सोचता हूं: बिना स्वतंत्रता और गरिमा के लोकतंत्र नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही बिना लोकतंत्र और गरिमा के स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, और ज़ाहिर है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र से ही गरिमा संभव हो सकती है। ऐसा समाज, जो स्वतंत्र रूप से आलोचना की जगह देता है—न कि खोखले अर्थहीन तरीके से जैसा कि आजकल पश्चिम में हो रहा है—और उसकी प्रशंसा करता है और उसके आधार पर खुद को प्रगतिशील बदलाव के लिए खुला रखता है (प्रगतिशील: जो लगातार स्वतंत्रता और अधिकारों के क्षितिज को बढ़ावा दे), सिर्फ वही सच्चा लोकतंत्र कहलाने लायक है। संदेह और रूढ़िबद्ध धारणाओं से स्वतंत्रता ही गरिमा को उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह कि जब समाज अपने नागरिकों और सांस्कृतिक गुटों में भरोसा रखता है, तब उस समाज के व्यक्ति गरिमापूर्ण ज़िंदगी जी पाते हैं। जब मैं आज़ादी के बारे में सोचता हूं तो मुझे उसके मूल में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और गरिमा एक साथ जुड़े हुए दिखते हैं।
आप और मैं दोनों जानते हैं कि जो हमारे खिलाफ हैं और जो हमारे साथ हैं वे दोनों ही हमसे अक्सर पूछा करते हैं कि हम हमारी ‘आज़ादी’ की मांग का स्पष्टीकरण करें। हमने इसे अक्सर एक औपचारिक शर्त के तौर पर व्यक्त किया है: कि हमें भारत से आज़ादी चाहिए—उसके हमारी ज़िंदगियों पर अवैध स्वामित्व से आज़ादी (और हां जो बलपूर्वक सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हैं, वे हमारी आज़ादी के इस स्पष्ट विवरण को तो सुनने से भी इनकार कर चुके हैं)। लेकिन हम जानते हैं कि आज़ादी का मतलब इस मजबूरन लागू किए गए संयोजन से खुद को स्वैच्छिक रूप से अलग करने से कहीं ज्यादा है। इस दुनिया में जहां बड़ी पूंजी का वैश्विक दानव और उसके साथ जुड़े असमान संकट, शक्तिपूर्ण (और अक्सर परमाणु बमों से लैस) एवं युद्धप्रिय राष्ट्र-राज्यों से तर-बतर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिंसक तांडव करते हैं, वहां आज़ादी एक छोटे मगर गरिमापूर्ण राष्ट्र के जीने के अर्थ के मूल तक जाती है। इस कोलाहल में हमारे पास आज़ादी की खोज के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हम बड़े राष्ट्रों के साथ प्रभुत्व की लड़ाई नहीं लड़ सकते (मैं प्रभुत्व की इच्छा को मरने की इच्छा के रूप में देखता हूं, एक तरह का पागलपन—परस्पर सुनिश्चित विनाश) और अगर लड़ भी सकते तो हमें लड़ना ही नहीं है। हम इस दुनिया में बस एक और राज्य का गठन करने की मांग नहीं कर रहे हैं; उसका कोई अर्थ नहीं होगा। आज़ादी की हमारी मांग एक स्पष्ट आवश्यकता और महत्वाकांक्षा है और अगर आप इसे ऐसे देखना चाहें तो एक आखिरी हताश इच्छा है; क्योंकि जब बड़े राज्यों ने मिलकर हमारा सामूहिक विनाश निश्चित कर लिया होगा, तब कम से कम हम यह तो जानेंगे कि हमने उनसे बेहतर ज़िंदगी जी थी, और वह एहसास और भी मीठा होगा, क्योंकि हमने ऐसा बिना छाती ठोके, किसी को ज़ख्मी किए या बहुत पैसे खर्च करके किया होगा। हमारा यही मतलब होता है जब हम कहते हैं कि अपने भविष्य का निर्णय करने का (अगर मंजिल नहीं तो कम से कम रास्ते का) अधिकार हमारा खुद का है। गुंडई करने वाले बड़े राज्यों ने खुद के और हमारे दोनों के भविष्य का निर्णय कर लिया है और हम उस क्षण से छुटकारा नहीं पा सकते जब यह सब गायब हो जाएगा—यह काल्पनिक आदर्श नजरिया है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा—पर हमारी मांग यह है कि जब तक वह समय हमारे ऊपर नहीं आ पड़ता, तब तक हमें इस दुनिया में अपना खुद का रास्ता ढूंढने दिया जाए। हम आपके साथ ही गिरेंगे पर उस अंतिम कब्रिस्तान तक आपके साथ चलने के लिए हमें विवश नहीं किया जा सकता।
मेरे कश्मीरी साथियों, हमने अपने जिस्मों पर सामूहिक जख्म खाए हैं। और हां, जिस आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए यह कीमत बिल्कुल वाजिब है। हमारे शरीर इस बात का पर्याप्त सबूत हैं कि हम आज़ादी के योग्य हैं। हालांकि, हम सिर्फ अपनी आज़ादी की मांग नहीं रख रहे हैं, बल्कि हमारी मांग है कि सभी पीड़ित छोटे राष्ट्रों और अल्पसंख्यकों को आज़ादी मिलनी चाहिए। हम उनके साथ हमेशा नैतिक एकजुटता में खड़े रहेंगे—यह सिद्धांत हमें इस्लाम और अन्य धर्मों में समान तौर पर मिलता है। इनके अलावा, न्यायोचित सह-अस्तित्व के सार्वभौमिक मानक में भी यही सिद्धांत है जिसके आधार पर हम इस धरती पर सामूहिक जीवन जीते हैं।
अगर हमारी आज़ादी की यह नैतिक धारणा रहती है तो उन सवालों का जवाब देना उतना मुश्किल नहीं होगा जो हमारी अपरिहार्य स्वतंत्रता के बाद (और पहले) हमारे सामने भविष्य में खड़े होंगे। चूंकि हम इस बात को ठुकरा नहीं सकते कि हम उसी शक्ति के बलबूते पर बनी वास्तविक दुनिया में रहते हैं, जिसे उखाड़ फेंक हम एक नए कश्मीरी समाज का गठन करना चाहते हैं, हमें उसके साथ जूझना तो होगा ही, लेकिन अपनी शर्तों पर, आज़ादी के जैविक सिद्धांत के साथ। चीन, भारत और पाकिस्तान के राज्यों के साथ हमारे संबंध क्या होंगे? और इन देशों के एवं दुनिया के अन्य लोगों के साथ हमारे संबंध क्या होंगे? आज़ादी के सिद्धांत की मांग है कि अपने पड़ोसियों के साथ हम शर्त रहित मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएं। हमें इस शर्त रहित मित्रता का प्रस्ताव अपने आस-पड़ोस के छोटे एवं बड़े राष्ट्रों के सामने रखना होगा। हम इस प्रस्ताव से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब होगा कि हम उन्हें और उनके आपसी संबंधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि दक्षिण और पूरे एशिया में स्वस्थ संबंध बनाने की चेष्टा करेंगे और उनमें पारस्परिक सहभागिता की भावना को मिलाने की कोशिश करेंगे। इन आस-पड़ोस के और अन्य देशों के लोगों को कश्मीर में तीर्थ यात्रा के लिए या अन्य किसी कारण से आने की पूरी छूट मिलेगी; सिवाय उन लोगों के, जो यहां हिंसा फैलाने के लिए आना चाहते हैं: क्योंकि उसका मतलब होगा इंसानों और प्रकृति के खिलाफ हिंसा करना। इस आज़ादी की भावना के साथ ही क्या कश्मीरी उन लोगों को खुशी से नहीं स्वीकारेंगे जिनको न्याय और सच का साथ देने के लिए अपने देशों में जान का खतरा है? अरुंधती रॉय को कौन एहसानमंदी के साथ कश्मीरी नागरिकता नहीं देना चाहेगा?
कई सालों से, और शायद सदियों से कश्मीरी मुसलमानों के कश्मीरी हिंदुओं के साथ संबंध उथल-पुथल रहे हैं। मुसलमानों और सिखों के बीच संबंध भले ही ताकत, बदला और दबाव से भरे नहीं हैं पर फिर भी वे हिंसा की संभावना से तो ग्रसित रहे ही हैं। यही मामला कश्मीर के कई सामाजिक गुटों और मुसलमान समुदायों का भी है। मैं यह नहीं कह रहा कि ये सारी तकलीफें एकदम दूर हो जाएंगी, लेकिन यह हम सब का दायित्व है, और अपेक्षाकृत आसान भी, कि इन संबंधों से हिंसा की संभावना को मिटा दिया जाए। नई ज़िंदगी को मौका दिया जाना चाहिए। साझे भविष्य के निर्माण में इतिहास को रोड़ा बनने नहीं देना चाहिए। कश्मीर के अंदर हमारे समाज की जरूरत है कि मित्रता केवल उन समुदायों के बीच ही न सुनिश्चित की जाए जो कश्मीरी राष्ट्र का गठन करेंगे, बल्कि उन सभी व्यक्तियों के बीच भी सुनिश्चित की जाए जो इन समुदायों में शामिल हैं। यह कर्तव्य मुख्य तौर पर कश्मीर के बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय का है कि वे सच्ची और चिरस्थायी मित्रता का हाथ कश्मीर के अल्पसंख्यकों की तरफ बढ़ाएं।[2]
हमारी आज़ादी, जो हमारे समाज और राष्ट्र की नई ज़िंदगी का आधार है, कश्मीर के क्षेत्र से गहरे रूप से जुड़ी है। हालांकि यह क्षेत्र उदारता और मेहमाननवाजी का क्षेत्र है, न कि अलगाव और शत्रुता का। कश्मीर के साथ हमारे संबंध प्राकृतिक नहीं, प्रकृति के हैं। मेरे दोस्तों, इस बात से मेरा मतलब यह है कि कश्मीर के एहसानमंद निवासी होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम मानव और प्रकृति के बीच शोषण के संबंध बनने से रोकें। प्रकृति प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वह तो एक सामूहिक तोहफा है, जिसको एक-दूसरे के साथ विवेकपूर्ण तरीके से साझा करना और मानवों और गैर-मानवों के आज और कल के लिए संरक्षित करना जरूरी है। अगर यहां पेड़ ही नहीं बचेंगे; अगर कश्मीर की नदियां और तालाब सूख जाएंगे और पहाड़ खोद दिए जाएंगे; अगर यहां की हवा दूषित हो जाएगी और मिट्टी कैमिकल से भर जाएगी; अगर यहां के भालू और हिम-तेंदुए जैसे गौरवपूर्ण निवासी अपने स्थानों से विस्थापित कर दिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे, तो फिर कश्मीर की आज़ादी का क्या मूल्य रह जाएगा? ऐसी आज़ादी में, जिसमें हम प्रकृति के साथ आदरपूर्ण संबंध बनाते हैं, हमारे निर्वाह के स्त्रोत—हमारी अर्थव्यवस्था—क्या रूप लेंगे? हम किन चीजों का उत्पादन करेंगे और कैसे उपभोग करेंगे? उत्पादन और उपभोग के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा, जो नैतिक रूप से प्रकृति की तरफ हमारे दायित्व के खिलाफ नहीं होगा लेकिन हमारी उचित जरूरतों को पूरा भी करेगा? क्या हमें आर्थिक तर्कवाद, औद्योगिक अतिउत्पादन और अतिउपभोक्तावाद से निजात पाने की जरूरत नहीं है? हम हमारी वस्तुओं और सेवाओं की अदला-बदली कैसे करेंगे। क्या छोटे पैमाने के व्यवसायों को हमारे समाज में विनिमय का नियामक एवं सैद्धांतिक तरीका नहीं बनना चाहिए, जो हमेशा लुटेरी कॉर्पोरेशन्स के खिलाफ निगरानी करेंगे?
मेरे दोस्तों, आज़ादी की हमारी यह यात्रा उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमने महसूस किया था कि हमें आज़ाद होने की जरूरत है। समय के साथ हममें से अधिकांश लोगों को यह समझ आया कि सिर्फ़ कश्मीर और उसके निवासियों की आज़ादी के लिए संघर्ष करके और उस संघर्ष में कामयाबी पाकर ही हम सच्चाई के साथ अपनी जिंदगियां जी सकते हैं। इसलिए इस निर्माण का काम बहुत पहले शुरू कर दिया गया था। ऐसा समाज बनाने के लिए, जो वास्तविक तौर पर हमारे जीने के योग्य हो, हमारी तरफ से इच्छाशक्ति के असाधारण प्रयास और भयंकर सहनशक्ति की जरूरत पड़ेगी। हम असली आज़ादी तब तक हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक हम अपने दिल और दिमाग से दूसरों के प्रति, उनके प्रति भी जो आज हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, नफरत और हिंसा को पूरी तरह से उखाड़ नहीं फेंकते। हमें याद रखना होगा कि हमारी लड़ाई उन विचारधाराओं और प्रक्रियाओं के खिलाफ है जो दूसरों पर प्रभुत्व जमाने को वैध ठहराती हैं और हमें वैसा करने पर विवश करती हैं। यह उनके खिलाफ नहीं है, जो इन चीजों को अंजाम देते हैं और कब्ज़ाधारी शक्तियों के नौकरों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। हमें वही बनना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं, वह नहीं जो हमारे उत्पीड़क हमें बनाना चाहते हैं। हमारे रोजमर्रा के विरोध के तरीकों के एवज में मैं बातचीत की व्यर्थ प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं कर रहा हूं—खासकर उस बातचीत का तो बिल्कुल नहीं जिसमें एक पक्ष के पीछे सैन्य शक्तियां खड़ी रहती हैं। बातचीत केवल पारस्परिक समझ के स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में ही संभव है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के स्वतंत्रता के अधिकार को ही नकार दे तो क्या बातचीत हो सकती है? न्याय और अन्याय किस जगह पर मिल सकते हैं? हालांकि, हमें उन चीजों को अनसुना या अनदेखा नहीं करना चाहिए, जो वे हमें दिखा और सुना रहे हैं। कान खोलकर सुनना मित्रता का सबसे अच्छा संकेत है। लेकिन जो मूल तौर पर अन्याय है, उसे हमें शिष्टापूर्वक ठुकरा देना चाहिए।
इस पीड़ा के पल में हमारा मूल कर्तव्य हमारे लोगों के प्रति है, उनके प्रति जो हमारे समाज में चल रहे विरोध की सबसे भारी कीमत चुकाते हैं, गरीब और कमजोर लोग। मेरे विचार उस कश्मीरी मां की ओर जाते हैं जिनकी मैंने हाल ही में तस्वीर देखी थी। उनके साथ एक जाहिल पुलिसवाला धक्का-मुक्की कर रहा था। वह उनका पड़ोसी भी हो सकता था। अभी भी मैं उस छोटे लड़के की तस्वीर अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया हूं, जो अपने भाई की लाश के आगे रो रहा था। उसकी दर्दभरी चीख, जिसने उसके चेहरे का सारा खून सोख लिया, तस्वीर से बाहर निकलकर मेरे ऊपर बम की तरह बरसती है। कोई आज़ादी एक मासूम ज़िंदगी के योग्य नहीं है। हमारे कब्ज़ेदार भी हमसे यही कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे मासूम कश्मीरी जानों को कब्ज़े की आग में झोंकते रहते हैं। हमारे कब्ज़ेदार हमसे हमारे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहते हैं, जहां वे पढ़ सकेंगे कि कैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे, लेकिन वे नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अपनी खुद की लंबे समय से अपेक्षित आज़ादी के बारे में जाने, उस आज़ादी का लुत्फ उठाना तो दूर की बात है। वे हमसे आग्रह ही नहीं करते, बल्कि हमसे मजबूरन अपने लोकतंत्र में वोट पड़वाते हैं, एक ऐसा लोकतंत्र जो वोट डालने की व्यर्थ और बंजर प्रक्रिया में तब्दील कर दिया गया है, ऐसा लोकतंत्र जिसमें हमारे वोट हमारी आवाजों को सशक्त नहीं करते बल्कि सिर्फ यह दिखाने के काम आते हैं कि बहुत से लोग वोट डालने आए थे।
मेरे दोस्तों, अब हम इन सब चीजों को पीछे छोड़ चुके हैं। हमारी कल्पना उनकी सेना से ज्यादा ताकतवर है। वे बारंबार गलत साबित हुए हैं। हमें आज़ादी की भावना को ज़िंदा रखना होगा। हमारे सामने केवल वही एक विकल्प है, क्योंकि हमें किसी और तरह से जीना नहीं आता।
[1] हालांकि कश्मीर में अधिकतर लोग मुसलमान हैं और नए समाज के गठन में इस्लाम की राजनीतिक-कानूनी परंपराओं की ओर देखेंगे, मेरे हिसाब से हमें खुद को सिर्फ उन चीजों में संकुचित नहीं करना चाहिए जो हमें इस्लाम में मिलती हैं, लेकिन जितना उससे ले सकें उतना लेना भी चाहिए। इस ‘चयनात्मक समायोजन’ के कारण कई हैं। मैं यहां उन में से कुछ का उल्लेख कर रहा हूं:
सबसे पहले, मैं इस्लाम को ‘विचार की सुसंगत प्रणाली’ (संपूर्ण विचारधारा या कसकर बंधी हुई इकाई) के रूप में नहीं देखता। बल्कि मुझे इस्लाम की परंपराओं और मूल ग्रंथों में अनेकता, अंतर्विरोध और तार्किक विरोधाभास दिखते हैं, जिनमें से बहुत यकीनन उन ऐतिहासिक/भौगोलिक भिन्नता के कारण उत्पन्न हुए हैं जिनकी वजह से और जिनके द्वारा इस्लाम की व्याख्या करने की कोशिश की गई है। मैं साफ करना चाहता हूं कि इनमें से बहुत-सी व्याख्या काफी उपजाऊ रहीं हैं। इसका सबूत हमें उन भिन्न प्रकार के पंथों, विचारधाराओं, धर्मशास्त्रों, फलसफ़ों और सामाजिक आंदोलनों में मिलता है, जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं।
दूसरा, इस्लाम की व्याख्या करने के लिए, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं हमें करना चाहिए, हमें इस्लाम को किसी तरह के सुसंगत एवं अखंड ग्रंथ की तरह देखना होगा। जबकि एक जीवित वास्तविकता के तौर पर इस्लाम कई तरह के आचरणों, मान्यताओं, आशाओं और आशंकाओं का मिश्रण है, जो बहुत-सी दूसरी परंपराओं और मान्यताओं के साथ अलग-अलग तरह से घुल कर बना है। यह बात उसी पुराने विवाद पर जाकर रुकती है: ‘किसका इस्लाम?’ इसलिए मैं इस्लाम की बात सिर्फ उसके कुछ नैतिक आयामों के संबंध में करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां हमें न्यायोचित मानव सह-अस्तित्व की नींव रखने की सामग्री मिल सकती है।
तीसरा, कश्मीर में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जिस तरह के समाज की मैं कल्पना कर रहा हूं, वह एक चिंता और आशा से निर्देशित है। आज़ादी के आदर्श की शक्ति और भाव सिर्फ एक ही परंपरा से नहीं आने चाहिए। उनको अनेक परंपराओं से खींचकर लाना सिर्फ राजनीतिक जरूरत ही नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है: दूसरों की परंपराओं के प्रति खुले रहने का केवल यही एक तरीका है। समावेशी समाज ‘किसी के स्वामित्व में नहीं, लेकिन सबका होता है’।
आखिर में, हमारे सामने यह सवाल आता है: वह किस तरह का समाज होगा जिसके अधर्मी सदस्य उसके धार्मिक सदस्यों के प्रति सम्मान पूर्ण होने के लिए और जिसके धार्मिक सदस्य उसके अधर्मी सदस्यों या दूसरे धर्म का पालन करने वाले सदस्यों के प्रति सम्मान पूर्ण होने के लिए बाध्य होंगे? ये चिंताऐं उन जगहों के संदर्भ में उठकर आती हैं जहां धर्म या धार्मिक अधिकार के दावों का इस्तेमाल दूसरों को चुप कराने के लिए किया जाता है। ऐसी जगह उन जगहों से अलग नहीं हैं, जहां ‘विज्ञान’ और ‘तर्कसंगतता’ पर विशेष दावे का इस्तेमाल धार्मिक लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। पूर्ण खुलेपन की भावना में हमें इस पारस्परिक दायित्व का प्रोत्साहन करने का तरीका ढूंढना होगा।
[2] पिछले बीस सालों में कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदू न केवल शारीरिक रूप से एक-दूसरे से और एक-दूसरे की ज़िंदगियों से दूर हुए हैं—बल्कि इस अलगाव की वे अलग-अलग कहानियां भी बताते हैं। इन कहानियों के अलग-अलग प्लॉट हैं, षड्यन्त्र के सिद्धांत हैं और मुख्य नायक भी हैं। वे अलग-अलग चीजों को तवज्जो देते हैं, एकतरफा प्यार से लेकर बड़े विश्वासघात तक, और कर्ताओं को स्पष्ट उद्देश्य देते हैं, जबकि उद्देश्यों को इतनी स्पष्टता से माप पाना शायद इतना आसान नहीं है। हालांकि, दो से ज्यादा साफ-सुथरी कहानियां हैं। अनेक कहानियां एक-दूसरे से टकराती हैं और आशंका एवं बेहतर ज्ञान उत्पन्न करती हैं। इन कहानियों को जब अतीत की सद्भाव (या संघर्ष) की कहानियों के साथ रखकर देखा जाता है तो वे विवादास्पद नैतिक-राजनीतिक क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जो प्रबल और तानाशाही आख्यानों को अस्थिर कर सकता है और अलगाववादी राजनीति को रोक सकता है। यह सब तब अधिक पेचीदा हो जाता है जब हिंदू और मुस्लिम (और अन्य समुदायों के) ‘हितों’ को एक-दूसरे से अलग और एक-दूसरे के साथ टकराव में देखा जाता है। मेरे विचार में स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन इस बात का निर्णय भविष्य पर ही छोड़ देना बेहतर होगा। मेरा मानना है कि कश्मीरी मुसलमानों और अन्य समुदायों को अपने हिंदू साथियों का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए और हिंदुओं को बिना किसी शर्त के वापस आने देना चाहिए; इसका मतलब यह है कि कश्मीरी मुसलमानों को हिंदुओं के आगे यह मांग नहीं रखनी चाहिए कि वे अनिवार्य रूप से आज़ादी के लिए कश्मीरी संघर्ष का समर्थन करें (या उसे समझें भी)। और हिंदुओं को यह मांग नहीं रखनी चाहिए कि वे तभी वापस आएंगे जब कश्मीरी अपनी आज़ादी का संघर्ष त्याग देंगे। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि कश्मीरी मुसलमान आज़ादी के संघर्ष के खिलाफ नहीं हो सकते या कश्मीरी हिंदू आज़ादी के संघर्ष में भाग नहीं ले सकते। वे ऐसा कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी है। भारतीय सरकार हिंदुओं के वापस आने को साधारण अवस्था में वापस आने से जोड़ती है—जिसकी परिभाषा उनके हिसाब से आज़ादी के संघर्ष को त्यागना है। हमें इस ‘या तो यह या तो वह’ के झूठे विरोधाभास में नहीं फंसना चाहिए।