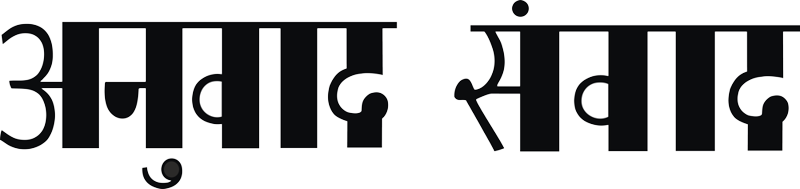Listen to this story
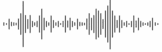
पटचित्र: The Nation
पहला भाग पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - https://anuvadsamvad.com/2022/07/02/kraantikariyon-ke-jeetne-ke-kuch-sanket
अनुवाद: अक्षत जैन और अंशुल राय
स्तोत्र: The Nation
प्रकाशन तिथी: 1965
एक बार क्रांतिकारी संघर्ष जब गुरिल्ला युद्ध की तरहीज पर पहुंचता है तो उसका केन्द्रीय उद्देश्य दुश्मन के नैतिक अलगाव को प्रज्वलित करना, उसे सक्रिय बनाए रखना और उसको संस्थागत ढांचे में पिरोना होता है। यह सब करने के लिए क्रांतिकारी पूर्व के भ्रष्ट प्रशासन के एवज़ में अपना खुद का प्रशासन प्रस्तुत करते हैं। संघर्ष का मुख्य काम सरकार को युद्ध में हराना नहीं बल्कि सरकार से बेहतर प्रशासन चलाना होता है। यह काम प्राथमिक तौर से गांवों में होता है, जहां अधिकतर आबादी निवास करती है और जहां सरकार की पहुंच महज़ शोषण करने वाले कर-संग्राहकर्ता के रूप में होती है। गांव में वहां का प्रधान और उसकी परिषद जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। इस कड़ी को नेस्तनाबूद करने के लिए सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना, संगठन और मेहनत की आवश्यकता होती है। गांव के अधिकारियों को बदलकर या उनका कत्ल करके सरकार को व्यवस्थित ढंग से गांवों से हटाया जाता है, और संघर्ष का राजनीतिक धड़ा गांव की प्रशासन व्यवस्था का कार्यभार उठाता है। क्रांतिकारियों को फिर प्रशासनिक ढांचा बनाना होता है, जिससे वह कर (टैक्स) इकट्ठा कर सकें, थोड़ी शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण का प्रबंध कर सकें और कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां चालू रख सकें। अगर क्रांतिकारी गुरिल्ला संघर्ष के पास जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सब प्रशासनिक ढांचे और व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी और क्रांतिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो वे डाकुओं के गिरोह से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे। ज़मीनी स्तर पर गुरिल्ला संघर्ष का बारीकी से अध्ययन करने वाले लोगों के विपरीत अमरीकी सरकार की समझ है कि गुरिल्ला का कार्य आसान होता है, क्योंकि वे सिर्फ विनाश करते हैं। संघर्ष के इस चरण में सामरिक विरोध से दूरी बनाई जाती है। सरकार भी हत्याओं को पुलिस की समस्या बताती है एवं कर न जमा होने की वजह बुरी फसल, प्रशासनिक भूल इत्यादि बतलाती है। हम जानते हैं कि 1957-60 के दौरान वियतकॉन्ग ने लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण वियतनाम के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यह वही वक्त है जब अमरीकी अंकल डिएम को अंकल हो के प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश कर रहे थे और चारों ओर यह कहते फिर रहे थे: ‘देखो, कोई सैन्य हमला नहीं हो रहा है, अर्थात कोई गुरिल्ला खतरा नहीं है।’
सबसे सम्मोहक, लेकिन साथ ही सबसे आत्मघाती मिथक यह है कि गुरिल्लाओं को जनता का सहयोग आतंक के बल पर मिलता है। गुरिल्ला युद्ध के लिए आवाम का निहायती प्रतिबद्ध लेकिन प्रच्छन्न सहयोग चाहिए होता है, जो बंदूक की नोक पर नहीं मिल सकता। सिर्फ पतित और पराजित गुरिल्ला ही आतंक का सहारा लेकर जनता के समर्थन को खोने का जोखिम उठा सकते हैं। कुछ हुक और मलय, जो हार मानने को तैयार नहीं थे, इस हद तक गिरे भी थे। गुरिल्ला ट्रेनिंग में आमजन के प्रति ‘सही एवं न्यायसंगत’ व्यवहार पर विशेष ज़ोर डाला जाता है। जनरल गियाप के अनुसार, ‘राजनीतिक कार्य सेना की आत्मा है।’
एक चीनी गुरिल्ला विशेषज्ञ समझाते हैं, ‘गुरिल्लाओं को सैन्य-प्रशिक्षण देते समय यह अहम रूप से समझाया जाता है कि वह कैसे इस तरह बर्ताव करें कि उन्हें जनता का सम्पूर्ण समर्थन प्राप्त हो।’
आतंक का इस्तेमाल गुरिल्ला सामाजिक और मानसिक ज़रूरतों के हिसाब से चुनिंदा जगहों पर ही करते हैं। वे सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाते हैं जिनको जनता सामूहिक तौर से दुश्मन मानती है, जैसे अफसर, ज़मींदार इत्यादि।
हालांकि, गांव के सरपंच की हत्या करना अकसर पेचीदा मामला होता है। चूंकि ज्यादातर सरपंच उसी इलाके के किसान होते हैं तो आम लोग उनसे पारंपरिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़े होते हैं। इस कारण उनकी समाज में मान्यता और इज्जत भी होती है। इसीलिए गुरिल्ला की पहली कोशिश यही होती है कि उन्हें संघर्ष से जुड़ने के लिए राज़ी कर लिया जाए। अगर उन्हें शामिल करने में सफलता नहीं मिलती तो बहुत ही सावधानीपूर्वक राजनीतिक जालसाजी से उनके कत्ल की संरचना तैयार की जाती है और जनता को उनका कत्ल वैध मानने के लिए तैयार किया जाता है।
अल्जीरिया की क्रांति के पहले कुछ सालों में एफ.एल.एन को बिना जनता की शत्रुता मोल लिए एक सरपंच को मारने में दो से बारह महीने लग जाते थे, जबकि यह युद्ध औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ था, जिसमें लोगों को मनाना आसान था। इसीलिए जब मैं वियतनाम में था तो मुझे यह सीखकर अचंभा हुआ कि वहां 1957 और 1961 के बीच 13,000 लोकल अफसरों की हत्या की गई थी।
प्रोफेसर बर्नार्ड फॉल इसका स्पष्टीकरण करते हैं: इन अफसरों को डीएम ने नियुक्त किया था जबकि वियतमिन काडर ने देश को फ़्रांस से आजाद कराया था; जनता के दिलों में वियतमिन काडर की तुलना में अफसरों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। और तो और, स्थानीय अफसर अमरीकी हथियारों से लेस और अमरीका द्वारा प्रशिक्षित की गई सेना के साथ मिलकर उन जमींदारों को वापस लाने के घिनौने कार्य में जुट गए थे जो फ़्रांस के खिलाफ लड़े गए युद्ध के दौरान देश छोड़ कर भागे थे। (वियतमिन के राज में वास्तविक तौर पर भूमि सुधार हुआ था।) ये अनुपस्थित ज़मींदार पिछले आठ सालों (1945 से लेकर 1954 तक) का भी भूमिकर मांगने लगे थे। युद्ध से पहले, भूमिकर उपज का पचास प्रतिशत हुआ करता थ। इसका मतलब यह कि अब किसान को उपज का चार सौ प्रतिशत भूमिकर तो देना ही था, उसके साथ जमीन पर अपना अधिकार भी! इस तरह के कामों मे संलग्न अफसरों के कत्ल को स्वीकार करवाने में वियतकॉन्ग को कोई परेशानी नहीं हुई।
क्रांतिकारी खुद को और संघर्ष को जीवित रखने के लिए भी आतंक का उपयोग करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के रॉबर्ट क्लीमन हमको बताते हैं कि वियतनाम के ‘विवादित इलाकों में जहां चालीस फीसद जनता रहती है, लोग दिन में साइगॉन की तरफदारी करते हैं तो रात में वियतकॉन्ग की। क्योंकि दिन में ही सरकार के सेनानी और अफसर वहां मौजूद होते हैं। यह एक पुरानी एशियाई परंपरा है।’ यह आखिरी वाक्य पढ़कर मुझे हंसी आई, क्योंकि मुझे पता है कि यह हमारी परंपरा नहीं है, बल्कि गुरिल्ला युद्ध दुनिया में सभी जगह इसी रीति से लड़ा जाता है। जनता को यह जताना पड़ता है कि वह कम से कम निरपेक्ष है, जिससे कि वह सरकारी सैनिकों की शत्रुता से बच सके। क्रांतिकारी सेनानी और अफसर रात में ‘कहीं पहाड़ से’ नहीं आन टपकते; वे दिन में भी वहीं होते हैं और अकसर सरकार के प्रति आज्ञाकारिता का स्वांग करने में सबसे आगे होते हैं। रात को वही वफादार किसान गुरिल्ला में तब्दील हो जाता है और सब उसे वैसे ही पहचानते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस वफादारी के स्वांग का कोई खुलासा न करे, उन लोगों को उदाहरणात्मक सज़ा दी जाती है जिन पर मुखबिरी करने का शक होता है।
सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने के विलंबित प्रयास को नाकाम करने के लिए दोयम दर्जे के आतंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो अमूमन प्राणघातक नहीं होता। सरकारी स्कूल शिक्षक एवं स्वास्थ्यकर्मी चुनिंदा तौर पर अपहरण और मत परिवर्तन के निशाने पर होते हैं। जून 1962 में दक्षिण वियतनाम में तैनात संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक ने यूनेस्को को बताया कि वियतकॉन्ग ने 1,200 से अधिक स्कूल टीचरों को अगवा कर लिया था। बाईस स्वास्थ्यकर्मियों के कत्ल और साठ के अगवा होने पर सरकार का मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ठप हो गया था। गुरिल्ला आम तौर पर यह ध्यान रखते हैं कि उनकी किसी भी कार्यवाही से जनता को हद से ज़्यादा तकलीफ न झेलनी पड़े और उनकी दीर्घकालिक आर्थिक व्यवस्था को ज़्यादा नुकसान न पहुंचे। उद्योगों और यहां तक कि विदेशी बगानों को भी बख़्श दिया जाता है, बशर्ते वे क्रांतिकारी मोर्चे को ‘कर’ पहुंचाते रहें। जहां सरकार उनकी सुरक्षा करने में नाकाम है, वहां अकसर कर आसानी से दे भी दिया जाता है। (वियतनाम में बड़े यूरोपी रबर के बगानों—जैसे मिशेलिन, एसआईपीएच और टेरे रूश़ आदि—ने थोड़े समय तक कर देने का विरोध किया लेकिन जब वियतकॉन्ग ने उनके फ्रांसीसी निरीक्षकों को अगवा किया तब वे लाइन पर आ गए और कर चुकाने लगें।)
यह कहना मुश्किल है कि सरकार का नैतिक अलगाव आखिर किस हद पर जाकर सम्पूर्ण और अपरिवर्तनीय हो जाता है, जिसके बाद सरकार द्वारा किए गए कोई भी सुधार कार्य या वादे जनता के विरोध को कम करने में असक्षम हो जाते हैं। कम से कम अल्जीरिया में वह हद तब पार हुई जब फ़्रांस ने आम जनता को टॉर्चर करना और मारना शुरू कर दिया, और जनता का ‘पुनर्वर्गीकरण’ करने की कोशिश की। बहुत से अल्जीरियाई नेताओं का मानना है कि उनका क्रांति का संघर्ष तब अपरिवर्तनीय हुआ जब फ़्रांस ने युद्ध के मैदान पर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की—जनरल मासु की क़स्बाह के ऊपर जीत, जिसके चलते अल्जीयर्स के मुस्लिम इलाके को 1957–58 में तहस-नहस कर दिया गया। फ़्रांस अब उन लोगों के सहयोग और विश्वास की उम्मीद नहीं कर सकता था जिन्हें वह अंधाधुंध तरीके से मार रहा था, ऐसा फिर चाहे वह अपने स्वभाव और इच्छा के विपरीत ही क्यों न कर रहा हो।
बुद्धिजीवियों और नरमपंथियों का पलायन अकसर क्रांतिकारी युद्ध के अपरिवर्तनीय होने से ज़्यादा उसकी सफलता का सांकेतिक होता है। खासकर एशियाई मूल के बुद्धिजीवी, जो लोकतांत्रिक और उदारवादी समूह से अपनी पहचान रखते हैं, उनका नजरिया व्यवस्थात्मक हिंसा के प्रति अरुचिपूर्ण होता है। अपनी संस्कृति से अलग-थलग पश्चिमी लिबास ओढ़े हुए ये शहरी बुद्धिजीवी किसानों पर भरोसा तो नहीं करते लेकिन उनकी दशा में सुधार की कामना रखते हैं। जब क्रांतिकारी युद्ध हिंसात्मक हो जाता है, तब ये लोग दोनों पक्षों से समान दूरी बनाकर चलते हैं। लेकिन साथ ही वे यह आशा करते हैं कि हिंसा की धमकियों को आड़ बनाकर सरकार के साथ कुछ सुधारात्मक कार्यों के लिए सौदेबाजी कर पाएंगे। वे देश छोड़कर जाना या क्रांतिकारियों का खुलकर सहयोग करना तब शुरू करते हैं जब यह पक्का हो जाता है कि सरकार ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली और क्रांतिकारी जल्द ही जीत जाएंगे।
क्रांतिकारी युद्ध की सफलता (या सरकार की क्रांतिकारी युद्ध में खुद की ज़मीन पर हार) का एक और संकेत यह भी है कि सरकार किसी दूसरे देश को क्रांतिकारियों का शरणस्थल बताकर उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देती है। क्रांतिकारी युद्ध में सरकार की पेशेवर सेना आक्रमण की तीव्रता बढ़ाने जैसे निर्मम हथकंडे का उपयोग करती है। इतनी उत्कंठा दरअसल उनकी युद्ध के विषय में नासमझी के कारण होती है, तदुपरांत सवाल उनकी प्रभावशीलता पर ही नहीं बल्कि उनकी सारी ट्रेनिंग और व्यवस्था की वैधता पर भी उठने लगता है। यही नहीं, पेशेवर सैनिकों का हौसला बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है, अगर उन्हें यह आभास हो जाता है कि उनका सामना लोकप्रिय विद्रोह से हो रहा है। इसी वजह से सरकार यह विश्वास करने पर मजबूर हो जाती है कि जनता का सहयोग आतंक के इस्तेमाल पर निर्धारित है; और इस आतंक पर अमल करने वाली कोई और नहीं बल्कि पेशेवर सेना है, जिसको विदेशी ताकत संचालित करती है, प्रशिक्षित करती है और हथियार देती है। सरकार चाहती है कि इस सेना से वह खुले मैदान पर लड़े, न कि गुरिल्ला युद्ध में। चूंकि जनता के खिलाफ किया गया प्रतिघात वे नतीजे नहीं दे सकता जिनकी सरकार आशा करती है, इसलिए खुले मैदान पर युद्ध करने का सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है और वह है किसी स्वायत्त देश पर आक्रमण करना। अल्जीरिया में इसी मजबूरी के चलते फ़्रांस ने सुएज़ पर आक्रमण में हिस्सा लिया और ट्यूनीशिया की सीमा पर स्थित टाउन साकीत सिदी यूसेफ़ (Sakiet Sidi Youssef) पर बमबारी की। इन कार्यवाहियों के कारण सेना में कई विद्रोह हुए, जिनमें से आखिरी सैनिक विद्रोह चौथे गणतंत्र (French fourth republic) के गिरने का सबब भी बना। अगर फ़्रांस की सरकार इस दबाव में झुक जाती तो फ़्रांस पहला ऐसा शक्तिशाली देश बनता जो शरणस्थल के अधिकार को मान्यता देने के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का उल्लंघन करता। इस सिद्धांत को तब तक कोरिया, यूनान, सायप्रस और मलय में लागू किया जा चुका था।
एक सक्रिय शरणस्थल के महत्व को कमतर नहीं आंकना चाहिए। हालांकि वह गुरिल्ला युद्ध की सफलता के लिए अनिवार्य नहीं है। क्यूबा, युगोस्लाविया एवं चीन में क्रांतिकारियों के पास सक्रिय शरणस्थल नहीं थे। बर्मा और यूनान में शरणस्थल थे लेकिन उनकी महत्ता सीमित ही थी। राजनीतिक और सामरिक तौर पर गुरिल्ला काफी हद तक आत्मनिर्भर होते हैं और सरहद पार से घुसपैठ बंद भी हो जाए तो भी अनादि समय तक लड़ाई जारी रख सकते हैं। हालांकि, विदेशी मदद का मानसिक और राजनयिक रूप से अपना महत्व होता है। संघर्ष के युद्ध में किसी शक्तिशाली विदेशी दुश्मन पर निर्णायक जीत हासिल नहीं की जा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा यह आशा की जा सकती है कि भारी नुकसान झेलते-झेलते वह इतना थक जाए कि अंतरराष्ट्रीय दबाव डालकर उसे समझौता करने पर मजबूर किया जा सके। विदेशी मदद गुरिल्ला की मांगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, और आज़ादी की उम्मीद को ज़िंदा रखती है। जब क्रांतिकारी सेना अपना कोई विदेशी सहयोगी खो देती है तो इससे उसके सामरिक सहयोग में क्षति नहीं पहुंचती, बल्कि उसकी उम्मीदों को नुकसान पहुंचता है। जब दुनिया की नजरें उन पर नहीं होती, जब राजनयिक प्रतिबंधों और युद्ध के विस्तार के बढ़ने का डर नहीं होता, तब गुरिल्ला के खिलाफ लड़ती हुई औपनिवेशिक सरकार आखिरी चाल चलने के लिए उपयुक्त होती है, वह अकेली चाल जो उसे जीता सकती है—वह नरसंहार या जेनोसाइड करना शुरू कर देती है।
अंततः यह मान लेना कि गुरिल्ला का स्वरूप बाकी सेनाओं की तरह होता है, जिसे किसी बाहरी या विदेशी सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, क्रांतिकारी युद्ध के संस्थागत, राजनीतिक और मानसिक तथ्यों को पूरी तरह से नजरंदाज करना है। ‘घरेलू’ गुरिल्ला के किसी भी विदेशी पर संदेह को कम नहीं समझा जा सकता, फिर चाहे वह विदेशी उसकी खुद की निर्वासित सरकार ही क्यों न हो। ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले साधन-संपन्न एवं ठोस लीडर और काडर हर रोज दुश्मन का सामना करते हैं, कर इकट्ठा करते हैं, प्रशासन चलाते हैं, जनता से वादे करते हैं और उन्हें उम्मीद देते हैं। इनको विदेश से नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होता। वे मित्रता भी मुश्किल से करते हैं और जब करते भी हैं तो इनकी मित्रता शंकापूर्ण और मुश्किलों से भरी होती है। अतः क्षेत्रीय कमाण्डर और राजनीतिक कमिसार अपने इलाकों के राजा होते हैं। वे समूह के रूप में साझे अनुभवों से जुड़े होते हैं, निडरता और संयमित विचार के साथ वे साझा भाव रखते हैं, ‘वहाँ के नेताओं और राजनयिकों’ के प्रति उनका रवैया संदेहपूर्ण होता है कि वे उन्हें बेच खाएंगे, और वे ऐसे किसी भी समझौते को ठुकराने में एकजुट होते हैं जिसको बनाते वक्त उनकी सहमति न ली गई हो।
वियतनाम में संकेत साफ हैं। दक्षिण वियतनाम की सरकार की कोई वैधता नहीं बची है। पश्चिमी ताकतों के सहयोग से बनी कोई भी सरकार उस देश में लोकप्रिय नहीं हो सकती जहां कम्युनिस्ट ने राष्ट्रवाद का रास्ता अपनाकर जनता को आज़ादी और एकता की आशा दी है, और जहां पर पश्चिम-समर्थक लीडर बाओ-डाय, डीएम और म्यूज़िकल चेयर जनरल रहे हैं। (बाओ-डाय वियतनाम का आखिरी सम्राट था, जिसने फ़्रांस और जापान के शासन में राज किया, और जो 1945 में खदेड़े जाने के बाद 1949 में फ़्रांस के शासन में राज करने रिवेरा से वापस आया। डीएम को अमरीका ने 1954 में सत्ता थमाई और उससे अमरीका ने ही 1963 में बौद्ध लोगों का भारी क्रूरता से दमन करने के कारण सत्ता छीनी। म्यूज़िकल चेयर जनरल उन जनरलों को बोला गया जिनको 1963 और 1965 के बीच अमरीका ने थोड़े-थोड़े समय के लिए सत्ता थमाई।)
प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी सहित अमरीका के पूर्व मुख्य सैन्य सलाहकार (लेफ्टिनेंट जनरल सैमुएल टी विलियम्स) भी खुद ऐसा बताते हैं कि आम जनता का कत्लेआम 1960 में ही शुरू हो गया था (अगर डीएम के शासन के दौरान किए गए दमन को न गिना जाए तो)। तब से परिस्थितियां और भी खराब हुईं हैं। बुद्धिजीवी और नरमपंथी या तो भाग गए हैं या गुरिल्ला समर्थक बन गए हैं। उत्तरी वियतनाम पर रोज बमबारी हो रही है। अमरीका और उसके दक्षिण वियतनामी सहयोगी क्रांतिकारी युद्ध हार चुके हैं, क्योंकि वे वियतनाम के लोगों का समर्थन नहीं जीत सके, और अब उनका नैतिक अलगाव सम्पूर्ण है।
एक एशियाई होने के नाते मैं कम्युनिज्म के आकर्षण और उसके खतरों से अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसलिए मैं उन नीतियों का समर्थन करूंगा जो उसके विस्तार को रोकने की संभावना रखती हों। लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि कम्युनिज्म भविष्य की बेजोड़ लहर है, इसीलिए न तो मैं आतंकित हो रहा हूं और न ही शिथिल। मेरा मानना है कि वियतनाम का मसला सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर भी अपने आप मे अनोखा है। मैं आशा करता हूं कि अमरीका वियतनाम में की गई गलतियां अन्य जगहों पर नहीं दोहराएगा। मैं डोमिनो सिद्धांत से सम्मति नहीं रखता और मुझे उन अमरीकियों को देखकर बहुत दुख होता है जो वियतनाम को ‘टेस्ट केस’ बुलाते हैं। वियतनाम दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां पर आज़ादी के संघर्ष के सबसे महत्वपूर्ण सालों में कम्युनिस्ट उसके लीडर थे। नए देशों में जहां लोगों की संस्थाओं के प्रति वफादारी कमजोर होती है, वहां प्रशासन को वैधता और लोकप्रियता राष्ट्रवादी वीरों और शहीदों से मिलती है। यह आजाद विश्व का दुर्भाग्य है कि वियतनाम का जॉर्ज वाशिंगटन या गांधी एक कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी था। यह समझना मुश्किल नहीं है कि हो ची मिन्ह और उसके साथियों (जैसे डिएनबिएनफू में प्रसिद्ध हुए जनरल गिआप) को मॉडर्न वियतनाम के संस्थापकों के रूप में देखा जाता है। यह दूषित आशावाद ही था जिसके चलते यह अपेक्षा की गई कि एक गैरहाज़िर रईस उस लीडर की जगह ले पाएगा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने देश को आज़ादी दिलाने में खपा दी, या फिर ऐसे नेतृत्व या काडर के सामने टिक पाएगा जिसने किसानों के साथ आज़ादी की कठिन लड़ाई में साथ में संघर्ष कर संबंधों में घनिष्ठता पैदा की। वियतनाम की आवाम को निराशा की दहलीज तक पहुंचाने के लिए डीएम को दोषी ठहरना गलत है। उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। जिन परिस्थितियों में वह था, उनमें उसके पास कुछ ही हथियार थे—1) जनता को अनुशासित करने के लिए शक्तिशाली सरकारी तंत्र; 2) अल्पसंख्यक वर्ग का पूर्ण सहयोग; और 3) बड़े पैमाने पर आतंक। ये प्रोग्राम से हटकर नहीं थे, बल्कि प्रोग्राम ही थे।
वियतनाम ऐसा अकेला देश है जहां अमरीका ने औपनिवेशिक सरकार को आजादी के संघर्ष के खिलाफ भारी मात्रा में सहयोग दिया। इससे वियतनाम के लोगों के दिलों में अमरीका के लिए प्यार तो नहीं बढ़ सकता था। फिर दक्षिण में अमरीका ने फ़्रांस की जगह ले ली और फ़्रांस के ही बनाए गए नेता बाओ-डाय का सहयोग किया; उसके बाद अमरीका ने डीएम को ‘वियतकॉन्ग के लोकतांत्रिक विकल्प’ के रूप में पेश किया और देश की एकजुटता के लिए जो चुनाव करवाने का वादा किया था, उससे पल्ला झाड़ लिया। इसलिए वियतनाम के अधिकतर लोगों के लिए मौजूदा युद्ध उनके आजादी के लिए संघर्षरत बने रहने का हिस्सा ही है। मुझे ज्ञात है कि एशियाई अमरीका की करतूतों के बारे में क्या सोचते हैं। वे इसे नया-उपनिवेशवाद बताते हैं; कई को लगता है कि यह साम्राज्यवाद है। मुझे पता है कि ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अमरीकी आज़ादी और न्याय के संघर्ष के प्रति स्वाभाविक तौर पर सहानुभूति रखते हैं, और वे जहां और जितना हो सके मदद करना चाहेंगे। मेरा मानना है कि जो अमरीका वियतनाम जैसे देशों में कर रहा है, उसको ‘मातृवाद’ कहना ज़्यादा वाजिब है, क्योंकि मुझे अमरीका की करतूतें देखकर उस कहानी की याद आती है जिसमें मादा हाथी जंगल में टहलते वक्त मादा तीतर के ऊपर कदम रखती है और उसे मार देती है। मादा तीतर के अनाथ बच्चों को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। ‘आह! मेरे अंदर भी मातृ प्रवृत्ति है’ वह अनाथ तीतरों से कहती है और उनके ऊपर बैठ जाती है।
(इस लेख को एडिट करने में शहादत खान ने मदद की है)