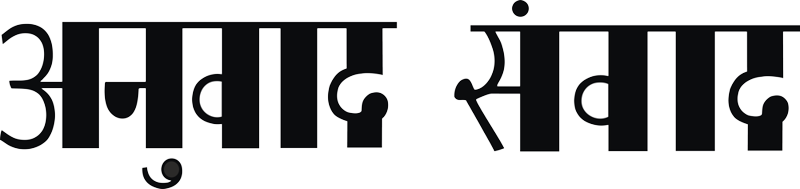Listen to this story
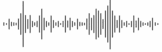
स्त्रोत: Raiot
अधिकार के रूप में विशेषाधिकार
कश्मीर में ऐसी सभाएं प्रायः आयोजित होती रहती हैं जहां बातों के सिवाय कुछ नहीं होता। ये सभाएं कश्मीर के ऊपर चील की तरह चक्कर काटती रहती हैं। जैसे ही हम किसी नवीन संवाद की संभावना पैदा करते हैं, ये सभाएं तेजी से हमारे ऊपर टूट पड़ती हैं और ऐसे संवाद की सभी संभावनाओं को ध्वस्त कर देती हैं। ऐसी ही एक सभा में, एक कश्मीरी पंडित महानुभाव ने वहाँ इकट्ठा हुए लोगों को उस असाधारण यातना की कहानी सुनाई जो उसने अपने कश्मीरी मुसलमान पड़ोसियों के हाथों झेली थी।
सभा की बनावट उल्लेखनीय है: लगभग तीस लोग थे, समान संख्या में कश्मीरी पंडित एवं मुसलमान और एक-दो हिन्दुस्तानी ब्राह्मण| ये ब्राह्मण ही सभा के आयोजक थे। यह सभा ‘पंडितों के मुद्दे’ पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। पंडितों में सिर्फ दो व्यक्ति ही चालीस साल से कम उम्र के थे, जिनमें एक का परिवार विस्थापित हो चुका था और दूसरे का कश्मीर में ही रुक गया था। मुसलमानों में सिर्फ तीन चालीस साल से ऊपर के थे, जिनमें एक औरत थी। कमरे में सिर्फ दो और औरतें थीं—एक कश्मीरी मुसलमान और दूसरी सभा की मुख्य आयोजक, हिन्दुस्तानी ब्राह्मण। मुझे पिछले कुछ वर्षों में यह सीखने को मिला कि ऐसी बनावट आकस्मिक नहीं होती थी; यह ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक सजाई हुई एक सेज थी। परिवर्तन की आशा सिर्फ एक ही चीज़ से की जा सकती थी और वो है ‘मानवीय कारक’: महिलाओं और पुरुषों की स्क्रिप्ट पर न चलने की प्रवृत्ति, एक ताज़े दृष्टिकोण को आज़माने की चाहत। तभी चमड़े के बैगों से नोट बुक निकालकर आयोजक ज़ोरदार तरीके से कुछ लिखने लगते हैं। अगली बार जब आप यह ताज़ा तर्क सुनेंगे तो गड्डी में आए नए पत्तों ने वितर्क तैयार कर रखा होगा या फिर आपको वह तर्क वापस कभी सुनने को ही नहीं मिलेगा क्योंकि जो पत्ता वो तर्क कर रहा था, उसे हटा दिया गया होगा।
हम एक बड़ी विलक्षण गोल टेबल के आसपास बैठे थे। (एक आदेश निकालना चाहिए कि सिर्फ़ उन टेबल को गोल कहा जा सकता है जिनकी विलक्षणता 0.5 से कम हो।) जैसे-जैसे चमकदार रंगों के जैकेट और पतले कोट पहने कश्मीरी नौजवान लड़के और लड़कियां बोलते गए—एक पंडित महानुभाव के शब्दों में, ‘बेअदब’ तरीके से—वैसे-वैसे अधपके बालों और साफ-सुथरे कोट पहने पंडित सज्जन अपना सिर हिलाते गए। एक पंडित सज्जन ‘कश्मीरियत’ की बातें करने लगे और बताने लगे कि कैसे 1990 के पहले सब फल-फूल रहा था। सबसे वरिष्ठ मुस्लिम सज्जन ने बताया कि उन्होंने कश्मीरियत शब्द पहली बार 1990 में भारतीय सेना की प्रेस विज्ञप्ति में सुना था। पंडित युवक, जिसका परिवार विस्थापित नहीं हुआ था, बताने लगा कि कैसे उसके मुसलमान दोस्त उसके साथ मज़ाक किया करते थे कि किसी दिन उसका खतना कर देंगे। उसकी यह बात सुनकर सब खी-खी करके हँसने लगे। एक और पंडित, जो कश्मीर में रुक गए थे, इतने गंभीर मुद्दे का मज़ाक बनाने के लिए सबको फटकारने लगे। ‘तकनीकी’ मुद्दों पर बहुत बखेड़ा हुआ। क्या यह नारा, ‘कशीर बयन पाकिस्तान, बट्टव रोसतय, बटनयव सान’ (कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंडित मर्दों के बगैर मगर पंडित औरतों के संग) सचमुच लोकप्रिय था और आम लोगों के बीच प्रचलित था या यह सिर्फ़ कुछ लोगों की निजी कुंठा थी? क्या किसी और नारे में जाबिरों या काफिरों जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है? कश्मीरी पंडित एक समुदाय हैं, एक वर्ग हैं या एक जाति? एक युवा मुसलमान बुद्धिजीवी ने पूछा, ‘यदि आप एक समुदाय थे और हैं तो क्या जब आप लौटकर वापस आएंगे तो आपमें से कुछ लोग नाई या कसाई का काम करने के लिए तैयार होंगे?’ इस सवाल से कुछ पंडित सज्जन क्रुद्ध हो गए।
धीरे-धीरे एक आम सहमति बनने लगी कि पंडितों का विस्थापन एक अनियमित, गूढ़ और आकस्मिक घटनाक्रम था जो बिल्कुल अप्रत्याशित था। तभी एक दूसरे युवा मुसलमान बुद्धिजीवी ने हस्तक्षेप करते हुए बड़े ही विस्तार से कश्मीर हितैषी समूहों की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिकाओं पर रोशनी डालते हुए भारत के उत्पीड़न से कश्मीर की आजादी के संघर्ष के इतिहास को प्रस्तुत किया; उसने यह भी बताया कि उन समूहों में कई ऐसे गुट थे जिनमें सिर्फ मुसलमान या पंडित शामिल थे और कई मिश्रित गुट भी थे जो अधिकतर वामपंथी थे। सभा का मिजाज बदल गया और लोग ऐतिहासिक शिकायतों और मतभेदों की बातें करने लगे। इससे कुछ पंडित सज्जन उखड़ गए। एक ने अचानक ऊंची आवाज़ में कहा, ‘ये बात सही है कि सब अचानक 1990 में नहीं बदला। उसके पहले से ही इस सबके होने के साफ संकेत मिलने लगे थे। हमारे इलाके में कश्मीरी मुसलमानों ने बंदूक उठाने के बहुत पहले से ही हमारे साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया था।’ जिस बुद्धिजीवी ने कसाई और नाई वाली टिप्पणी पहले की थी, वह इस पंडित सज्जन के इलाके का ही था, उसने पूछा, ‘क्या आप कृपा करके हमें यह बता सकते हैं कि आपको मुसलमानों के हाथों किस तरह का भेदभाव सहना पड़ा था?’ ‘हाँ, क्यों नहीं,’ उसने झट से जवाब दिया, ‘हमारे इलाके में मुसलमानों ने हमारा बहिष्कार 1990 के पहले ही करना शुरू कर दिया था।’ ‘कैसे?’ बुद्धिजीवी ने पूछा। ‘आप लोगों को सरकारी नौकरियां मिलने लगी थीं और आपने हमारे खेतों में काम करना बंद कर दिया था।’ सारे मुसलमान युवक उसकी हंसी के छूटने का इंतज़ार करते हुए उसको घूरकर देखने लगे। वह गंभीर बना रहा।
दुर्भाग्य से, अधिकार और विशेषाधिकार में फर्क ना कर पाने की ये प्रवृत्ति कश्मीरी मुसलमानो और पंडितों के रिश्ते पर अपनी फूहड़ परछाई आज तक डाल रही है। चिंताजनक रूप से बड़ी संख्या में पंडित लोग और संस्थाएँ लगातार एक ऐसी कथा रचने में लगे हुए हैं जो इतनी एकतरफा, रूढ़ और अंतर्विरोधों से भरी हुई है कि उसका समाधान सिर्फ फासीवाद में ही संभव है। ये अनायास नहीं है कि कश्मीरी पंडितों का ‘होलोकास्ट’ (Holocaust) हिन्दू भारत के नए मुखौटे की प्रमुख व्यस्तताओं में से एक है।

तारीख तय कर लें
यहाँ एक मसला है तारीख तय करने का भी है। 19 जनवरी की तारीख को हिंदुस्तान में (लेकिन कश्मीर में नहीं) व्यापक तौर से उस दिन के रूप में मनाया जा रहा है जिस दिन पंडित कश्मीर से विस्थापित होने पर मजबूर किए गए थे। यह तथ्यात्मक रूप से गलत बात है। पंडितों का विस्थापन उस दिन के पहले से ही होना शुरू हो गया था और बड़ी संख्या में उस दिन के बाद भी होता रहा—जैसे कि जनवरी के बचे हुए दिनों में एवं फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी। बहुत सारे पंडितों ने कश्मीर में रुकने का भी निर्णय लिया था, जिसके बारे में पर्याप्त चर्चा नहीं होती। 19 जनवरी 1990 की रात में कुछ खास नहीं था, सिवाय इसके कि उस रात को भारतीय सेना ने सृनगर (Srinagar) में हथियार ढूंढने के लिए बहुत बड़ा डोर-टू-डोर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसका मतलब यह नहीं कि पंडितों के लिए उस समय भय का वातावरण नहीं था, मगर यह भय का वातावरण उनके लिए उस समय तक आम था और 19 जनवरी 1990 की रात के बारे में कुछ भी खास नहीं था। इसका मतलब यह भी नहीं कि कश्मीरी पंडितों के अलावा स्मरणोत्सव को जारी रखने या खारिज करने का अधिकार किसी और को है।
चूंकि यह स्थापित तथ्य नहीं है इसलिए उपयोगी विचार विमर्श सिर्फ़ इसके उद्देश्य और अर्थ का पता करने पर ही हो सकता है। फिर 19 जनवरी को इस तरह उल्लेखित क्यों किया जा रहा है? यह सवाल दरअसल एक साथ दो प्रश्नों को समाहित करता है। लंबे समय के स्मरणोत्सव को मनाने के लिए केवल एक दिन का ही इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? वह दिन 19 जनवरी ही क्यों है, कोई दूसरा दिन क्यों नहीं?
स्पष्टीकरण तक पहुंचने की कोशिश में कई सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। 19 जनवरी की रात उस दिन के ठीक बाद थी जब जगमोहन को दूसरी बार जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह दिन उस राजकीय आतंकवाद के लंबे दौर की शुरुआत को चिन्हित करता है जो दुनिया भर में कभी-कभार ही देखा गया है। जनवरी 22 का दिन गौकदल हत्याकांड को चिन्हित करता है।
ज़ाहिर-सी बात है, एक दिन का स्मरणोत्सव मनाना कई हफ्तों और महीनों तक अपने दुख को विस्तार देने से ज़्यादा समझदारी की बात है। इस उदासीन और मसरूफ़ दुनिया में दुख सहने का वक्त किसके पास है? आप ट्विटर पर अगर हर रोज ‘होलोकास्ट’ लिखेंगे तो आपको ट्रोल घोषित करके खारिज कर दिया जाएगा।

कश्मीरी पंडितों के खाली घर
जो कश्मीरी विस्थापित नहीं हुए, उन्होंने यह सबक अच्छे से सीखा है। इसलिए हम कुनन पोशपोरा और शोपियां का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप से उस संस्थागत यौन शोषण को दर्शाने के लिए करते हैं जो भारतीय सेना द्वारा कश्मीरी औरतों—और मर्दों—के साथ किया गया। (दस हजार से भी ज़्यादा औरतों का बलात्कार किया गया।) वेजिब्योउर (जिसे हिन्दुस्तानी बिजबिहाड़ा कहते हैं), हंडवारा और सोपोर हत्याकांड जिस तरह से भारतीय सेना कश्मीरियों को बेरहमी से मारती आई है उसके प्रतिनिधि उदाहरण बने। (कश्मीर में अभी तक लगभग 70,000 लोग मारे जा चुके हैं।) और ऐसा ही एक उदाहरण गौकदल हत्याकांड भी है। छत्तीसिंघपोरा हत्याकांड दर्शाता है कि कैसे भारतीय राज्य कश्मीर में अल्पसंख्यकों को मरवाता है ताकि वह फूट डालकर शासन कर सके। अल-फरान अपहरण कांड इसका उदाहरण है कि राज्य इस्लामी आतंकवाद के भूत को जगाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। (सरकार समर्थक सैन्य-जनों ने, 'प्रशासन’ की पूरी जानकारी में, गोरे पर्यटकों को अगवा कर लिया था। कुछ समय बाद उनमें से केवल एक का शव मिला और बाकी सब बिना किसी सुराग के गायब कर दिए गए। सच बाहर आने से पहले काफी दिनों तक आज़ादीपरस्त मिलिटेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था।) एपीडीपी (लापता लोगों के माता-पिता की समिति) उन दस हज़ार कश्मीरियों का स्मरणोत्सव महीने में एक बार मनाती है जिन्हें जबरन लापता कर दिया गया। अगर हम हर कत्ल, बलात्कार, जबरन गायब कर दिए जाने, घर की तबाही, टॉर्चर सेशन, मारपीट, क्रैक डाउन और अवमानना को अंकित करें तो हमें इसके लिए सात महाद्वीपों से भी बड़े कैलंडर की ज़रूरत होगी।
तो हाँ, दिन चिह्नित करने से, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, मदद तो होती ही है। मगर इसके साथ दूसरी समस्याएं भी आती हैं। हिंदुस्तान में और उसके बाहर कुछ ऐसे लोग हैं, जिनमें कुछ कश्मीरी भी हैं, जो यह मानते हैं कि जिस तरह से बलात्कार को कश्मीर में युद्ध के साधन की तरह इस्तेमाल किया गया है, उसका समाधान कुनन पोशपोर जैसे मामलों में किसी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप से किया जा सकता है। वैसे ही जबरन विस्थापन के लिए किसी एक दिन को चिह्नित करने का तात्पर्य है जो विस्थापित हुए और जिन्होंने उन्हें विस्थापित होने पर मजबूर किया उन लोगों के बीच एक साफ-सुथरा सामंजस्य बनाया जा सकता है।
सृनगर में शहीदों के कब्रिस्तान में रोती हुई एक माँ
नफरत से भरी टोकरी
यह एक महत्वपूर्ण मामला है। दो प्रमुख टोकरियाँ हैं, जिनमें कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के तथ्य एवं तर्क के अंडे हैं। पहली टोकरी की सामग्री कुछ इस प्रकार है: कश्मीरी मुसलमान और पंडित अलग अलग समुदाय हैं जो एक दूसरे से आठ सौ सालों से नफरत करते आए हैं, तब से जब से निचली जाति के कश्मीरी सामूहिक रूप से इस्लाम में परिवर्तित हुए और जिससे कश्मीर बहुसंख्यक रूप से मुसलमान समाज बना और उच्च जाति के ब्राह्मणों से वैचारिक श्रेष्ठता छिन गई (सैद्धांतिक रूप से सारे मुसलमान बराबर होते हैं)। कश्मीर के इतिहास में जब भी इन दोनों अखंड समूहों में से कोई एक किसी विदेशी के साथ जुड़ा है, तो उसे दूसरे समूह की तुलना में ज्यादा लाभ मिला है। बीसवीं सदी की शुरुआत में पंडितों की स्थिति मज़बूत थी क्योंकि वे हिन्दू डोगरा शासकों के साथ जुड़े हुए थे। उनके पास बेहूदा तौर पर भारी मात्रा में ज़मीनें एवं संपत्तियां थी और नौकरशाही में भी उनका ही प्रभुत्व था।
जब कश्मीर पर हिंदुस्तान का राज शुरू हुआ, तब भारतीय सरकार की प्रजातंत्र को लेकर कुछ गलत धारणाएं थीं, जिनके तहत उसने कश्मीरियों से जनमत-संग्रह (Plebiscite) का वादा कर डाला। उसने कश्मीरी पंडितों की कीमत पर कश्मीरी मुसलमानों की सनक को बढ़ावा दिया और ऐसे भूमि वितरण कार्यक्रम की इजाज़त दी जो उस समय से आज तक का सबसे उग्र कार्यक्रम माना जाता है। इसके अंतर्गत जोतने वालों को (जो कि अधिकतर मुसलमान थे) मालिकाना हक मिला, जिससे पंडित ज़मींदारों को अपनी जागीरों से वंचित होना पड़ा। इससे ऐसी स्थिति भी बनी जिससे मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, परिणामस्वरूप कुछ कश्मीरी मुसलमान सरकारी विभागों और नौकरशाही के उन ऊंचे स्तरों तक पहुंच गए जो पहले कश्मीरी पंडितों की जागीर हुआ करते थे।
भारत सरकार की तरफ से इतनी उदारता के बाद भी एहसान फरामोश कश्मीरी स्वाधीनता के अधिकार की मांग करते रहे। तमाम धांधलीपूर्ण चुनावों के बाद वे गुट बनाकर पाकिस्तान गए और वहां से बंदूकें एवं गोला बारूद ले कर लौटे। उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। भारत सरकार का ढांचा पूरी तरह से ढह गया। कश्मीरी पंडित कश्मीर में भारतीय राज्य के प्रतिनिधि थे और उनको तीन विकल्प दिए गए, ‘रालिव, गालिव, या चालिव’ (मिलना—मुसलमानों के साथ; घुलना—यानी मर जाना, अपना विनाश करना; या भागना)। ज़ाहिर है कि वे राष्ट्रविरोधी कश्मीरी मुसलमानों के साथ नहीं मिल सकते थे, तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था और वह था भागना।
मगर हिन्दू भारत उनके प्रति दयावान साबित नहीं हुआ। उसने उन्हें प्रवासी शिविरों में सड़ने के लिए छोड़ दिया। उनके वापस लौटने की परिस्थितियां भी नहीं बनाई।
इस टोकरी में सुलह के अंडे नहीं हैं। अगर कश्मीरी पंडित भारतीय राज्य के अविभाज्य अंग हैं और अगर सशस्त्र कश्मीरी लड़ाकों और गैर-लड़ाकों में कोई अंतर नहीं है तो सुलह की गुंजाइश ही कहां रहती है? यह तो एक सम्पूर्ण युद्ध है, जो सिर्फ़ कश्मीरी मुसलमानों के सम्पूर्ण उन्मूलन से ही खत्म हो सकता है।
इस टोकरी में दोनों तरीके के पंडित शामिल हैं—वे जो बेहतर ज़िंदगी और नौकरी की तलाश में 1990 के बहुत पहले ही हिंदुस्तान चले गए थे (जैसे अनुपम खेर—कश्मीर खूबसूरत तो होगा मगर वह छोटी जगह है) और वे जो 1990 में—‘नरसंहार के शिकार’ के रूप में—विस्थापित हुए थे। यह एक रोचक तरीका है जिससे नंबर बढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आंकड़े (भारतीय सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 219 कश्मीरी पंडित मारे गए, मानवाधिकार समूह कहते हैं 629) उन्हे कोई जंग जितवा देंगे।
1990 में कश्मीर में दो लाख कश्मीरी पंडित थे। सभी विस्थापित तो हुए नहीं। तो विस्थापित होने वालों का नंबर ज़रूर एक से दो लाख के बीच ही होगा। लेकिन क्या इससे लोगों का अपने घरों से जबरन बाहर निकाले जाने का दुख कम हो जाता है? क्या इससे जो गुनहगार हैं उनका दोष कम हो जाता है? क्या हम मानवीय इतिहास के ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमारे पास नरसंहार से कम किसी चीज के लिए वक्त नहीं है?
नरसंहार पर एक दूसरा पहलू भी है। जैसा कि मोहम्मद जुनैद ने बिल्कुल अलग संदर्भ में कहा है—अगर कोई ताकत ‘लोगों के विनाश की उम्मीद, अपेक्षा, विचार, योजना, या रणनीति बना रही है, तो क्या वह नरसंहार है?’ कई समीक्षक यह तो मानते हैं कि 1990 से कश्मीर में पंडितों के मारे जाने की संख्या भारतीय सरकार और मानवाधिकार समूह के आंकड़ों के बीच ही कहीं है, मगर तब वे यह तर्क देते हैं कि यह फिर भी सांस्कृतिक नरसंहार है, क्योंकि विस्थापन से जीने का एक तरीका पूरी तरह नष्ट हो गया है।
इसका व्याख्यान करने के लिए कि जीने का वह तरीका क्या था, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पंडितों का तो जन्म ही बौद्धिक वर्ग में जाने के लिए हुआ था और मुसलमानों के लिए मज़दूरी करने के रास्ते खुले हुए थे। मुसलमान लोग पंडितों का ज्ञान के रखवालों के रूप में सम्मान करते थे। अगर मुसलमान शिक्षा प्राप्त कर भी लेते थे, तो इसके लिए उन्हें पंडित शिक्षकों का आभारी होना पड़ता था। पंडितों के पास बेहूदा तौर पर उपजाऊ ज़मीन, बगीचे, उद्योग, सरकारी नौकरियां, निजी क्षेत्र के उद्यम, और बेहतर एवं बड़े घर इसलिए थे क्योंकि वे मुसलमानों से ज़्यादा प्रतिभाशाली एवं मेहनतकश थे, जब कि मुसलमान अपनी दैनिक कमाई अपने नाती फोल यानी गोश्त के टुकड़े पर ही खर्च करके गंवा देते थे। बहुत सारे पंडित यह सब खुलकर बोलते हैं। उन्हें अपने बाग याद आते हैं, उन्हें अपने आँगन में लगे चेरी, बादाम, नाशपाती एवं सेब के पेड़, एवं सुसज्जित तरीके से बने हुए विशाल घर और पुस्तकालय भी याद आते हैं। उन्हें कश्मीर के मौसम की याद आती है। जब भी वे कश्मीरी मुसलमान का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि वह हमेशा से मूर्ख ही रहा है, जिसे पाकिस्तान से लेकर बुर्किना फासो तक कोई भी बेवकूफ बना सकता है; वह एक खतरनाक बर्बर प्राणी है जिसकी हिंसा उसकी जहालत से पैदा होती है; वह एक ऐसा वहशी है, जिसे जब पंडितों के घरों में आने कि इजाज़त मिली या जिसने उनके घर विस्थापन के बाद ‘कौड़ियों के दाम’ खरीदे, तब भी वह गधे का गधा ही रहा और उसने उनके घरों के खूबसूरत अग्रभागों का और कोमलता से बोए हुए पेड़ों का विनाश कर दिया। वे श्रद्धालु कश्मीरी मुसलमान को याद करते हैं।
ज़ाहिर है कि जीने के ऐसे तरीके की कोई भी स्वाभिमानी कश्मीरी मुसलमान वापसी नहीं चाहेगा।
क्या जीने के सारे तरीके पवित्र होते हैं?
अतः इस टोकरी का सार है कौटिल्य की दिखाई कूटनीति जिसका नाम है संसार—कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ अपने शक्तिशाली मित्र हिन्दू भारत के साथ जुड़ें। इस सार की तर्कसंगतता प्राचीन है: हिंदुस्तान में ब्राह्मणवाद को हिन्दू धर्म ने संभाला हुआ है (अगर आप उन दोनों में भेद करना चाहते हैं तो) मगर अधिकांश लोगों के मुसलमान बनने के बाद कश्मीर में ब्राह्मणवाद को बनाए रखने के लिए हमेशा से (और आज भी) किसी न किसी विदेशी ताकत की ज़रूरत पड़ती रही है।
इस टोकरी में एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं है। अगर सरकार कश्मीरी मुसलमानों पर ऐसा खौफनाक अत्याचार करने की काबिलियत रखती है—जिसमें नियमित तौर पर चुन-चुनकर घेरना, कत्ल करना, गिरफ्तारियां, टॉर्चर, हत्याकांड, इत्यादि शामिल थे (22 जनवरी 1990 को गौकदल हत्याकांड हुआ था जिसमें 51 लोग भारतीय सेना द्वारा पुल पर मारे गए और कुछ 250 घायल हुए, 25 जनवरी 1990 को हंडवारा में बीएसएफ ने 26 नागरिकों का कत्लेआम किया)—तो ऐसा कैसे हुआ कि वह कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करने में असमर्थ रही और उनका विस्थापन नहीं रोक पाई? राज्य का तंत्र इतने चुनिंदा रूप से और इतनी बुरी तरीके से फ़ेल क्यों हो गया?
यह टोकरी कश्मीरी मुसलमानों को बेचने के लिए नहीं है। यह तो भारतीय राज्य, हिन्दू भारत और ‘इस्लामोफ़ोबिया’ (islamophobia) की सर्वव्यापक श्रेणी के लिए है।
और एक टोकरी उम्मीद की
दूसरी टोकरी की सामग्री कुछ ऐसी है: कश्मीर का इतिहास उतना ही विविध रहा है जितना कि दुनिया में किसी भी और जगह का रहा है। उसमें भी अर्थव्यवस्था, धार्मिकता, स्थान, भाषा, रिश्तेदारी और इतिहास की सरल एवं जटिल परस्पर क्रिया पर आधारित हितधारी समूह रहे हैं। इन हितधारी समूहों ने एक-दूसरे पर हावी होने के लिए हर तरह के प्रयास किए, जिसमें बाहर वालों से दोस्ती, उत्पीड़न और युद्ध करना शामिल हैं। अंग्रेज डोगराओं को कश्मीर में लेकर आए, लेकिन विडंबना यह भी है कि उन्होंने कश्मीरियों को प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद से भी अवगत कराया। पंडितों और शक्तिशाली मुसलमानों का एक छोटा वर्ग, जो कि पंडितों के मुकाबले संख्या में काफी कम था, डोगरा के साथ जुड़ गया। बहुसंख्यक कश्मीरी किसान वर्ग और बचा हुआ मज़दूर वर्ग, जोकि लगभग सारे ही मुसलमान थे, कष्ट और नितान्त गरीबी का जीवन जीते रहे। आधुनिक शिक्षा और लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, साम्यवाद, इत्यादि जैसे विचारों की बढ़त से कई सारे कश्मीरी पंडित और मुसलमान, अधिकांश वामपंथी, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने को प्रभावित हुए।
कश्मीर पर हिंदुस्तान के शासन की शुरुआत में ऐसी ही स्थिति थी। हिंदुस्तान ने प्रजातंत्र की अवधारणा का अनुष्ठानिक अभिवादन करते हुए ब्राह्मण हुकूमत पेश की। इस स्थिति पर कई प्रतिक्रियाएं आईं। वामपंथी कश्मीरियों को न तो ब्राह्मण हुकूमत चाहिए थी और न ही हिंदुओं की प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, लेकिन उन्हें बाद वाले विकल्प में दांव-पेंच की वे संभावनाएं दिखीं जिससे वे अपने अंतिम लक्ष्य यानी आज़ादी की ओर पहुंच सकें। इस्लामवादियों ने, जिनमें बहुत से पाकिस्तान समर्थक थे, दोनों ही विकल्पों को नामंज़ूर कर दिया लेकिन कई महत्वपूर्ण अवसरों पर नीतिगत शांति का रास्ता चुना (इस्लामवादियों को नीतिगत शांति बहुत पसंद है)। उच्च वर्गीय कश्मीरी, पंडित और मुसलमान दोनों, तत्कालीन उलझनों में बहुत सारी जायदाद खो बैठे, मगर उन्होंने शासकों यानी भारतीय राज्य के साथ जुड़ने की कोशिश शुरू की जिससे वे बची खुची जायदाद को अपने पास रख सकें।
क्योंकि उच्च वर्गीय पंडितों और मुसलमानों के बीच अंतर्विवाह की कोई संभावनाएँ नहीं थीं और वे दोनों राज्य से एक समान समर्थन मांग रहे थे, इसलिए दोनों के बीच द्वेषपूर्ण प्रतिद्वंद्विता बढ़ती गई। अपनी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए भारतीय राज्य ने पंडितों को कंप्रडर (comprador) मुसलमानों के ऊपर चुना (इसलिए भी क्योंकि बहुत से कश्मीरी पंडित खुद ही राज्य थे)। दोनों युद्धरत गुट अपने आपको मजबूत करने का प्रयास करने लगे। पंडित चूंकि संख्या में बहुत कम थे, इसलिए उच्च वर्गीय पंडितों ने भारतीय राज्य को और ज़ोर से गले लगाने का एवं अन्य पंडितों को मुफस्सिल से खींचकर सरकार के कार्यों में लगाने का भी प्रयास किया। मुसलमान इस बात से क्रोधित हुए कि पंडित शासन कला का पवित्र ज्ञान अपने परिचित मुसलमानों की जगह अनजान पंडितों को दे रहे थे। उच्च वर्गीय मुसलमान प्रजातंत्र या बहुसंख्यकवाद के भूत को इस्तेमाल करने का प्रयास करने लगे। पंडितों ने देखा कि मुसलमान अपने आपको बड़े राजनीतिक दलों में संगठित कर रहे हैं और उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी।
इस दौरान, बहुसंख्यक कश्मीरी, जिनमें बहुत अल्प-संख्या में पंडित भी शामिल थे, अपने छोटे-मोटे और शांतिपूर्ण आज़ादी के आंदोलन से तंग आ रहे थे। एक मुकाम पर ऐसी समझ विकसित हुई कि आंदोलन को बढ़ाना होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल (line of control) पहले युवा कश्मीरियों के पसीने में डूबी और फिर उनके खून में, ये वे लोग थे जो बॉर्डर पार जाकर बंदूकें लेकर लौट रहे थे और आज़ादी के लिए जान लेने एवं देने को तैयार थे। और उन्होंने यही किया भी। जो कोई भी भारतीय राज्य को सहयोग करता, वह व्यक्ति खुला निशाना बनता, जैसे आज़ादीपरस्त लोग चालीस से भी ज़्यादा सालों से बन रहे थे। जंग पुरानी थी मगर अब दोनों पक्षों के पास सेना थी। लोगों को पक्ष चुनना पड़ा।
जिन लोगों को युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे या तो कश्मीर से भाग गए या सेना के पास सुरक्षा के लिए इस आशा में चले गए कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। भारतीय राज्य ने आतंक का शासनकाल शुरू कर दिया। कश्मीरी बहादुरी से लड़े मगर उनकी बंदूकें कम पड़ गईं। बीस साल और 70,000 कश्मीरियों के मरने के बाद, युद्ध हल्का तो हुआ है लेकिन अभी भी उसी आक्रोश से चल रहा है। कश्मीरियों ने अपनी लड़ाई को अमर बनाने के लिए अपनी कई पराजयों को स्मरणोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया। भारतीय राज्य को यह पता है और वह जीत का दावा करने के लिए मचल रहा है, मगर उसकी जगह वह पूरा युद्ध ही नकार रहा है, जिससे कश्मीरियों से उनकी हार भी छीनी जा सके। इसी बीच जो लोग कश्मीर छोड़कर भाग गए थे, उन्हें यह समझ आ गया कि हिंदुस्तान उनका उतना अपना नहीं है जितना वे उसको अपना बनाना चाहते थे। उन्हें कुछ खोने का एहसास है। वे वापस लौटना चाहते हैं, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए और अगली पीढ़ी इसकी बिल्कुल परवाह ही न करे।
सिर्फ दूसरी टोकरी ही मुसलमान और पंडित दोनों खरीददार चाहती है। इस टोकरी में कुछ खराब अंडे हैं, मगर इसमें उम्मीद के भी अंडे हैं।
स्वयं का खंडन करने वाले विचार
पिछले कुछ सालों में एक टोकरी को दूसरी टोकरी में खाली करने का प्रयास हुआ है, जिसका हिन्दू भारत की तरफ ज़्यादा खिंचाव है। यह अंडों को तोड़े बिना नहीं किया जा सकता, सारे अंडों को। बढ़ती मात्रा में कश्मीरी पंडित समीक्षक कुछ चुनिंदा स्मृतियों पर आंशिक शोक जताने के लिए उतर आए हैं। एक ओर, आज़ादी की राजनीति को पूरी तरह से नज़रंदाज किया जा रहा है। दूसरी ओर, कश्मीरी मुसलमानों पर ज़ोर डाला जा रहा है कि वे विस्थापित कश्मीरी पंडितों का स्वागत करें। पंडित विस्थापन के उपदेश को सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह खुद को ही हराने वाला एजेंडा है।
कश्मीरियों की कई पीढ़ियों ने इस आलंकारिक प्रश्न, ‘हम क्या चाहते’, का जवाब ‘आज़ादी’ से दिया है, हिंदुस्तान से आज़ादी। अगर सुलह की कोई भी संभावना है तो इसका जवाब किसी दूसरे प्रश्न से नहीं दिया जा सकता: ‘कश्मीरी पंडितों का क्या?’ इस आखिरी सवाल का जवाब एक दूसरे सवाल के जवाब का हिस्सा हो सकता है और होना भी चाहिए ‘आज़ादी का मतलब क्या?’ मगर इसके हो पाने के लिए पहले वाले सवाल को सुनना भी पड़ेगा और उसका जवाब भी देना पड़ेगा।
(इस लेख को एडिट करने में अविनाश पांडे ने मदद की है)