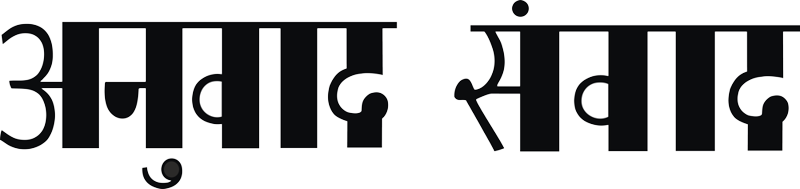Listen to this story
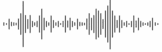
अनुवादक: शहादत और अक्षत
स्रोत: Outlook Magazine
राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद की जगह पर सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, अब हिंदुत्व की ताक़तों ने बाबर से ध्यान हटाकर औरंगज़ेब आलमगीर पर निशाना साधा है—जो मुग़ल साम्राज्य के छठे और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले बादशाह थे, और जिनका शासन दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली सल्तनतों में गिना जाता है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए लिखे गए औपनिवेशिक आख्यानों में अक्सर औरंगजेब को एक क्रूर, कट्टर और हिंदू विरोधी शासक के रूप में दर्शाया जाता था। यही एकतरफ़ा और तोड़ी-मरोड़ी गई छवि अब हिंदुत्व की राजनीति के लिए एक मुफ़ीद औज़ार बन चुकी है।
लेकिन औरंगज़ेब का ऐतिहासिक मूल्यांकन कहीं ज़्यादा जटिल और सन्दर्भ-संपन्न है। आख़िरकार, वे एक सामंती दौर के शासक थे, जो अपने समय की सीमाओं, सोच और सत्ता के ढांचे में काम कर रहे थे। इसके उलट, आज की हिंदुत्ववादी राजनीति उन्हीं विभाजनकारी और दमनकारी प्रवृत्तियों को लोकतांत्रिक भारत में दोहराने की कोशिश कर रही है—और ऐसा करते हुए वो उन संवैधानिक मर्यादाओं को चोट पहुँचा रही है जिन्हें भारत की जनता ने साझे विश्वास और न्याय के मूल्यों पर आधारित कर के चुना था।
इतिहास के रूप में मिथक
हिंदुत्व की ताक़तें लंबे समय से मिथकों को इतिहास की तरह पेश करके अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में माहिर रही हैं। वे औरंगज़ेब के नाम पर बसे ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर पहले ही ‘छत्रपति संभाजीनगर’ करवा चुकी हैं। जबकि इतिहास में औरंगाबाद का महत्व औरंगज़ेब के शासनकाल में एक प्रमुख प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में रहा है—इसकी पहचान मुग़ल काल की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है। नाम बदलने की यह कोशिश दरअसल उस इतिहास को मिटाने और एक ऐसा नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास है जो हिंदुत्व की विचारधारा के अनुरूप हो।
दिलचस्प बात यह है कि उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में कहीं भी यह प्रमाण नहीं मिलता कि शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी का औरंगाबाद से कोई सीधा संबंध रहा हो। यह नामकरण ज़्यादा औरंगज़ेब को खलनायक बनाने और मराठा प्रतीकों को महिमामंडित करने का प्रयास लगता है, न कि किसी ठोस ऐतिहासिक आधार पर आधारित निर्णय।
हाल ही में बॉलीवुड फिल्म छावा की रिलीज के साथ औरंगजेब-विरोधी बयानबाजी ने और जोर पकड़ लिया है। मराठा और मुगल सेना के बीच संघर्ष को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने के साथ यह फ़िल्म औरंगजेब को एक क्रूर और अत्याचारी शासक के रूप में चित्रित करती है। यह फ़िल्म उस व्यापक रुझान का हिस्सा है जिसमें बॉलीवुड हिंदुत्व के नैरेटिव को मज़बूती देने वाले सिनेमा का एक माध्यम बनता जा रहा है — जैसे कि द केरल स्टोरी, द कश्मीर फ़ाइल्स, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, इमरजेंसी और आर्टिकल 370 जैसी फ़िल्में। इनमें से कई फिल्मों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेताओं द्वारा खुलकर प्रमोट किया गया, जिससे इन कहानियों को राजनीतिक वैधता और संस्थागत समर्थन भी हासिल हुआ।
छावा फ़िल्म ने साम्प्रदायिक तनाव भड़काने में एक अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद औरंगाबाद के पास स्थित खुल्दाबाद में औरंगज़ेब की सादगीपूर्ण क़ब्र को गिराने की माँगें उठने लगीं। इस पूरे घटनाक्रम का अंजाम नागपुर में हुए साम्प्रदायिक टकरावों के रूप में सामने आया—एक ऐसा शहर जिसे अब तक हिन्दू-मुस्लिम संघर्षों के संदर्भ में नहीं जाना जाता था। महाराष्ट्र में इस तरह तनाव का उभरना महज़ इत्तेफ़ाक़ नहीं है; यह भावनात्मक और विभाजनकारी मुद्दों को सुनियोजित ढंग से भुनाने की रणनीति है, जो एक साफ़ राजनीतिक मक़सद के तहत की जा रही है।
इस तरह के विवाद जानबूझकर इसीलिए खड़े किए जा रहे हैं ताकि आम लोगों की रोज़मर्रा की जद्दोजहद, उनकी आजीविका और ज़िंदगी से जुड़े असल सवालों से ध्यान हटाया जा सके—और उनकी चेतना को एक काल्पनिक ‘स्वर्णिम अतीत’ के नशे में डुबो दिया जाए, जिसे गढ़े गए और तोड़े-मरोड़े गए इतिहास के ज़रिए पेश किया जा रहा है।
एक-पक्षीय चित्रण
औरंगज़ेब की आलोचना अक्सर इस बात को लेकर की जाती है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की उदार नीतियों से अलग राह अपनाई। उनके सत्ता में आने की प्रक्रिया—जिसमें उन्होंने अपने भाइयों को मरवा दिया और अपने पिता शाहजहाँ को क़ैद कर लिया—को अक्सर उनकी बेरहमी का प्रमाण माना जाता है। लेकिन उस दौर की राजसत्ताओं में ऐसे घटनाक्रम असामान्य नहीं थे। उस समय उत्तराधिकार की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, जिससे अक्सर भाइयों के बीच हिंसक संघर्ष होते थे।
उदाहरण के लिए, उस्मानी (Ottoman) साम्राज्य में सत्ता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भाई-वध को बाक़ायदा संस्थागत रूप दिया गया था—सुल्तान मेहमत द्वितीय ने इसे राज्यहित में वैध करार दिया था। हमारे अपने इतिहास में, छत्रपति संभाजी ने भी शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में जब आंतरिक कलह का सामना किया, तो उन्होंने अपनी सौतेली माँ सोयराबाई को बंदी बनाकर राजगद्दी पर नियंत्रण स्थापित किया। ऐसे सत्ता संघर्ष राजपूतों की रियासतों, विजयनगर साम्राज्य, नेपाल के मल्ल वंश और दक्षिण भारत के नायक राजाओं के इतिहास में भी आम मिलते हैं।
औरंगज़ेब की कार्रवाइयाँ दरअसल उस समय की राजशाही राजनीति की कठोर हक़ीक़तों को दर्शाती थीं—ये न तो उनके व्यक्तित्व की कोई अनोखी विशेषता थी और न ही उनके मज़हब का परिणाम।
एक और आम आलोचना यह की जाती है कि औरंगज़ेब ने 1679 में गैर-मुसलमानों पर जज़िया दोबारा लागू किया। जज़िया, जो इस्लामी क़ानून में निहित है, दरअसल एक ऐसा टैक्स था जो गैर-मुस्लिम प्रजा (धिम्मियों) पर लगाया जाता था—इसके बदले उन्हें सैन्य सेवा से छूट और राज्य की सुरक्षा मिलती थी। यह कर सिर्फ़ उन सक्षम गैर-मुस्लिम युवाओं पर लगाया जाता था जिन्होंने सेना में सेवा देने से इनकार किया हो।
जज़िया को लागू करने का मुख्य कारण धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक था। औरंगज़ेब के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य पर भारी वित्तीय दबाव था—लगातार सैन्य अभियानों, कृषि उत्पादन में गिरावट और व्यापार में अवरोधों के चलते राज्य की आमदनी पर असर पड़ा था। ऐसे में गैर-मुस्लिम आबादी के एक व्यापक हिस्से पर कर लगाने से राजकोष को ज़रूरी राहत मिली।
राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जज़िया औरंगज़ेब की सत्ता को मज़बूत करने का एक उपाय था—एक ऐसे समय में जब उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था: राजपूतों के विद्रोह, शिवाजी के नेतृत्व में उभरती मराठा शक्ति, दरबारी अशराफ़ी में असंतोष और सफ़वी साम्राज्य व मध्य एशिया से बाहरी ख़तरे। इन परिस्थितियों में औरंगज़ेब ने रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम वर्गों के साथ अपनी पहचान को जोड़ते हुए अपनी वैधता को मज़बूत करने की कोशिश की, ताकि साम्राज्य के पारंपरिक घटकों का समर्थन बनाए रखा जा सके।
लेकिन इस नीति का दूसरा पहलू यह था कि इससे गैर-मुस्लिम समुदायों, विशेष रूप से हिन्दू और जैन करदाताओं में नाराज़गी बढ़ी। इससे पुराने सहयोगियों—जैसे राजपूतों—के साथ संबंधों में भी खटास आई। यह साम्प्रदायिक तनावों को और गहरा करने वाला कारक बना, जिसने असंतोष को बढ़ाया और एक ऐसी विभाजनकारी विरासत छोड़ी जिसे औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी संभाल नहीं सके।
एक जटिल और संतुलित छवि
औरंगज़ेब की छवि को अक्सर हिन्दू-विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि उनकी नीतियाँ एक कहीं अधिक जटिल और व्यावहारिक शासन दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर व्यावहारिकता अपनाते हुए बड़ी संख्या में हिन्दुओं को अपने शासन में शामिल किया। इतिहासकार पार्वती शर्मा लिखती हैं कि जहाँ अकबर के दरबार में 14 हिन्दू मनसबदार थे, वहीं औरंगज़ेब के शासनकाल में यह संख्या 148 तक पहुँच गई थी। शाहजहाँ के समय कुल मनसबदारों में हिन्दुओं की हिस्सेदारी जहाँ 24.5% थी, वहीं औरंगज़ेब के शासन में यह बढ़कर 30% से भी अधिक हो गई—जो दर्शाता है कि उनकी नियुक्तियाँ मज़हबी पहचान की बजाय योग्यता पर आधारित थीं।
राजा जसवंत सिंह (मारवाड़) और राजा जय सिंह (आमेर) जैसे दो हिन्दू सरदारों को ख़ज़ाने जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा भी कई हिन्दू अधिकारी उच्च पदों पर तैनात थे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि औरंगज़ेब के शासन की कई प्रमुख नीतियाँ इन्हीं हिन्दू अधिकारियों द्वारा बनाई गई थीं। यह मुग़ल प्रशासन की उस परंपरा का हिस्सा था जिसमें शासक वर्ग को विविध जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमियों से तैयार किया जाता था—जिसमें मध्य एशियाई, ईरानी, अफ़ग़ान, भारतीय मुसलमान और राजपूत सभी शामिल थे। इस विविधता का उद्देश्य सत्ता के संतुलन को बनाए रखना था, ताकि कोई एक वर्ग शासन पर हावी न हो सके—और यही मुग़ल शासनों की व्यावहारिक समझ को दर्शाता है।
औरंगज़ेब की नीतियाँ हिन्दू त्योहारों और मंदिरों के प्रति भी एकतरफ़ा नहीं थीं—बल्कि वे धार्मिक आस्थाओं, प्रशासनिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक चुनौतियों के मेल से तय होती थीं। काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि जैसे मंदिरों के विध्वंस को अक्सर बहुत प्रचारित किया जाता है, लेकिन ये घटनाएँ ज़्यादातर राजनीतिक और प्रतीकात्मक मक़सद से की गई थीं। अक्सर वे उन स्थलों को निशाना बनाकर की जाती थीं जो किसी विरोधी सत्ता केंद्र या बग़ावत से जुड़े हुए थे। उत्तर भारत में मंदिरों पर कार्रवाई राजनीतिक विरोधियों को दबाने का माध्यम बनी, जबकि दक्षिण भारत में मंदिरों को संरक्षण देकर स्थानीय गठबंधनों को मज़बूत करने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण कायम करने की कोशिश की गई।
ऐतिहासिक दस्तावेज़ों से इस बात का सीधा खंडन होता है कि औरंगज़ेब की नीतियाँ सिर्फ़ साम्प्रदायिक थीं। उपलब्ध अभिलेख बताते हैं कि औरंगज़ेब ने बनारस, कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में स्थित कई मंदिरों की देखरेख के लिए बड़ी जागीरें दान में दी थीं। दक्षिण भारत में भी अनेक मंदिरों को भारी अनुदान दिए गए ताकि मुग़ल शासन की पकड़ नये अधिग्रहित इलाक़ों में मजबूत हो सके। इन फैसलों के पीछे प्राथमिक तौर पर राजनीतिक दूरदृष्टि और प्रशासनिक व्यावहारिकता थी, न कि कोई व्यापक साम्प्रदायिक एजेंडा।
इस प्रकार औरंगजेब की नीतियों में राजनीतिक व्यावहारिकता, आर्थिक रणनीति और धार्मिक विचारों का मिश्रण दिखाई देता है। उन्हें एकपक्षीय व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करना इतिहास को विकृत करता है और समाज में और अधिक विभाजन का ख़तरा पैदा करता है।
शिवाजी बनाम औरंगजेब
औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच संघर्ष मुख्य रूप से राजनीतिक था। वह धार्मिक या सांप्रदायिक मतभेदों के बजाय क्षेत्रीय नियंत्रण और संप्रभुता पर केंद्रित था। दोनों शासक अपने-अपने राज्य विस्तार की कोशिश में लगे थे, जिससे टकराव होना स्वाभाविक था।
औरंगजेब का लक्ष्य भारत भर में मुगल साम्राज्य के प्रभाव को मजबूत करना और उसका विस्तार करना था। मराठों सहित अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ उनके अभियान राजनीतिक प्रभुत्व की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थे। उनमें से कई का नेतृत्व हिंदू सेनापतियों के हाथ में था, इस हद तक कि इससे मुस्लिम सरदारों में नाराजगी पैदा हो गई। औरंगज़ेब ने अपने निर्णय को शरीअत के संदर्भ में समझाया, जिसमें यह प्रावधान है कि सार्वजनिक प्रशासन में हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर पद मिलना चाहिए। यह उनके प्रशासन की उस समझ को दर्शाता है जो धार्मिक पहचान से ज़्यादा क्षमता और कुशलता को महत्व देती थी।
शिवाजी महाराज की राजनीतिक प्राथमिकता भी एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना और बाहरी प्रभुत्व के ख़िलाफ़ प्रतिरोध पर केंद्रित थी। उनकी सेना और प्रशासन भी समावेशी था, जिसमें कई मुस्लिम अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे: उनके विश्वस्त सेनापति सिद्दी हिलालस; एक प्रमुख कमांडर इन चीफ़ दौलत ख़ान; प्रमुख सैन्य पद पर रहे इब्राहिम ख़ान; 13 विश्वस्त मुस्लिम सेनापतियों में शामिल काज़ी हैदर; सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले सिद्दी इब्राहिम; एक और मुस्लिम सेनापति सिद्दी वहवाह; और उनकी सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नूरख़ान बेग, सुल्तान ख़ान, दाऊद ख़ान और शमा ख़ान; विश्वस्त मुस्लिम सेनापतियों में शामिल हुसैन ख़ान मियानी; दौलत ख़ान के साथ कमांडर-इन-चीफ़ रहे सिद्दी मिस्त्री; और भरोसेमंद सेनापतियों में गिने जाने वाले मदार मेहतर भी उनके साथ थे। इससे स्पष्ट होता है कि शिवाजी भी धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं थे, बल्कि उनका नेतृत्व व्यावहारिक और समावेशी था।
औरंगज़ेब और शिवाजी के बीच हुए संवाद और समझौते भी इस टकराव की राजनीतिक प्रकृति को ही रेखांकित करते हैं। उदाहरण के लिए, 1665 की पुरंदर संधि में शिवाजी ने कुछ क़िले मुग़लों को सौंपे और एक अधीन शासक (वस्सल) के रूप में मुग़ल दरबार की मान्यता स्वीकार की—जो इस बात को दर्शाता है कि दोनों पक्षों के बीच प्रयोजनपरक बातचीत और राजनीतिक समझौता संभव था।
अंततः, इन दोनों नेताओं के बीच का संघर्ष धार्मिक वैमनस्य पर आधारित नहीं था, बल्कि सत्ता के दावों और भू-राजनीतिक हितों से प्रेरित था। दोनों ही शासकों ने अपने-अपने शासन में समावेशी प्रशासन की मिसालें पेश कीं, जो उनके समय की व्यावहारिक शासन-नीति का प्रतिबिंब थीं।
औरंगज़ेब का किरदार
हर शासक की तरह औरंगज़ेब न तो कोई नैतिक आदर्श थे, न ही महज़ एक खलनायक। एक राजा की तरह उन्होंने भी अपनी प्रजा के प्रति ज़िम्मेदारी को आत्मसात किया था। लेकिन इन सब तथ्यों से इतर, यह भी सच है कि औरंगज़ेब की मृत्यु को तीन सौ साल से ज़्यादा हो चुके हैं।
आज उनके ख़िलाफ़ चलाया जा रहा यह अत्यधिक दुश्मनी से भरा अभियान एक अजीब विडंबना को जन्म देता है—वह यह कि यह अभियान खुद उसी विकृत छवि को दोहराता है, जो सत्ता में बैठे लोग औरंगज़ेब को लेकर गढ़ते आए हैं।
भारत इस समय कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है—बढ़ती बेरोज़गारी, गिरते निवेश (वित्त वर्ष 2024–25 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है), घटता उपभोग (जिसका संकेत HSBC इंडिया कॉम्पोज़िट परचेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स में लगातार आती गिरावट से मिलता है), बढ़ती असमानता, गहराता कृषि संकट, गिरता हुआ रुपया और महंगाई का तेज़ दबाव।
इन चुनौतियों को और भी कठिन बना रहे हैं निर्यात क्षेत्र में आ रही रुकावटें, जो रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनीतिक संकटों के चलते वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान की वजह से पैदा हुई हैं—साथ ही अमेरिका की व्यापार नीतियों से जुड़े संभावित ख़तरे भी हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और अस्थिर कर सकते हैं।
लेकिन इन ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने और देश की सामूहिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के बजाय, हमारे नेतृत्व का ध्यान इस समय औरंगज़ेब की क़ब्र पर बहस करने और मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने में लगा हुआ है।
अगर औरंगज़ेब के शासनकाल से कोई सबक लिया जा सकता है, तो वह यही है कि धर्म और राजनीति के घालमेल से शासन अंततः कमज़ोर ही होता है। धार्मिक कट्टरता को थोपने की उनकी कोशिशों ने उनके कई अहम सहयोगियों को उनसे दूर कर दिया, समाज में विभाजन को और गहरा किया, और व्यापक प्रतिरोध को जन्म दिया—जिसका नतीजा यह हुआ कि मुग़ल साम्राज्य की नींव हिल गई और उसका पतन तेज़ हो गया।
क्या औरंगज़ेब का भूत हमारे नेताओं को जगाकर राजधर्म की और सचेत होने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे वे इस देश के सामने खड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर पायें?